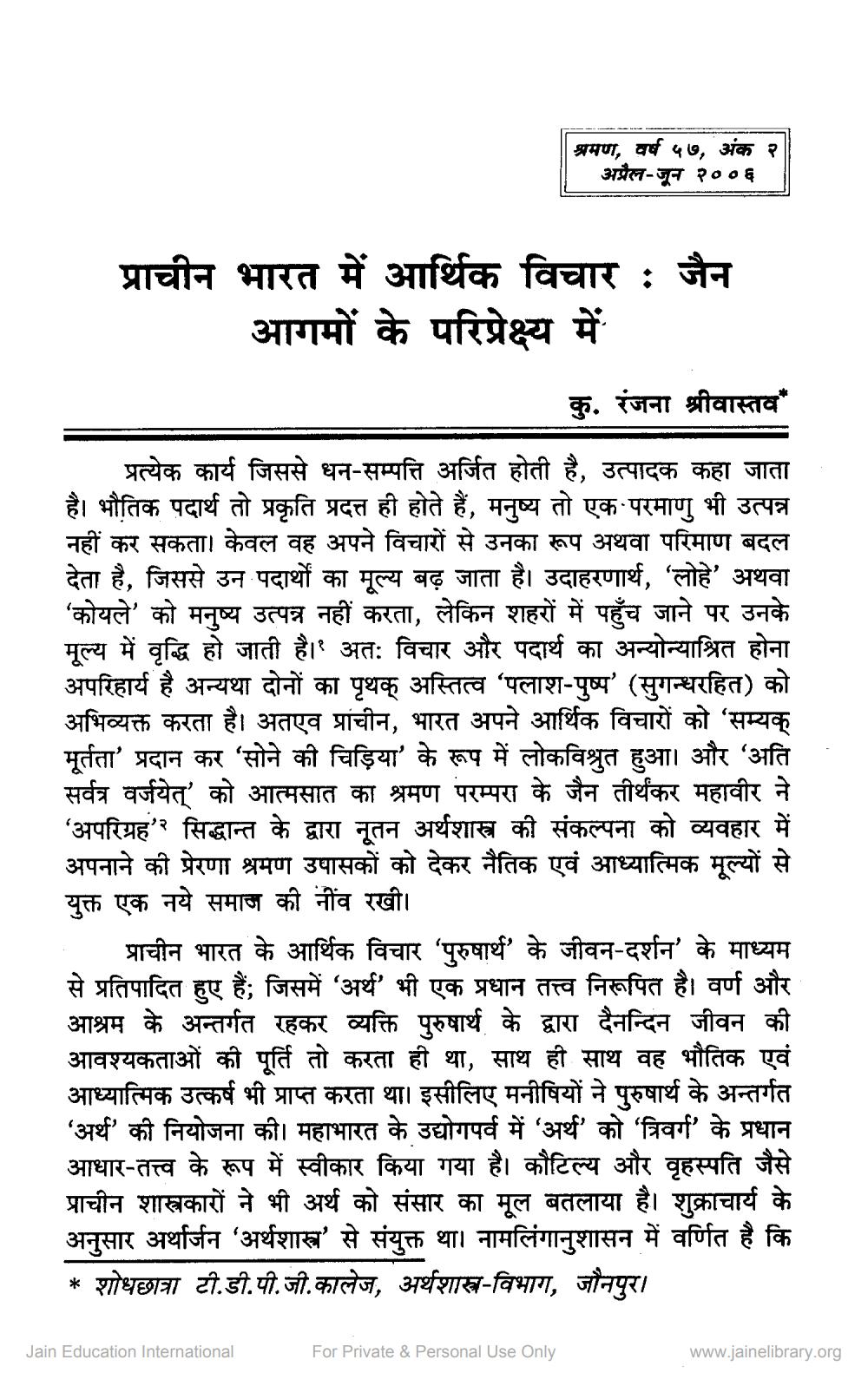________________
श्रमण, वर्ष ५७, अंक २
अप्रैल-जून २००६
प्राचीन भारत में आर्थिक विचार : जैन
आगमों के परिप्रेक्ष्य में
कु. रंजना श्रीवास्तव
प्रत्येक कार्य जिससे धन-सम्पत्ति अर्जित होती है, उत्पादक कहा जाता है। भौतिक पदार्थ तो प्रकृति प्रदत्त ही होते हैं, मनुष्य तो एक परमाणु भी उत्पन्न नहीं कर सकता। केवल वह अपने विचारों से उनका रूप अथवा परिमाण बदल देता है, जिससे उन पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है। उदाहरणार्थ, 'लोहे' अथवा 'कोयले' को मनुष्य उत्पन्न नहीं करता, लेकिन शहरों में पहुँच जाने पर उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। अत: विचार और पदार्थ का अन्योन्याश्रित होना अपरिहार्य है अन्यथा दोनों का पृथक् अस्तित्व ‘पलाश-पुष्प' (सुगन्धरहित) को अभिव्यक्त करता है। अतएव प्राचीन, भारत अपने आर्थिक विचारों को 'सम्यक् मूर्तता' प्रदान कर 'सोने की चिड़िया' के रूप में लोकविश्रुत हुआ। और 'अति सर्वत्र वर्जयेत्' को आत्मसात का श्रमण परम्परा के जैन तीर्थंकर महावीर ने 'अपरिग्रह'२ सिद्धान्त के द्वारा नूतन अर्थशास्त्र की संकल्पना को व्यवहार में अपनाने की प्रेरणा श्रमण उपासकों को देकर नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त एक नये समाज की नींव रखी। - प्राचीन भारत के आर्थिक विचार 'पुरुषार्थ' के जीवन-दर्शन' के माध्यम से प्रतिपादित हुए हैं; जिसमें 'अर्थ' भी एक प्रधान तत्त्व निरूपित है। वर्ण और आश्रम के अन्तर्गत रहकर व्यक्ति पुरुषार्थ के द्वारा दैनन्दिन जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता ही था, साथ ही साथ वह भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष भी प्राप्त करता था। इसीलिए मनीषियों ने पुरुषार्थ के अन्तर्गत 'अर्थ' की नियोजना की। महाभारत के उद्योगपर्व में 'अर्थ' को 'त्रिवर्ग' के प्रधान
आधार-तत्त्व के रूप में स्वीकार किया गया है। कौटिल्य और वृहस्पति जैसे प्राचीन शास्त्रकारों ने भी अर्थ को संसार का मूल बतलाया है। शुक्राचार्य के अनुसार अर्थार्जन 'अर्थशास्त्र' से संयुक्त था। नामलिंगानुशासन में वर्णित है कि * शोधछात्रा टी.डी.पी.जी.कालेज, अर्थशास्त्र-विभाग, जौनपुर।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org