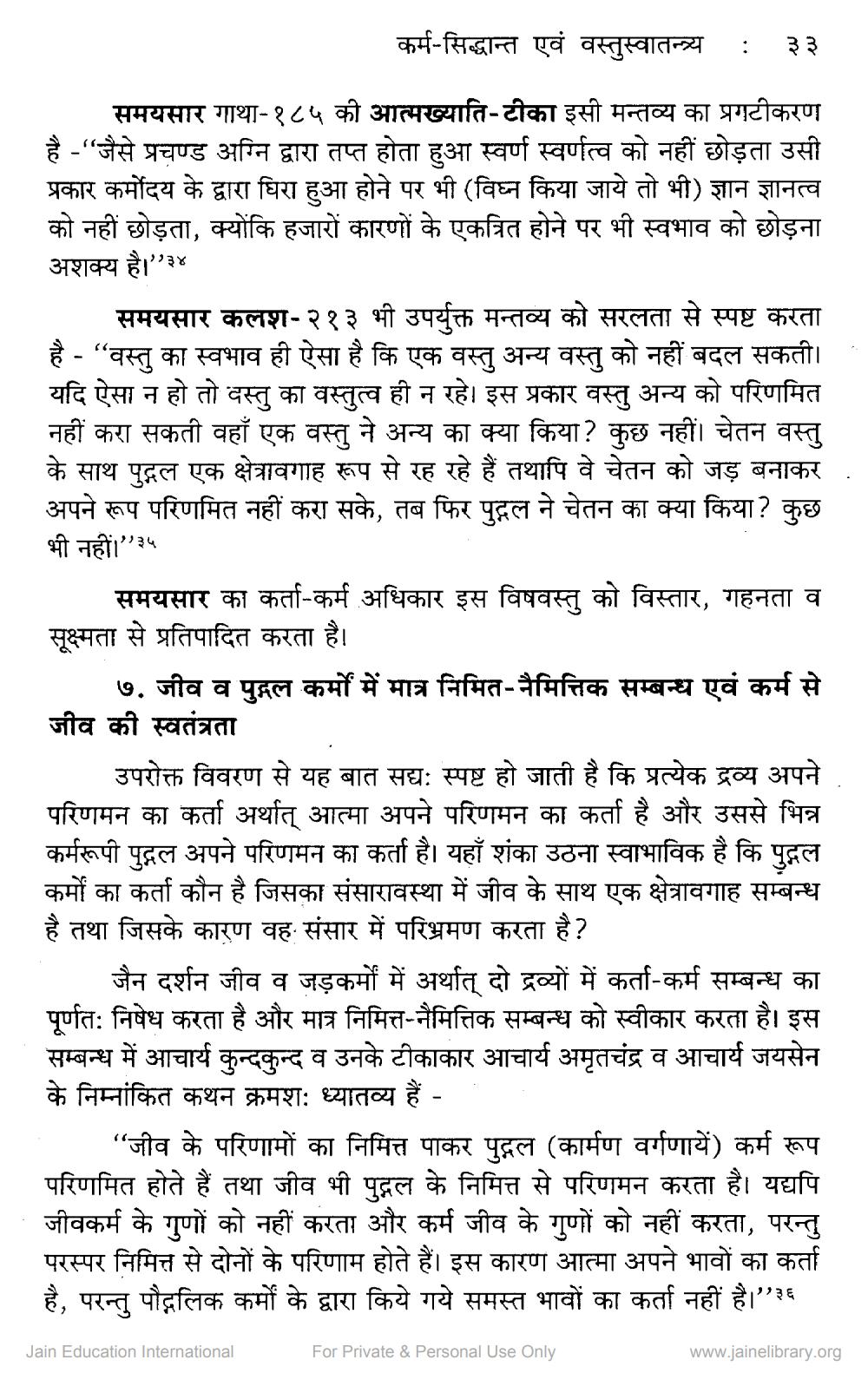________________
कर्म - सिद्धान्त एवं वस्तुस्वातन्त्र्य : ३३
समयसार गाथा - १८५ की आत्मख्याति - टीका इसी मन्तव्य का प्रगटीकरण है - " जैसे प्रचण्ड अग्नि द्वारा तप्त होता हुआ स्वर्ण स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता उसी प्रकार कर्मोदय के द्वारा घिरा हुआ होने पर भी (विघ्न किया जाये तो भी) ज्ञान ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता, क्योंकि हजारों कारणों के एकत्रित होने पर भी स्वभाव को छोड़ना अशक्य है।'’३४
समयसार कलश - २१३ भी उपर्युक्त मन्तव्य को सरलता से स्पष्ट करता है - “वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है कि एक वस्तु अन्य वस्तु को नहीं बदल सकती। यदि ऐसा न हो तो वस्तु का वस्तुत्व ही न रहे। इस प्रकार वस्तु अन्य को परिणमित नहीं करा सकती वहाँ एक वस्तु ने अन्य का क्या किया ? कुछ नहीं । चेतन वस्तु के साथ पुद्गल एक क्षेत्रावगाह रूप से रह रहे हैं तथापि वे चेतन को जड़ बनाकर अपने रूप परिणमित नहीं करा सके, तब फिर पुद्गल ने चेतन का क्या किया ? कुछ भी नहीं ।
११३५
समयसार का कर्ता-कर्म अधिकार इस विषवस्तु को विस्तार, गहनता व सूक्ष्मता से प्रतिपादित करता है।
७. जीव व पुद्गल कर्मों में मात्र निमित- नैमित्तिक सम्बन्ध एवं कर्म से जीव की स्वतंत्रता
उपरोक्त विवरण से यह बात सद्यः स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन का कर्ता अर्थात् आत्मा अपने परिणमन का कर्ता है और उससे भिन्न कर्मरूपी पुद्गल अपने परिणमन का कर्ता है। यहाँ शंका उठना स्वाभाविक है कि पुद्गल कर्मों का कर्ता कौन है जिसका संसारावस्था में जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध है तथा जिसके कारण वह संसार में परिभ्रमण करता है ?
जैन दर्शन जीव व जड़कर्मों में अर्थात् दो द्रव्यों में कर्ता-कर्म सम्बन्ध का पूर्णत: निषेध करता है और मात्र निमित्त - नैमित्तिक सम्बन्ध को स्वीकार करता है। इस सम्बन्ध में आचार्य कुन्दकुन्द व उनके टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र व आचार्य जयसेन के निम्नांकित कथन क्रमश: ध्यातव्य हैं -
" जीव के परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल (कार्मण वर्गणायें) कर्म रूप परिणमित होते हैं तथा जीव भी पुद्गल के निमित्त से परिणमन करता है । यद्यपि जीवकर्म के गुणों को नहीं करता और कर्म जीव के गुणों को नहीं करता, परन्तु परस्पर निमित्त से दोनों के परिणाम होते हैं। इस कारण आत्मा अपने भावों का कर्ता है, परन्तु पौगलिक कर्मों के द्वारा किये गये समस्त भावों का कर्ता नहीं है। "
१३६
For Private & Personal Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org