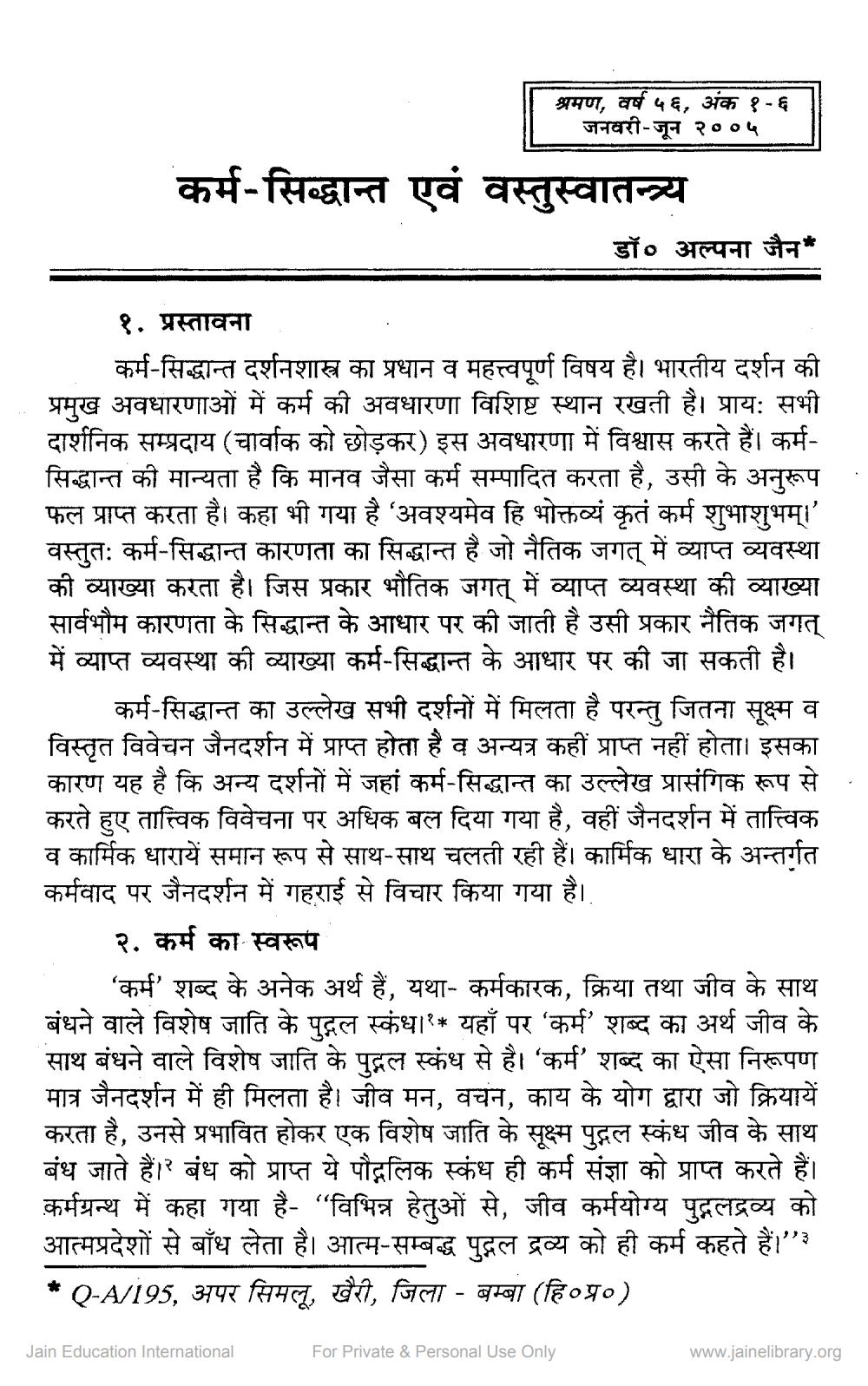________________
श्रमण, वर्ष ५६, अंक १-६
जनवरी-जून २००५
कर्म-सिद्धान्त एवं वस्तुस्वातन्त्र्य
डॉ० अल्पना जैन*
१. प्रस्तावना
कर्म-सिद्धान्त दर्शनशास्त्र का प्रधान व महत्त्वपूर्ण विषय है। भारतीय दर्शन की प्रमुख अवधारणाओं में कर्म की अवधारणा विशिष्ट स्थान रखती है। प्रायः सभी दार्शनिक सम्प्रदाय (चार्वाक को छोड़कर) इस अवधारणा में विश्वास करते हैं। कर्मसिद्धान्त की मान्यता है कि मानव जैसा कर्म सम्पादित करता है, उसी के अनुरूप फल प्राप्त करता है। कहा भी गया है 'अवश्यमेव हि भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्।' वस्तुतः कर्म-सिद्धान्त कारणता का सिद्धान्त है जो नैतिक जगत् में व्याप्त व्यवस्था की व्याख्या करता है। जिस प्रकार भौतिक जगत में व्याप्त व्यवस्था की व्याख्या सार्वभौम कारणता के सिद्धान्त के आधार पर की जाती है उसी प्रकार नैतिक जगत् में व्याप्त व्यवस्था की व्याख्या कर्म-सिद्धान्त के आधार पर की जा सकती है।
कर्म-सिद्धान्त का उल्लेख सभी दर्शनों में मिलता है परन्तु जितना सूक्ष्म व विस्तृत विवेचन जैनदर्शन में प्राप्त होता है व अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होता। इसका कारण यह है कि अन्य दर्शनों में जहां कर्म-सिद्धान्त का उल्लेख प्रासंगिक रूप से करते हुए तात्त्विक विवेचना पर अधिक बल दिया गया है, वहीं जैनदर्शन में तात्त्विक व कार्मिक धारायें समान रूप से साथ-साथ चलती रही हैं। कार्मिक धारा के अन्तर्गत कर्मवाद पर जैनदर्शन में गहराई से विचार किया गया है।
२. कर्म का स्वरूप
'कर्म' शब्द के अनेक अर्थ हैं, यथा- कर्मकारक, क्रिया तथा जीव के साथ बंधने वाले विशेष जाति के पुद्गल स्कंधा* यहाँ पर 'कर्म' शब्द का अर्थ जीव के साथ बंधने वाले विशेष जाति के पुद्गल स्कंध से है। 'कर्म' शब्द का ऐसा निरूपण मात्र जैनदर्शन में ही मिलता है। जीव मन, वचन, काय के योग द्वारा जो क्रियायें करता है, उनसे प्रभावित होकर एक विशेष जाति के सूक्ष्म पुद्गल स्कंध जीव के साथ बंध जाते हैं। बंध को प्राप्त ये पौद्गलिक स्कंध ही कर्म संज्ञा को प्राप्त करते हैं। कर्मग्रन्थ में कहा गया है- “विभिन्न हेतुओं से, जीव कर्मयोग्य पुद्गलद्रव्य को आत्मप्रदेशों से बाँध लेता है। आत्म-सम्बद्ध पुद्गल द्रव्य को ही कर्म कहते हैं।''३ * Q-A/195, अपर सिमलू, खैरी, जिला - बम्बा (हि०प्र०)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org