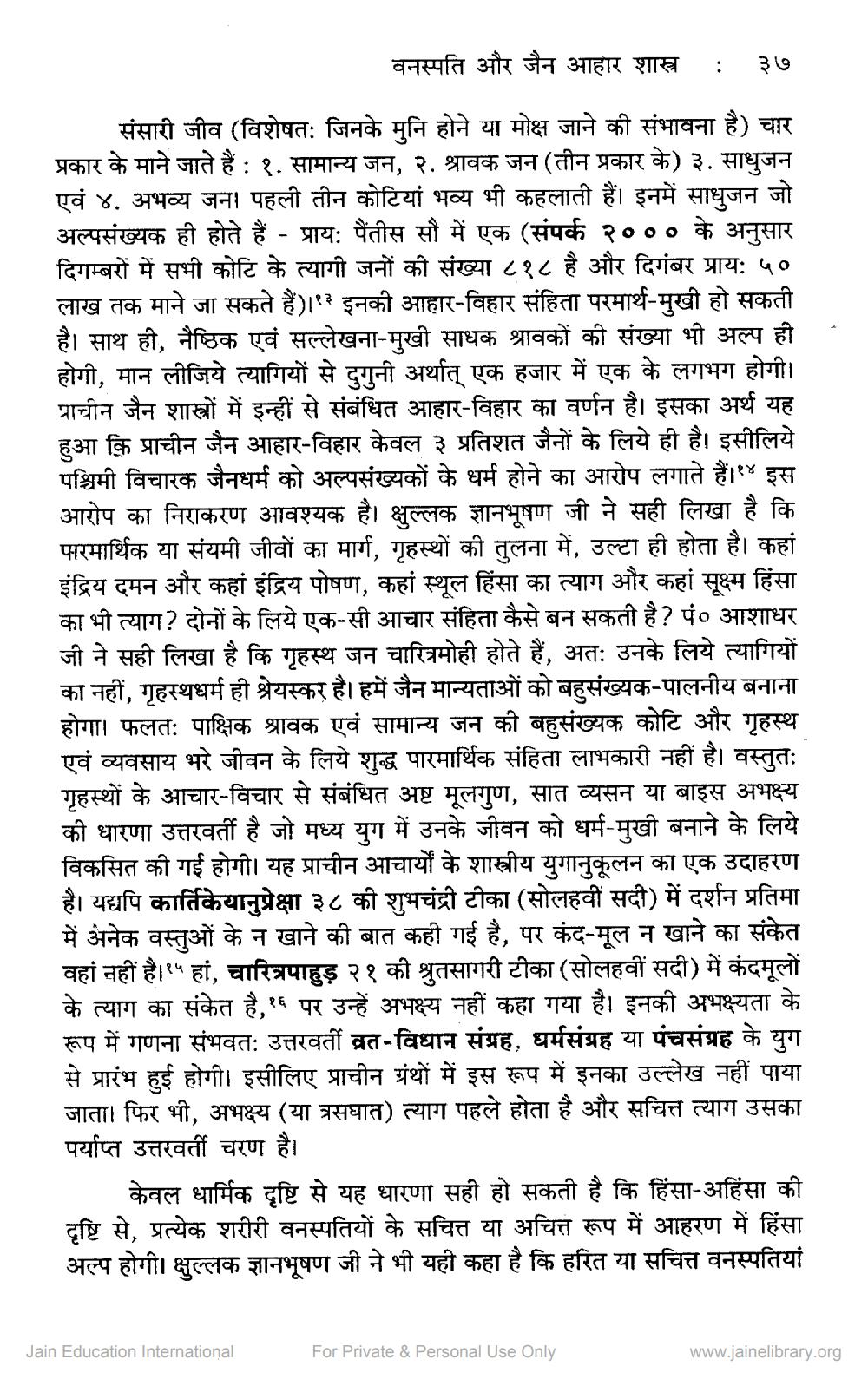________________
वनस्पति और जैन आहार शास्त्र : ३७
संसारी जीव (विशेषतः जिनके मुनि होने या मोक्ष जाने की संभावना है ) चार प्रकार के माने जाते हैं : १. सामान्य जन, २. श्रावक जन (तीन प्रकार के) ३. साधुजन एवं ४. अभव्य जन। पहली तीन कोटियां भव्य भी कहलाती हैं। इनमें साधुजन जो अल्पसंख्यक ही होते हैं प्राय: पैंतीस सौ में एक (संपर्क २००० के अनुसार दिगम्बरों में सभी कोटि के त्यागी जनों की संख्या ८१८ है और दिगंबर प्रायः ५० लाख तक माने जा सकते हैं)। १३ इनकी आहार-विहार संहिता परमार्थ - मुखी हो सकती है। साथ ही, नैष्ठिक एवं सल्लेखना - मुखी साधक श्रावकों की संख्या भी अल्प ही होगी, मान लीजिये त्यागियों से दुगुनी अर्थात् एक हजार में एक के लगभग होगी। प्राचीन जैन शास्त्रों में इन्हीं से संबंधित आहार-विहार का वर्णन है । इसका अर्थ यह हुआ कि प्राचीन जैन आहार-विहार केवल ३ प्रतिशत जैनों के लिये ही है । इसीलिये पश्चिमी विचारक जैनधर्म को अल्पसंख्यकों के धर्म होने का आरोप लगाते हैं। १४ इस आरोप का निराकरण आवश्यक है। क्षुल्लक ज्ञानभूषण जी ने सही लिखा है कि पारमार्थिक या संयमी जीवों का मार्ग, गृहस्थों की तुलना में, उल्टा ही होता है । कहां इंद्रिय दमन और कहां इंद्रिय पोषण, कहां स्थूल हिंसा का त्याग और कहां सूक्ष्म हिंसा का भी त्याग ? दोनों के लिये एक-सी आचार संहिता कैसे बन सकती है? पं० आशाधर जी ने सही लिखा है कि गृहस्थ जन चारित्रमोही होते हैं, अतः उनके लिये त्यागियों का नहीं, गृहस्थधर्म ही श्रेयस्कर है। हमें जैन मान्यताओं को बहुसंख्यक - पालनीय बनाना होगा। फलतः पाक्षिक श्रावक एवं सामान्य जन की बहुसंख्यक कोटि और गृहस्थ एवं व्यवसाय भरे जीवन के लिये शुद्ध पारमार्थिक संहिता लाभकारी नहीं है। वस्तुतः गृहस्थों के आचार-विचार से संबंधित अष्ट मूलगुण, सात व्यसन या बाइस अभक्ष्य की धारणा उत्तरवर्ती है जो मध्य युग में उनके जीवन को धर्म- मुखी बनाने के लिये विकसित की गई होगी। यह प्राचीन आचार्यों के शास्त्रीय युगानुकूलन का एक उदाहरण है । यद्यपि कार्तिकेयानुप्रेक्षा ३८ की शुभचंद्री टीका (सोलहवीं सदी) में दर्शन प्रतिमा में अनेक वस्तुओं के न खाने की बात कही गई है, पर कंद-मूल न खाने का संकेत वहां नहीं है। १५ हां, चारित्रपाहुड़ २१ की श्रुतसागरी टीका (सोलहवीं सदी) में कंदमूलों के त्याग का संकेत है, १६ पर उन्हें अभक्ष्य नहीं कहा गया है। इनकी अभक्ष्यता के रूप में गणना संभवत: उत्तरवर्ती व्रत विधान संग्रह, धर्मसंग्रह या पंचसंग्रह के युग से प्रारंभ हुई होगी। इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में इस रूप में इनका उल्लेख नहीं पाया जाता। फिर भी, अभक्ष्य ( या त्रसघात) त्याग पहले होता है और सचित्त त्याग उसका पर्याप्त उत्तरवर्ती चरण है।
-
-
केवल धार्मिक दृष्टि से यह धारणा सही हो सकती है कि हिंसा - अहिंसा की दृष्टि से, प्रत्येक शरीरी वनस्पतियों के सचित्त या अचित्त रूप में आहरण में हिंसा अल्प होगी। क्षुल्लक ज्ञानभूषण जी ने भी यही कहा है कि हरित या सचित्त वनस्पतियां
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org