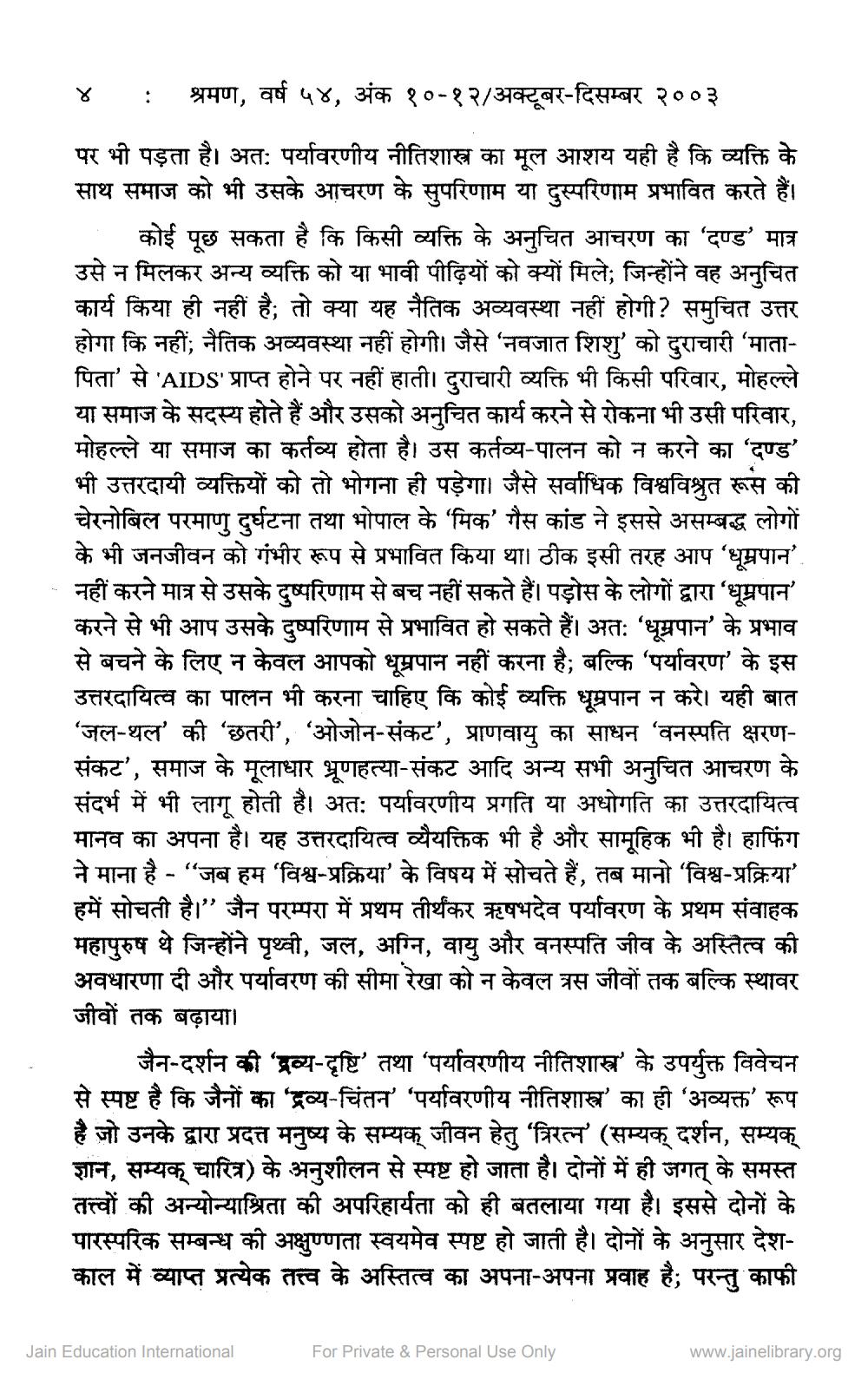________________
४
:
श्रमण, वर्ष ५४, अंक १०-१२/अक्टूबर-दिसम्बर २००३
पर भी पड़ता है। अत: पर्यावरणीय नीतिशास्त्र का मूल आशय यही है कि व्यक्ति के साथ समाज को भी उसके आचरण के सुपरिणाम या दुस्परिणाम प्रभावित करते हैं।
कोई पूछ सकता है कि किसी व्यक्ति के अनुचित आचरण का 'दण्ड' मात्र उसे न मिलकर अन्य व्यक्ति को या भावी पीढ़ियों को क्यों मिले; जिन्होंने वह अनुचित कार्य किया ही नहीं है; तो क्या यह नैतिक अव्यवस्था नहीं होगी? समुचित उत्तर होगा कि नहीं; नैतिक अव्यवस्था नहीं होगी। जैसे 'नवजात शिशु को दुराचारी 'मातापिता' से 'AIDS' प्राप्त होने पर नहीं हाती। दुराचारी व्यक्ति भी किसी परिवार, मोहल्ले या समाज के सदस्य होते हैं और उसको अनुचित कार्य करने से रोकना भी उसी परिवार, मोहल्ले या समाज का कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य-पालन को न करने का ‘दण्ड' भी उत्तरदायी व्यक्तियों को तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे सर्वाधिक विश्वविश्रुत रूस की चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना तथा भोपाल के 'मिक' गैस कांड ने इससे असम्बद्ध लोगों के भी जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। ठीक इसी तरह आप 'धूम्रपान' नहीं करने मात्र से उसके दुष्परिणाम से बच नहीं सकते हैं। पड़ोस के लोगों द्वारा 'धूम्रपान' करने से भी आप उसके दुष्परिणाम से प्रभावित हो सकते हैं। अत: 'धूम्रपान' के प्रभाव से बचने के लिए न केवल आपको धूम्रपान नहीं करना है; बल्कि 'पर्यावरण' के इस उत्तरदायित्व का पालन भी करना चाहिए कि कोई व्यक्ति धूम्रपान न करे। यही बात 'जल-थल' की 'छतरी', 'ओजोन-संकट', प्राणवायु का साधन 'वनस्पति क्षरणसंकट', समाज के मूलाधार भ्रूणहत्या-संकट आदि अन्य सभी अनुचित आचरण के संदर्भ में भी लागू होती है। अत: पर्यावरणीय प्रगति या अधोगति का उत्तरदायित्व मानव का अपना है। यह उत्तरदायित्व व्यैयक्तिक भी है और सामूहिक भी है। हाफिंग ने माना है - "जब हम 'विश्व-प्रक्रिया' के विषय में सोचते हैं, तब मानो 'विश्व-प्रक्रिया' हमें सोचती है।" जैन परम्परा में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव पर्यावरण के प्रथम संवाहक महापुरुष थे जिन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति जीव के अस्तित्व की अवधारणा दी और पर्यावरण की सीमा रेखा को न केवल त्रस जीवों तक बल्कि स्थावर जीवों तक बढ़ाया।
जैन-दर्शन की 'द्रव्य-दृष्टि' तथा 'पर्यावरणीय नीतिशास्त्र के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जैनों का 'द्रव्य-चिंतन' 'पर्यावरणीय नीतिशास्त्र' का ही 'अव्यक्त' रूप है जो उनके द्वारा प्रदत्त मनुष्य के सम्यक् जीवन हेतु 'त्रिरत्न' (सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चारित्र) के अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है। दोनों में ही जगत् के समस्त तत्त्वों की अन्योन्याश्रिता की अपरिहार्यता को ही बतलाया गया है। इससे दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध की अक्षुण्णता स्वयमेव स्पष्ट हो जाती है। दोनों के अनुसार देशकाल में व्याप्त प्रत्येक तत्त्व के अस्तित्व का अपना-अपना प्रवाह है; परन्तु काफी
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org