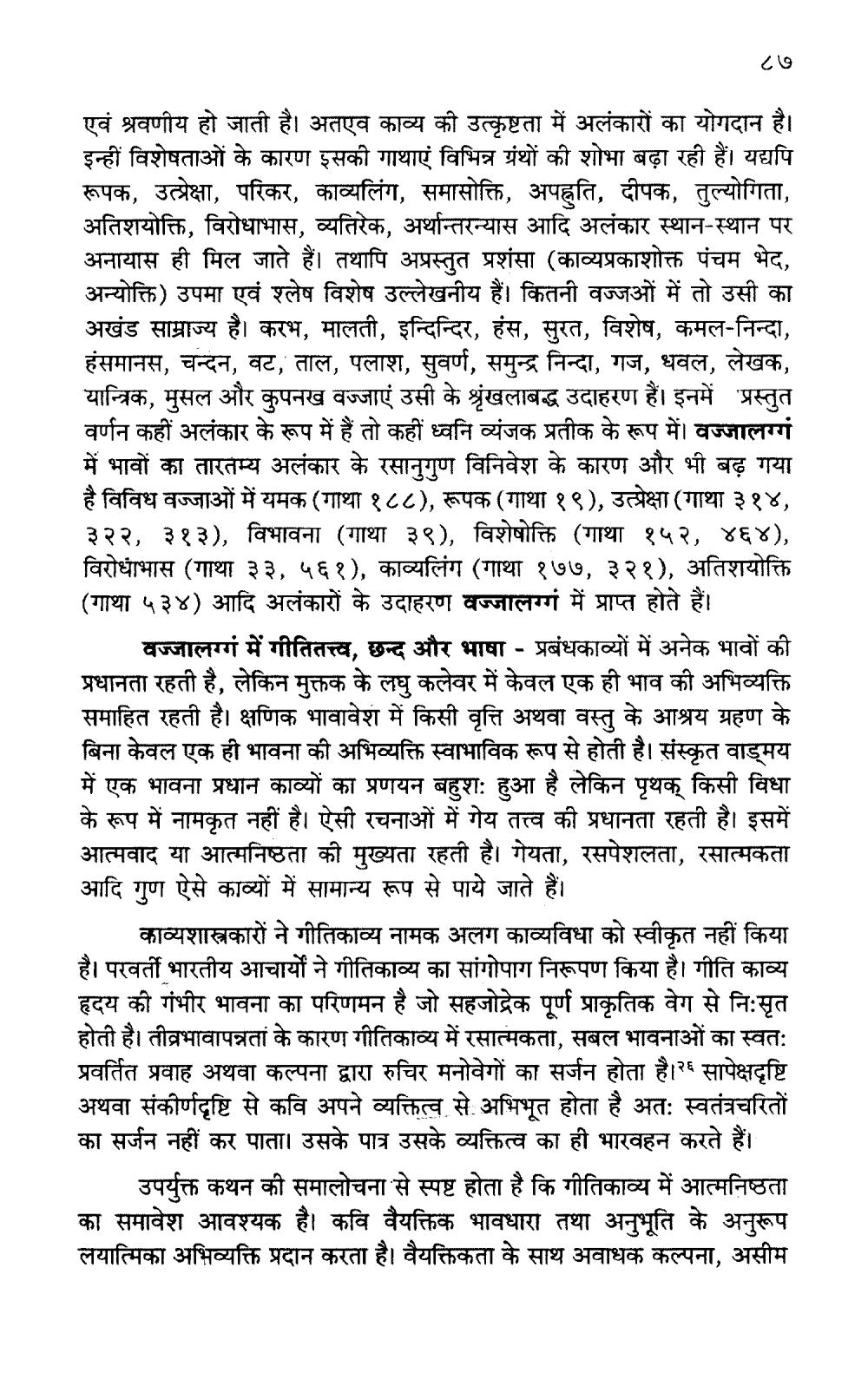________________
८७
एवं श्रवणीय हो जाती है। अतएव काव्य की उत्कृष्टता में अलंकारों का योगदान है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसकी गाथाएं विभिन्न ग्रंथों की शोभा बढ़ा रही हैं। यद्यपि रूपक, उत्प्रेक्षा, परिकर, काव्यलिंग, समासोक्ति, अपहृति, दीपक, तुल्योगिता, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, व्यतिरेक, अर्थान्तरन्यास आदि अलंकार स्थान-स्थान पर अनायास ही मिल जाते हैं। तथापि अप्रस्तुत प्रशंसा (काव्यप्रकाशोक्त पंचम भेद, अन्योक्ति) उपमा एवं श्लेष विशेष उल्लेखनीय हैं। कितनी वज्जओं में तो उसी का अखंड साम्राज्य है। करभ, मालती, इन्दिन्दिर, हंस, सुरत, विशेष, कमल-निन्दा, हंसमानस, चन्दन, वट, ताल, पलाश, सुवर्ण, समुन्द्र निन्दा, गज, धवल, लेखक, यान्त्रिक, मुसल और कुपनख वज्जाएं उसी के श्रृंखलाबद्ध उदाहरण हैं। इनमें 'प्रस्तुत वर्णन कहीं अलंकार के रूप में हैं तो कहीं ध्वनि व्यंजक प्रतीक के रूप में। वज्जालग्गं में भावों का तारतम्य अलंकार के रसानुगुण विनिवेश के कारण और भी बढ़ गया है विविध वज्जाओं में यमक (गाथा १८८), रूपक (गाथा १९), उत्प्रेक्षा (गाथा ३१४, ३२२, ३१३), विभावना (गाथा ३९), विशेषोक्ति (गाथा १५२, ४६४), विरोधाभास (गाथा ३३, ५६१), काव्यलिंग (गाथा १७७, ३२१), अतिशयोक्ति (गाथा ५३४) आदि अलंकारों के उदाहरण वज्जालग्गं में प्राप्त होते हैं।
वज्जालग्गं में गीतितत्त्व, छन्द और भाषा - प्रबंधकाव्यों में अनेक भावों की प्रधानता रहती है, लेकिन मुक्तक के लघु कलेवर में केवल एक ही भाव की अभिव्यक्ति समाहित रहती है। क्षणिक भावावेश में किसी वृत्ति अथवा वस्तु के आश्रय ग्रहण के बिना केवल एक ही भावना की अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूप से होती है। संस्कृत वाङ्मय में एक भावना प्रधान काव्यों का प्रणयन बहुश: हुआ है लेकिन पृथक् किसी विधा के रूप में नामकृत नहीं है। ऐसी रचनाओं में गेय तत्त्व की प्रधानता रहती है। इसमें आत्मवाद या आत्मनिष्ठता की मुख्यता रहती है। गेयता, रसपेशलता, रसात्मकता आदि गुण ऐसे काव्यों में सामान्य रूप से पाये जाते हैं।
काव्यशास्त्रकारों ने गीतिकाव्य नामक अलग काव्यविधा को स्वीकृत नहीं किया है। परवर्ती भारतीय आचार्यों ने गीतिकाव्य का सांगोपाग निरूपण किया है। गीति काव्य हृदय की गंभीर भावना का परिणमन है जो सहजोद्रेक पूर्ण प्राकृतिक वेग से नि:सृत होती है। तीव्रभावापन्नता के कारण गीतिकाव्य में रसात्मकता, सबल भावनाओं का स्वतः प्रवर्तित प्रवाह अथवा कल्पना द्वारा रुचिर मनोवेगों का सर्जन होता है।२६ सापेक्षदृष्टि अथवा संकीर्णदृष्टि से कवि अपने व्यक्तित्व से अभिभूत होता है अत: स्वतंत्रचरितों का सर्जन नहीं कर पाता। उसके पात्र उसके व्यक्तित्व का ही भारवहन करते हैं।
उपर्युक्त कथन की समालोचना से स्पष्ट होता है कि गीतिकाव्य में आत्मनिष्ठता का समावेश आवश्यक है। कवि वैयक्तिक भावधारा तथा अनुभूति के अनुरूप लयात्मिका अभिव्यक्ति प्रदान करता है। वैयक्तिकता के साथ अवाधक कल्पना, असीम