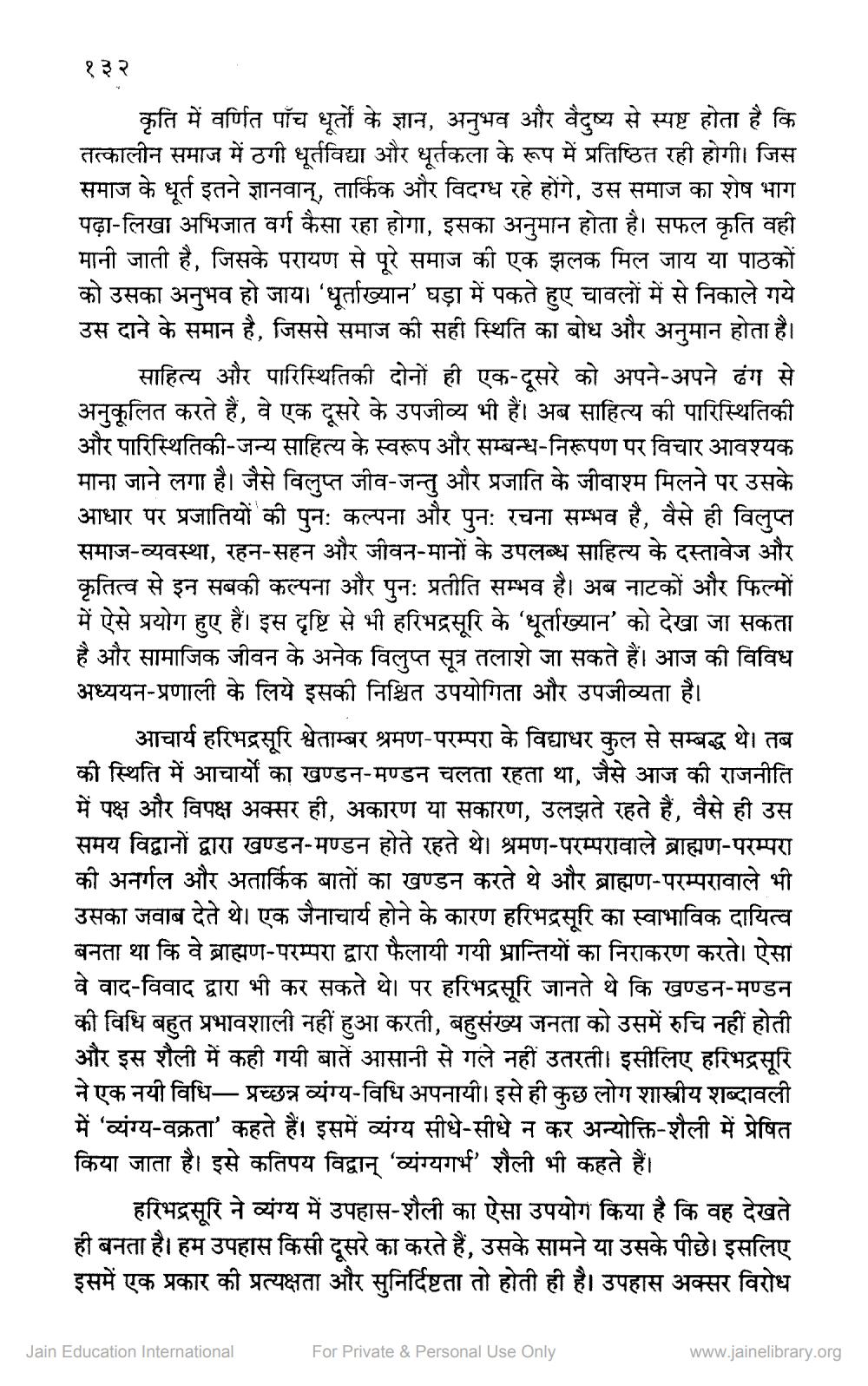________________
१३२
कृति में वर्णित पाँच धर्तों के ज्ञान, अनभव और वैदष्य से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज में ठगी धूर्तविद्या और धूर्तकला के रूप में प्रतिष्ठित रही होगी। जिस समाज के धूर्त इतने ज्ञानवान्, तार्किक और विदग्ध रहे होंगे, उस समाज का शेष भाग पढ़ा-लिखा अभिजात वर्ग कैसा रहा होगा, इसका अनुमान होता है। सफल कृति वही मानी जाती है, जिसके परायण से पूरे समाज की एक झलक मिल जाय या पाठकों को उसका अनुभव हो जाय। 'धूर्ताख्यान' घड़ा में पकते हुए चावलों में से निकाले गये उस दाने के समान है, जिससे समाज की सही स्थिति का बोध और अनुमान होता है।
साहित्य और पारिस्थितिकी दोनों ही एक-दूसरे को अपने-अपने ढंग से अनुकूलित करते हैं, वे एक दूसरे के उपजीव्य भी हैं। अब साहित्य की पारिस्थितिकी
और पारिस्थितिकी-जन्य साहित्य के स्वरूप और सम्बन्ध-निरूपण पर विचार आवश्यक माना जाने लगा है। जैसे विलुप्त जीव-जन्तु और प्रजाति के जीवाश्म मिलने पर उसके आधार पर प्रजातियों की पुन: कल्पना और पुन: रचना सम्भव है, वैसे ही विलुप्त समाज-व्यवस्था, रहन-सहन और जीवन-मानों के उपलब्ध साहित्य के दस्तावेज और कृतित्व से इन सबकी कल्पना और पुन: प्रतीति सम्भव है। अब नाटकों और फिल्मों में ऐसे प्रयोग हुए हैं। इस दृष्टि से भी हरिभद्रसूरि के 'धूर्ताख्यान' को देखा जा सकता है और सामाजिक जीवन के अनेक विलुप्त सूत्र तलाशे जा सकते हैं। आज की विविध अध्ययन-प्रणाली के लिये इसकी निश्चित उपयोगिता और उपजीव्यता है।
आचार्य हरिभद्रसूरि श्वेताम्बर श्रमण-परम्परा के विद्याधर कुल से सम्बद्ध थे। तब की स्थिति में आचार्यों का खण्डन-मण्डन चलता रहता था, जैसे आज की राजनीति में पक्ष और विपक्ष अक्सर ही, अकारण या सकारण, उलझते रहते हैं, वैसे ही उस समय विद्वानों द्वारा खण्डन-मण्डन होते रहते थे। श्रमण-परम्परावाले ब्राह्मण-परम्परा की अनर्गल और अतार्किक बातों का खण्डन करते थे और ब्राह्मण-परम्परावाले भी उसका जवाब देते थे। एक जैनाचार्य होने के कारण हरिभद्रसूरि का स्वाभाविक दायित्व बनता था कि वे ब्राह्मण-परम्परा द्वारा फैलायी गयी भ्रान्तियों का निराकरण करते। ऐसा वे वाद-विवाद द्वारा भी कर सकते थे। पर हरिभद्रसूरि जानते थे कि खण्डन-मण्डन की विधि बहुत प्रभावशाली नहीं हुआ करती, बहुसंख्य जनता को उसमें रुचि नहीं होती और इस शैली में कही गयी बातें आसानी से गले नहीं उतरती। इसीलिए हरिभद्रसूरि ने एक नयी विधि— प्रच्छन्न व्यंग्य-विधि अपनायी। इसे ही कुछ लोग शास्त्रीय शब्दावली में 'व्यंग्य-वक्रता' कहते हैं। इसमें व्यंग्य सीधे-सीधे न कर अन्योक्ति-शैली में प्रेषित किया जाता है। इसे कतिपय विद्वान् ‘व्यंग्यगर्भ' शैली भी कहते हैं।
हरिभद्रसूरि ने व्यंग्य में उपहास-शैली का ऐसा उपयोग किया है कि वह देखते ही बनता है। हम उपहास किसी दूसरे का करते हैं, उसके सामने या उसके पीछे। इसलिए इसमें एक प्रकार की प्रत्यक्षता और सुनिर्दिष्टता तो होती ही है। उपहास अक्सर विरोध
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org