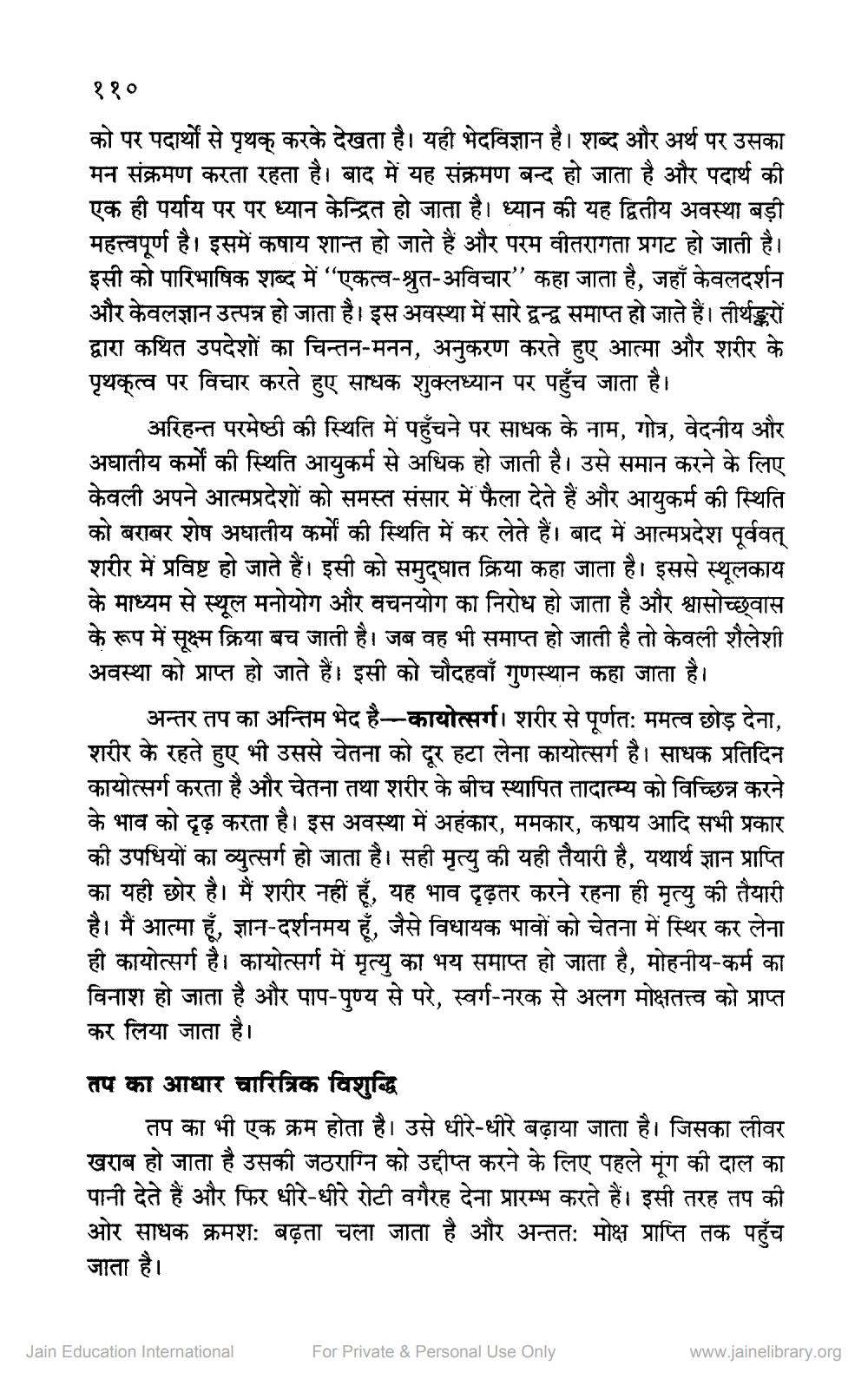________________
११०
को पर पदार्थों से पृथक् करके देखता है। यही भेदविज्ञान है। शब्द और अर्थ पर उसका मन संक्रमण करता रहता है। बाद में यह संक्रमण बन्द हो जाता है और पदार्थ की एक ही पर्याय पर पर ध्यान केन्द्रित हो जाता है। ध्यान की यह द्वितीय अवस्था बड़ी महत्त्वपूर्ण है। इसमें कषाय शान्त हो जाते हैं और परम वीतरागता प्रगट हो जाती है। इसी को पारिभाषिक शब्द में “एकत्व-श्रुत-अविचार" कहा जाता है, जहाँ केवलदर्शन
और केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में सारे द्वन्द्व समाप्त हो जाते हैं। तीर्थङ्करों द्वारा कथित उपदेशों का चिन्तन-मनन, अनुकरण करते हुए आत्मा और शरीर के पृथक्त्व पर विचार करते हुए साधक शुक्लध्यान पर पहुँच जाता है।
अरिहन्त परमेष्ठी की स्थिति में पहँचने पर साधक के नाम, गोत्र, वेदनीय और अघातीय कर्मों की स्थिति आयुकर्म से अधिक हो जाती है। उसे समान करने के लिए केवली अपने आत्मप्रदेशों को समस्त संसार में फैला देते हैं और आयुकर्म की स्थिति को बराबर शेष अघातीय कर्मों की स्थिति में कर लेते हैं। बाद में आत्मप्रदेश पूर्ववत् शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसी को समुद्घात क्रिया कहा जाता है। इससे स्थूलकाय के माध्यम से स्थूल मनोयोग और वचनयोग का निरोध हो जाता है और श्वासोच्छवास के रूप में सूक्ष्म क्रिया बच जाती है। जब वह भी समाप्त हो जाती है तो केवली शैलेशी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इसी को चौदहवाँ गुणस्थान कहा जाता है।
अन्तर तप का अन्तिम भेद है-कायोत्सर्ग। शरीर से पूर्णत: ममत्व छोड़ देना, शरीर के रहते हुए भी उससे चेतना को दूर हटा लेना कायोत्सर्ग है। साधक प्रतिदिन कायोत्सर्ग करता है और चेतना तथा शरीर के बीच स्थापित तादात्म्य को विच्छिन्न करने के भाव को दृढ़ करता है। इस अवस्था में अहंकार, ममकार, कषाय आदि सभी प्रकार की उपधियों का व्युत्सर्ग हो जाता है। सही मृत्यु की यही तैयारी है, यथार्थ ज्ञान प्राप्ति का यही छोर है। मैं शरीर नहीं हूँ, यह भाव दृढ़तर करने रहना ही मृत्यु की तैयारी है। मैं आत्मा हूँ, ज्ञान-दर्शनमय हूँ, जैसे विधायक भावों को चेतना में स्थिर कर लेना ही कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, मोहनीय-कर्म का विनाश हो जाता है और पाप-पुण्य से परे, स्वर्ग-नरक से अलग मोक्षतत्त्व को प्राप्त कर लिया जाता है। तप का आधार चारित्रिक विशुद्धि
तप का भी एक क्रम होता है। उसे धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है। जिसका लीवर खराब हो जाता है उसकी जठराग्नि को उद्दीप्त करने के लिए पहले मूंग की दाल का पानी देते हैं और फिर धीरे-धीरे रोटी वगैरह देना प्रारम्भ करते हैं। इसी तरह तप की
ओर साधक क्रमश: बढ़ता चला जाता है और अन्तत: मोक्ष प्राप्ति तक पहुँच जाता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org