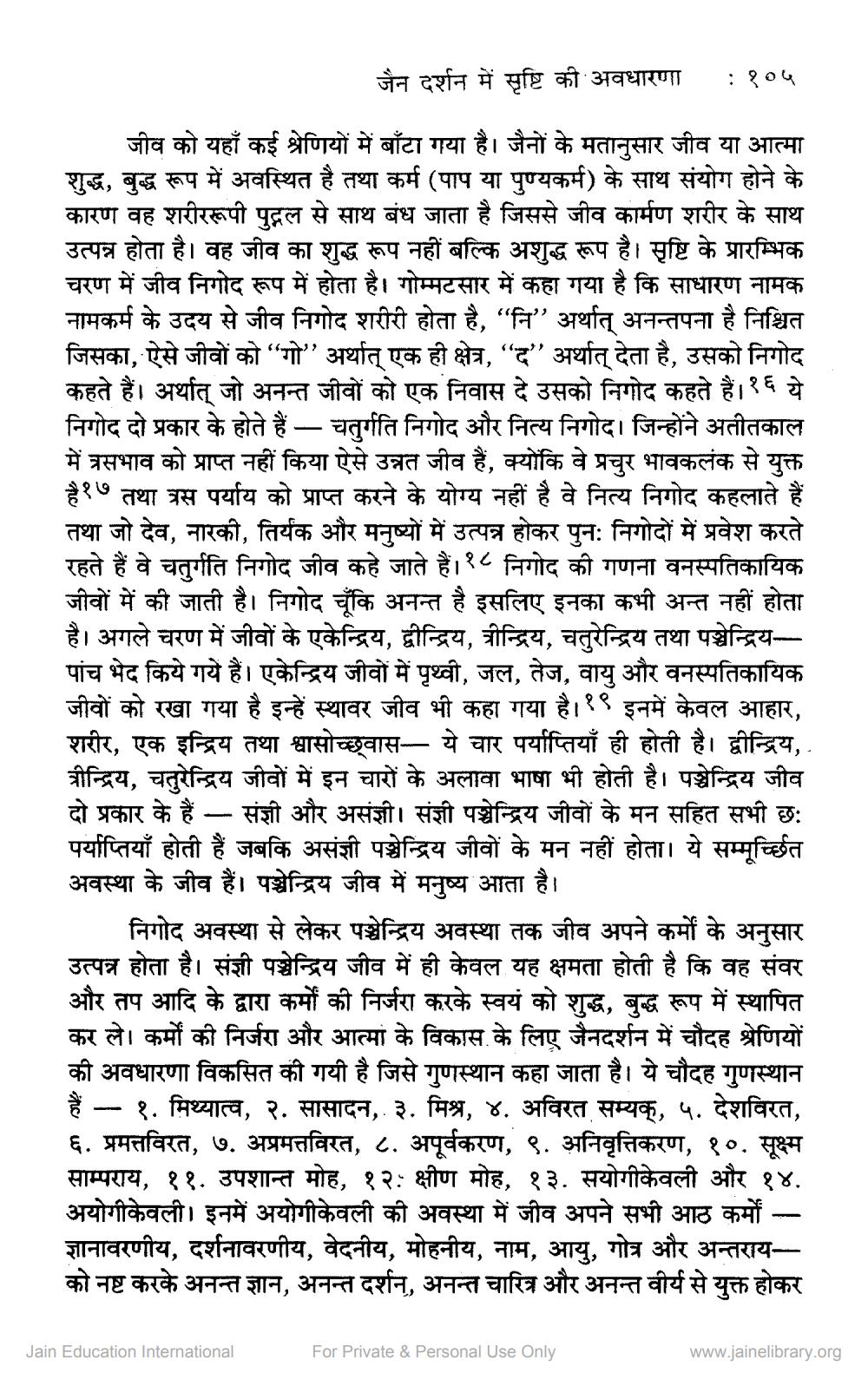________________
जैन दर्शन में सृष्टि की अवधारणा : १०५
-
जीव को यहाँ कई श्रेणियों में बाँटा गया है। जैनों के मतानुसार जीव या आत्मा शुद्ध, बुद्ध रूप में अवस्थित है तथा कर्म (पाप या पुण्यकर्म) के साथ संयोग होने के कारण वह शरीररूपी पुद्गल से साथ बंध जाता है जिससे जीव कार्मण शरीर के साथ उत्पन्न होता है। वह जीव का शुद्ध रूप नहीं बल्कि अशुद्ध रूप है। सृष्टि के प्रारम्भिक चरण में जीव निगोद रूप में होता है। गोम्मटसार में कहा गया है कि साधारण नामक नामकर्म के उदय से जीव निगोद शरीरी होता है, "नि” अर्थात् अनन्तपना है निश्चित जिसका, ऐसे जीवों को "गो" अर्थात् एक ही क्षेत्र, "द" अर्थात् देता है, उसको निगोद कहते हैं। अर्थात् जो अनन्त जीवों को एक निवास दे उसको निगोद कहते हैं । १६ ये निगोद दो प्रकार के होते हैं • चतुर्गति निगोद और नित्य निगोद । जिन्होंने अतीतकाल में त्रसभाव को प्राप्त नहीं किया ऐसे उन्नत जीव हैं, क्योंकि वे प्रचुर भावकलंक से युक्त है १७ तथा त्रस पर्याय को प्राप्त करने के योग्य नहीं है वे नित्य निगोद कहलाते हैं। तथा जो देव, नारकी, तिर्यक और मनुष्यों में उत्पन्न होकर पुनः निगोदों में प्रवेश करते रहते हैं वे चतुर्गति निगोद जीव कहे जाते हैं । १८ निगोद की गणना वनस्पतिकायिक जीवों में की जाती है। निगोद चूँकि अनन्त है इसलिए इनका कभी अन्त नहीं होता है। अगले चरण में जीवों के एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरेन्द्रिय तथा पञ्चेन्द्रियपांच भेद किये गये हैं। एकेन्द्रिय जीवों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और वनस्पतिकायिक जीवों को रखा गया है इन्हें स्थावर जीव भी कहा गया है । १९ इनमें केवल आहार, शरीर, एक इन्द्रिय तथा श्वासोच्छ्वास- ये चार पर्याप्तियाँ ही होती है । द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरेन्द्रिय जीवों में इन चारों के अलावा भाषा भी होती है । पञ्चेन्द्रिय जीव दो प्रकार के हैं संज्ञी और असंज्ञी। संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवों के मन सहित सभी छः पर्याप्तियाँ होती हैं जबकि असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवों के मन नहीं होता। ये सम्मूर्च्छित अवस्था के जीव हैं। पञ्चेन्द्रिय जीव में मनुष्य आता है।
--
हैं
निगोद अवस्था से लेकर पञ्चेन्द्रिय अवस्था तक जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्पन्न होता है । संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव में ही केवल यह क्षमता होती है कि वह संवर और तप आदि के द्वारा कर्मों की निर्जरा करके स्वयं को शुद्ध, बुद्ध रूप में स्थापित कर ले। कर्मों की निर्जरा और आत्मा के विकास के लिए जैनदर्शन में चौदह श्रेणियों की अवधारणा विकसित की गयी है जिसे गुणस्थान कहा जाता है। ये चौदह गुणस्थान १. मिथ्यात्व, २. सासादन, ३. मिश्र, ४. अविरत सम्यक्, ५. देशविरत, ६. प्रमत्तविरत, ७. अप्रमत्तविरत, ८. अपूर्वकरण, ९. अनिवृत्तिकरण, १०. सूक्ष्म साम्पराय, ११. उपशान्त मोह, १२ : क्षीण मोह, १३. सयोगीकेवली और १४. अयोगकेवली । इनमें अयोगीकेवली की अवस्था में जीव अपने सभी आठ कर्मों ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, आयु, गोत्र और अन्तरायकष्ट कर अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र और अनन्त वीर्य से युक्त होकर
-
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org