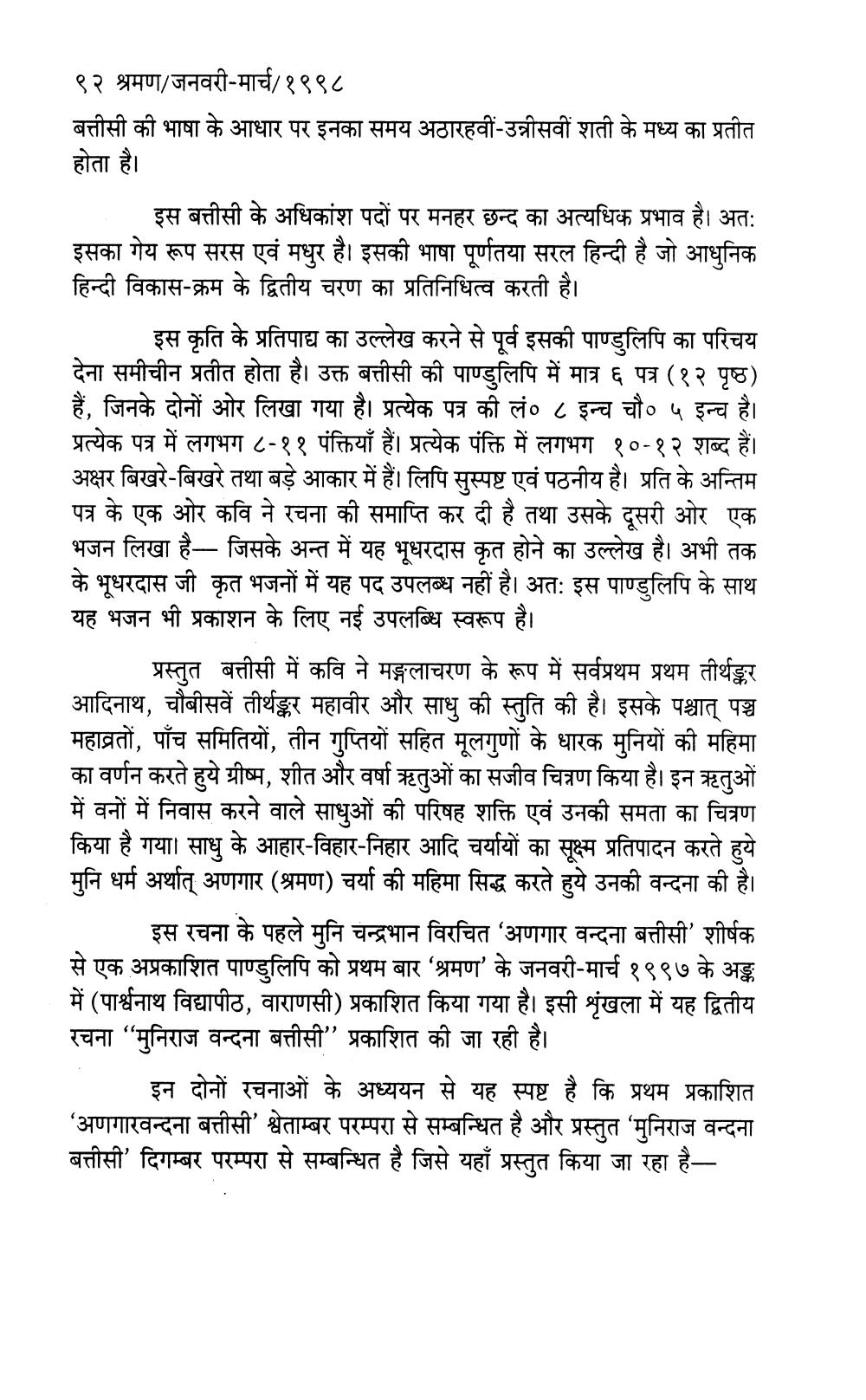________________
९२ श्रमण/जनवरी-मार्च/१९९८ बत्तीसी की भाषा के आधार पर इनका समय अठारहवीं-उन्नीसवीं शती के मध्य का प्रतीत होता है।
इस बत्तीसी के अधिकांश पदों पर मनहर छन्द का अत्यधिक प्रभाव है। अत: इसका गेय रूप सरस एवं मधुर है। इसकी भाषा पूर्णतया सरल हिन्दी है जो आधुनिक हिन्दी विकास-क्रम के द्वितीय चरण का प्रतिनिधित्व करती है।
इस कृति के प्रतिपाद्य का उल्लेख करने से पूर्व इसकी पाण्डुलिपि का परिचय देना समीचीन प्रतीत होता है। उक्त बत्तीसी की पाण्डुलिपि में मात्र ६ पत्र (१२ पृष्ठ) हैं, जिनके दोनों ओर लिखा गया है। प्रत्येक पत्र की लं० ८ इन्च चौ० ५ इन्च है। प्रत्येक पत्र में लगभग ८-११ पंक्तियाँ हैं। प्रत्येक पंक्ति में लगभग १०-१२ शब्द हैं। अक्षर बिखरे-बिखरे तथा बड़े आकार में हैं। लिपि सुस्पष्ट एवं पठनीय है। प्रति के अन्तिम पत्र के एक ओर कवि ने रचना की समाप्ति कर दी है तथा उसके दूसरी ओर एक भजन लिखा है- जिसके अन्त में यह भूधरदास कृत होने का उल्लेख है। अभी तक के भूधरदास जी कृत भजनों में यह पद उपलब्ध नहीं है। अत: इस पाण्डुलिपि के साथ यह भजन भी प्रकाशन के लिए नई उपलब्धि स्वरूप है।
प्रस्तत बत्तीसी में कवि ने मङ्गलाचरण के रूप में सर्वप्रथम प्रथम तीर्थङ्कर आदिनाथ, चौबीसवें तीर्थङ्कर महावीर और साधु की स्तुति की है। इसके पश्चात् पञ्च महाव्रतों, पाँच समितियों, तीन गुप्तियों सहित मूलगुणों के धारक मुनियों की महिमा का वर्णन करते हुये ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतुओं का सजीव चित्रण किया है। इन ऋतुओं में वनों में निवास करने वाले साधुओं की परिषह शक्ति एवं उनकी समता का चित्रण किया है गया। साधु के आहार-विहार-निहार आदि चर्यायों का सूक्ष्म प्रतिपादन करते हुये मुनि धर्म अर्थात् अणगार (श्रमण) चर्या की महिमा सिद्ध करते हुये उनकी वन्दना की है।
इस रचना के पहले मुनि चन्द्रभान विरचित 'अणगार वन्दना बत्तीसी' शीर्षक से एक अप्रकाशित पाण्डुलिपि को प्रथम बार 'श्रमण' के जनवरी-मार्च १९९७ के अङ्क में (पार्श्वनाथ विद्यापीठ, वाराणसी) प्रकाशित किया गया है। इसी श्रृंखला में यह द्वितीय रचना “मुनिराज वन्दना बत्तीसी' प्रकाशित की जा रही है।
इन दोनों रचनाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि प्रथम प्रकाशित 'अणगारवन्दना बत्तीसी' श्वेताम्बर परम्परा से सम्बन्धित है और प्रस्तुत ‘मुनिराज वन्दना बत्तीसी' दिगम्बर परम्परा से सम्बन्धित है जिसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है