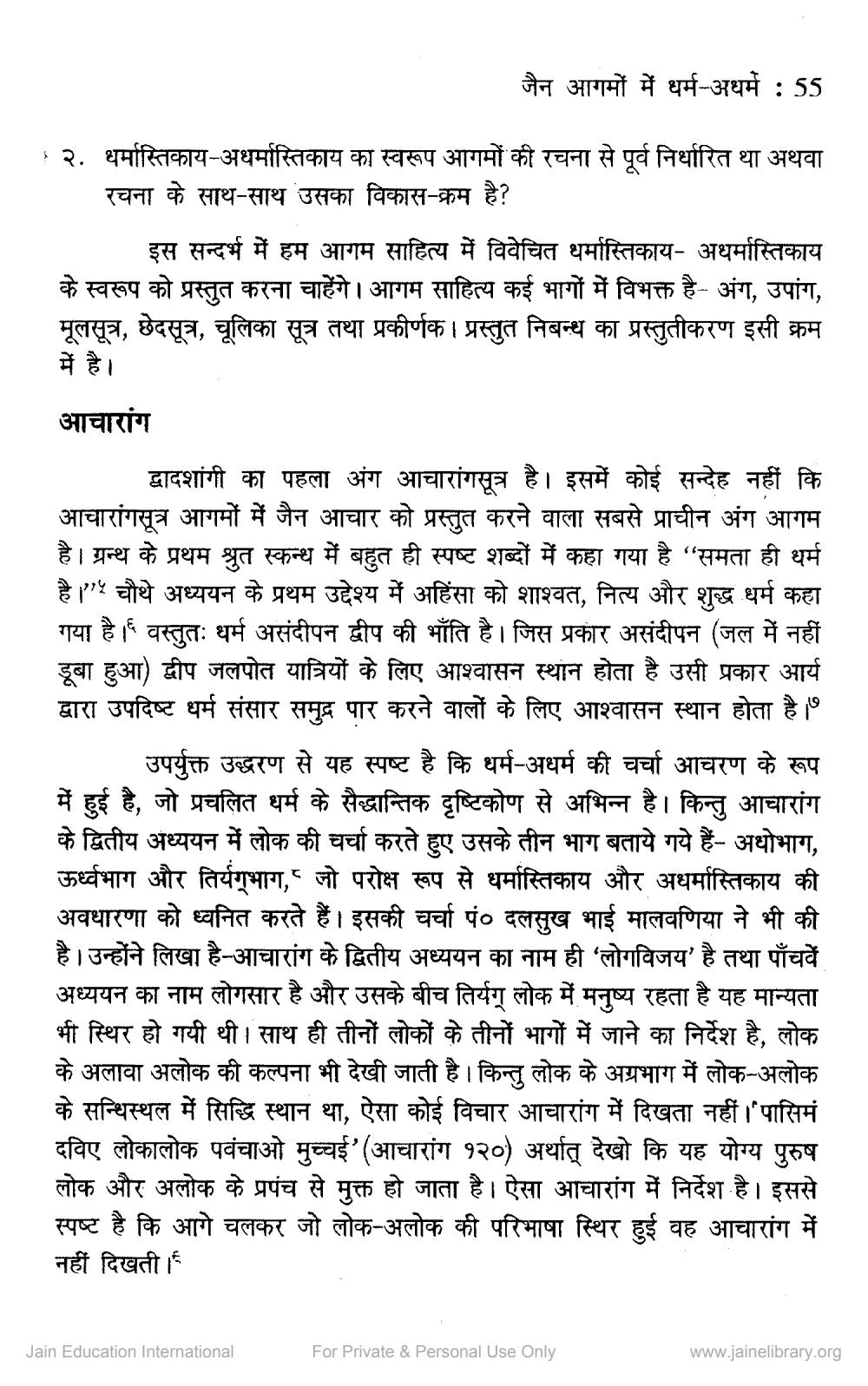________________
जैन आगमों में धर्म-अधर्म : 55
* २. धर्मास्तिकाय-अधर्मास्तिकाय का स्वरूप आगमों की रचना से पूर्व निर्धारित था अथवा रचना के साथ-साथ उसका विकास-क्रम है ?
इस सन्दर्भ में हम आगम साहित्य में विवेचित धर्मास्तिकाय- अधर्मास्तिकाय के स्वरूप को प्रस्तुत करना चाहेंगे। आगम साहित्य कई भागों में विभक्त है- अंग, उपांग, मूलसूत्र, छेदसूत्र, चूलिका सूत्र तथा प्रकीर्णक । प्रस्तुत निबन्ध का प्रस्तुतीकरण इसी क्रम में है ।
आचारांग
"
द्वादशांगी का पहला अंग आचारांगसूत्र है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आचारांगसूत्र आगमों में जैन आचार को प्रस्तुत करने वाला सबसे प्राचीन अंग आगम है । ग्रन्थ के प्रथम श्रुत स्कन्ध में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है "समता ही धर्म है ।"" चौथे अध्ययन के प्रथम उद्देश्य में अहिंसा को शाश्वत, नित्य और शुद्ध धर्म कहा गया है । वस्तुतः धर्म असंदीपन द्वीप की भाँति है । जिस प्रकार असंदीपन ( जल में नहीं डूबा हुआ) द्वीप जलपोत यात्रियों के लिए आश्वासन स्थान होता है उसी प्रकार आर्य द्वारा उपदिष्ट धर्म संसार समुद्र पार करने वालों के लिए आश्वासन स्थान होता है । ७
८
उपर्युक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि धर्म-अधर्म की चर्चा आचरण के रूप में हुई है, जो प्रचलित धर्म के सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से अभिन्न है । किन्तु आचारांग के द्वितीय अध्ययन में लोक की चर्चा करते हुए उसके तीन भाग बताये गये हैं- अधोभाग, ऊर्ध्वभाग और तिर्यग्भाग, जो परोक्ष रूप से धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय की अवधारणा को ध्वनित करते हैं। इसकी चर्चा पं० दलसुख भाई मालवणिया ने भी की है। उन्होंने लिखा है- आचारांग के द्वितीय अध्ययन का नाम ही 'लोगविजय' है तथा पाँचवें अध्ययन का नाम लोगसार है और उसके बीच तिर्यग् लोक में मनुष्य रहता है यह मान्यता भी स्थिर हो गयी थी। साथ ही तीनों लोकों के तीनों भागों में जाने का निर्देश है, लोक के अलावा अलोक की कल्पना भी देखी जाती है । किन्तु लोक के अग्रभाग में लोक- अलोक के सन्धिस्थल में सिद्धि स्थान था, ऐसा कोई विचार आचारांग में दिखता नहीं ।' पासिमं दविए लोकालोक पवंचाओ मुच्चई ' ( आचारांग १२० ) अर्थात् देखो कि यह योग्य पुरुष लोक और अलोक के प्रपंच से मुक्त हो जाता है । ऐसा आचारांग में निर्देश है। इससे स्पष्ट है कि आगे चलकर जो लोक - अलोक की परिभाषा स्थिर हुई वह आचारांग में नहीं दिखती।
I
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org