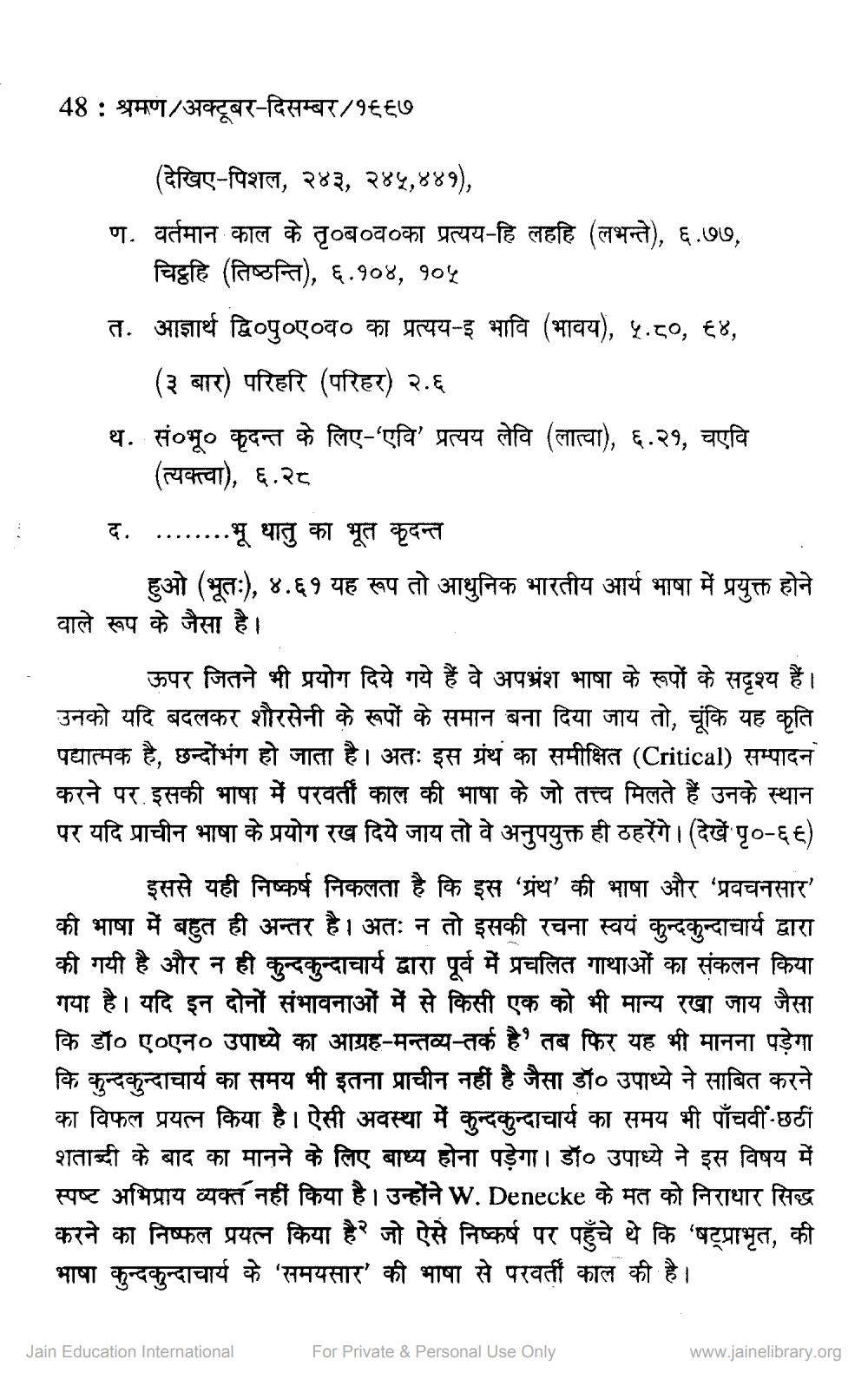________________
48 : श्रमण / अक्टूबर-दिसम्बर / १६६७
(देखिए - पिशल, २४३, २४५, ४४१),
ण. वर्तमान काल के तृ०ब०व०का प्रत्यय - हि लहहि ( लभन्ते), ६.७७, चिट्ठहि ( तिष्ठन्ति ), ६.१०४, १०५
त. आज्ञार्थ द्वि०पु०ए०व० का प्रत्यय - इ भावि ( भावय), ५.८०, ६४, ( ३ बार ) परिहरि ( परिहर) २.६
थ. सं०भू० कृदन्त के लिए - 'एवि' प्रत्यय लेवि ( लात्वा ), ६.२१, चएवि ( त्यक्त्वा ), ६.२८
भू धातु का भूत कृदन्त
हुओ (भूतः ), ४.६१ यह रूप तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में प्रयुक्त होने वाले रूप के जैसा है ।
द.
I
ऊपर जितने भी प्रयोग दिये गये हैं वे अपभ्रंश भाषा के रूपों के सदृश्य हैं उनको यदि बदलकर शौरसेनी के रूपों के समान बना दिया जाय तो, चूंकि यह कृति पद्यात्मक है, छन्दोंभंग हो जाता है। अतः इस ग्रंथ का समीक्षित (Critical) सम्पादन करने पर इसकी भाषा में परवर्ती काल की भाषा के जो तत्त्व मिलते हैं उनके स्थान पर यदि प्राचीन भाषा के प्रयोग रख दिये जाय तो वे अनुपयुक्त ही ठहरेंगे। (देखें पृ०-६६ )
इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि इस 'ग्रंथ' की भाषा और 'प्रवचनसार' की भाषा में बहुत ही अन्तर है । अतः न तो इसकी रचना स्वयं कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा की गयी है और न ही कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा पूर्व में प्रचलित गाथाओं का संकलन किया गया है । यदि इन दोनों संभावनाओं में से किसी एक को भी मान्य रखा जाय जैसा कि डॉ० ए०एन० उपाध्ये का आग्रह - मन्तव्य तर्क है' तब फिर यह भी मानना पड़ेगा कि कुन्दकुन्दाचार्य का समय भी इतना प्राचीन नहीं है जैसा डॉ० उपाध्ये ने साबित करने का विफल प्रयत्न किया है। ऐसी अवस्था में कुन्दकुन्दाचार्य का समय भी पाँचवीं - छठीं शताब्दी के बाद का मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। डॉ० उपाध्ये ने इस विषय में स्पष्ट अभिप्राय व्यक्त नहीं किया है। उन्होंने W. Denecke के मत को निराधार सिद्ध करने का निष्फल प्रयत्न किया है जो ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि 'षट्प्राभृत, की भाषा कुन्दकुन्दाचार्य के 'समयसार' की भाषा से परवर्ती काल की है
1
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org