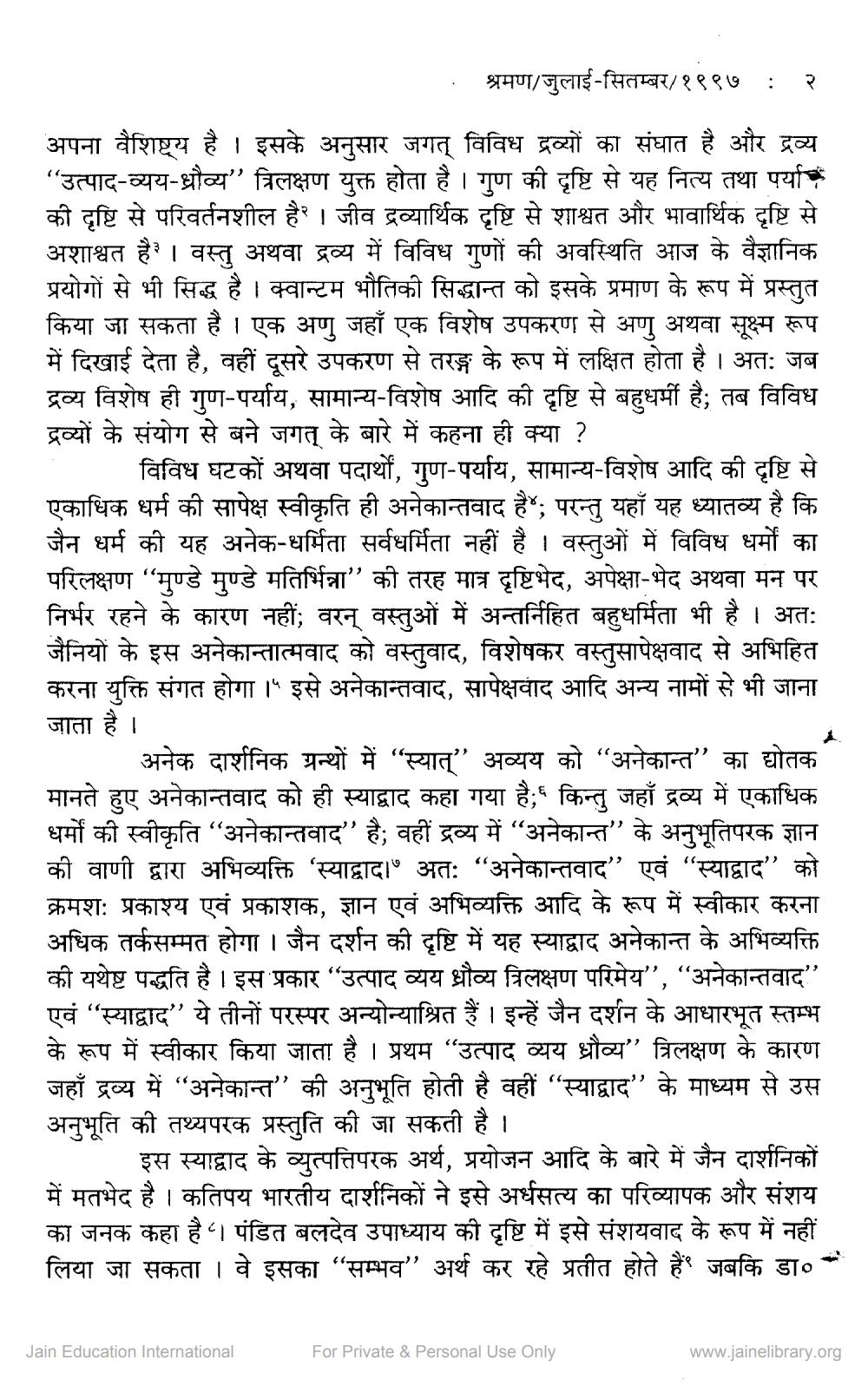________________
.. श्रमण/जुलाई-सितम्बर/१९९७ : २
अपना वैशिष्ट्य है । इसके अनुसार जगत् विविध द्रव्यों का संघात है और द्रव्य "उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य' त्रिलक्षण युक्त होता है । गुण की दृष्टि से यह नित्य तथा पर्याय की दृष्टि से परिवर्तनशील है । जीव द्रव्यार्थिक दृष्टि से शाश्वत और भावार्थिक दृष्टि से अशाश्वत है । वस्तु अथवा द्रव्य में विविध गुणों की अवस्थिति आज के वैज्ञानिक प्रयोगों से भी सिद्ध है। क्वान्टम भौतिकी सिद्धान्त को इसके प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है । एक अणु जहाँ एक विशेष उपकरण से अणु अथवा सूक्ष्म रूप में दिखाई देता है, वहीं दूसरे उपकरण से तरङ्ग के रूप में लक्षित होता है । अत: जब द्रव्य विशेष ही गुण-पर्याय, सामान्य-विशेष आदि की दृष्टि से बहुधर्मी है; तब विविध द्रव्यों के संयोग से बने जगत् के बारे में कहना ही क्या ?
_ विविध घटकों अथवा पदार्थों, गुण-पर्याय, सामान्य-विशेष आदि की दृष्टि से एकाधिक धर्म की सापेक्ष स्वीकृति ही अनेकान्तवाद है; परन्तु यहाँ यह ध्यातव्य है कि जैन धर्म की यह अनेक-धर्मिता सर्वधर्मिता नहीं है । वस्तुओं में विविध धर्मों का परिलक्षण "मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना" की तरह मात्र दृष्टिभेद, अपेक्षा-भेद अथवा मन पर निर्भर रहने के कारण नहीं; वरन् वस्तुओं में अन्तर्निहित बहुधर्मिता भी है । अत: जैनियों के इस अनेकान्तात्मवाद को वस्तुवाद, विशेषकर वस्तुसापेक्षवाद से अभिहित करना युक्ति संगत होगा ।" इसे अनेकान्तवाद, सापेक्षवाद आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है।
अनेक दार्शनिक ग्रन्थों में “स्यात्' अव्यय को “अनेकान्त' का द्योतक मानते हुए अनेकान्तवाद को ही स्याद्वाद कहा गया है; किन्तु जहाँ द्रव्य में एकाधिक धर्मों की स्वीकृति “अनेकान्तवाद' है; वहीं द्रव्य में “अनेकान्त'' के अनुभूतिपरक ज्ञान की वाणी द्वारा अभिव्यक्ति ‘स्याद्वाद। अत: “अनेकान्तवाद” एवं “स्याद्वाद" को क्रमश: प्रकाश्य एवं प्रकाशक, ज्ञान एवं अभिव्यक्ति आदि के रूप में स्वीकार करना अधिक तर्कसम्मत होगा । जैन दर्शन की दृष्टि में यह स्याद्वाद अनेकान्त के अभिव्यक्ति की यथेष्ट पद्धति है। इस प्रकार “उत्पाद व्यय ध्रौव्य विलक्षण परिमेय”, “अनेकान्तवाद" एवं “स्याद्वाद'' ये तीनों परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। इन्हें जैन दर्शन के आधारभूत स्तम्भ के रूप में स्वीकार किया जाता है । प्रथम "उत्पाद व्यय ध्रौव्य' त्रिलक्षण के कारण जहाँ द्रव्य में “अनेकान्त'' की अनुभूति होती है वहीं “स्याद्वाद' के माध्यम से उस अनुभूति की तथ्यपरक प्रस्तुति की जा सकती है।
इस स्याद्वाद के व्युत्पत्तिपरक अर्थ, प्रयोजन आदि के बारे में जैन दार्शनिकों में मतभेद है । कतिपय भारतीय दार्शनिकों ने इसे अर्धसत्य का परिव्यापक और संशय का जनक कहा है । पंडित बलदेव उपाध्याय की दृष्टि में इसे संशयवाद के रूप में नहीं लिया जा सकता । वे इसका “सम्भव' अर्थ कर रहे प्रतीत होते हैं जबकि डा०*
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org