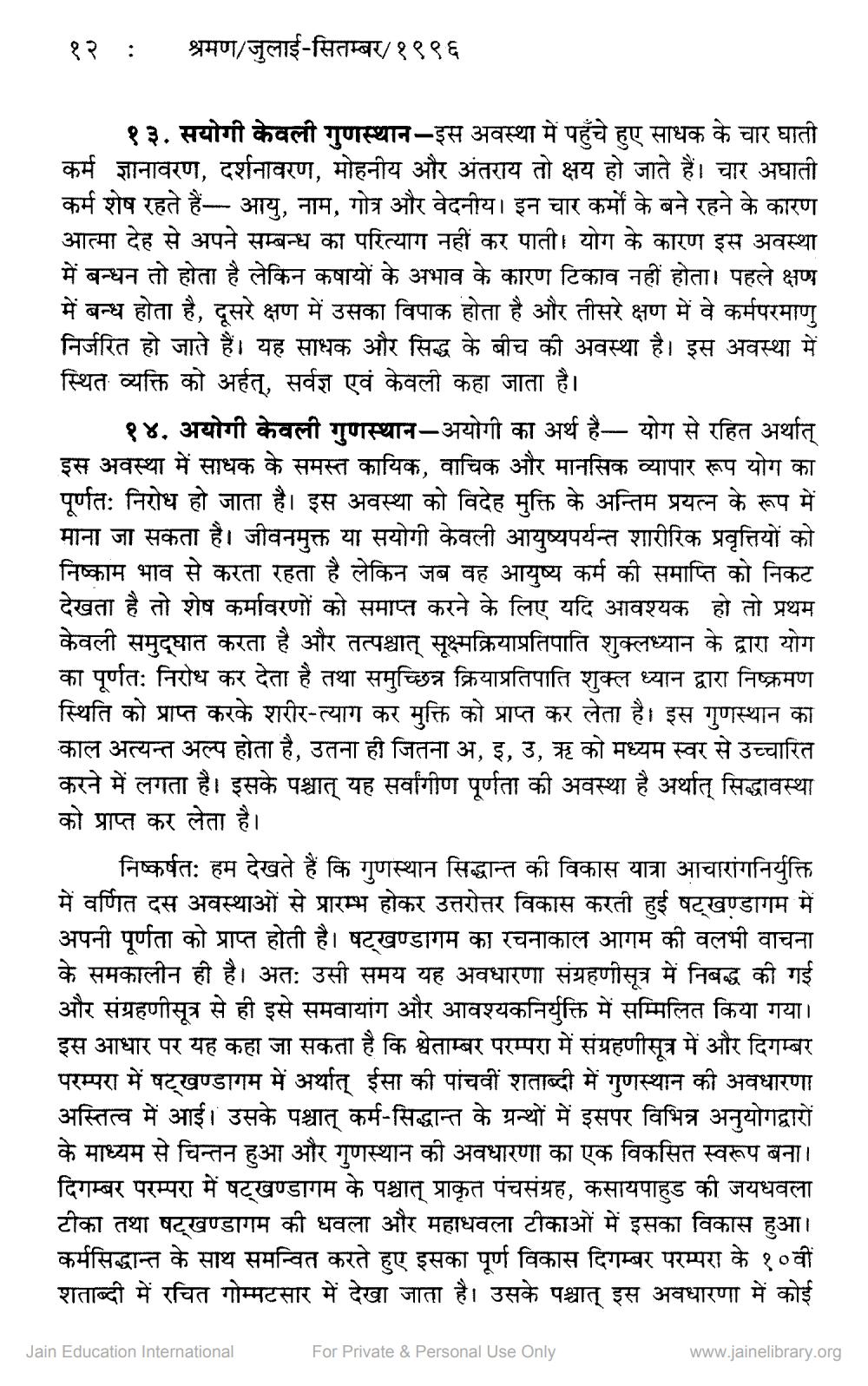________________
१२ :
श्रमण/जुलाई-सितम्बर/१९९६
१३. सयोगी केवली गुणस्थान-इस अवस्था में पहुँचे हुए साधक के चार घाती कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय तो क्षय हो जाते हैं। चार अघाती कर्म शेष रहते हैं- आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। इन चार कर्मों के बने रहने के कारण आत्मा देह से अपने सम्बन्ध का परित्याग नहीं कर पाती। योग के कारण इस अवस्था में बन्धन तो होता है लेकिन कषायों के अभाव के कारण टिकाव नहीं होता। पहले क्षण में बन्ध होता है, दूसरे क्षण में उसका विपाक होता है और तीसरे क्षण में वे कर्मपरमाणु निर्जरित हो जाते हैं। यह साधक और सिद्ध के बीच की अवस्था है। इस अवस्था में स्थित व्यक्ति को अर्हत्, सर्वज्ञ एवं केवली कहा जाता है।
१४. अयोगी केवली गुणस्थान-अयोगी का अर्थ है- योग से रहित अर्थात् इस अवस्था में साधक के समस्त कायिक, वाचिक और मानसिक व्यापार रूप योग का पूर्णत: निरोध हो जाता है। इस अवस्था को विदेह मुक्ति के अन्तिम प्रयत्न के रूप में माना जा सकता है। जीवनमुक्त या सयोगी केवली आयुष्यपर्यन्त शारीरिक प्रवृत्तियों को निष्काम भाव से करता रहता है लेकिन जब वह आयुष्य कर्म की समाप्ति को निकट देखता है तो शेष कर्मावरणों को समाप्त करने के लिए यदि आवश्यक हो तो प्रथम केवली समुद्घात करता है और तत्पश्चात् सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति शुक्लध्यान के द्वारा योग का पूर्णत: निरोध कर देता है तथा समुच्छिन्न क्रियाप्रतिपाति शुक्ल ध्यान द्वारा निष्क्रमण स्थिति को प्राप्त करके शरीर-त्याग कर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस गुणस्थान का काल अत्यन्त अल्प होता है, उतना ही जितना अ, इ, उ, ऋ को मध्यम स्वर से उच्चारित करने में लगता है। इसके पश्चात् यह सर्वांगीण पूर्णता की अवस्था है अर्थात् सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। ___ निष्कर्षत: हम देखते हैं कि गुणस्थान सिद्धान्त की विकास यात्रा आचारांगनियुक्ति में वर्णित दस अवस्थाओं से प्रारम्भ होकर उत्तरोत्तर विकास करती हुई षट्खण्डागम में अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है। षट्खण्डागम का रचनाकाल आगम की वलभी वाचना के समकालीन ही है। अत: उसी समय यह अवधारणा संग्रहणीसूत्र में निबद्ध की गई और संग्रहणीसूत्र से ही इसे समवायांग और आवश्यकनियुक्ति में सम्मिलित किया गया। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि श्वेताम्बर परम्परा में संग्रहणीसूत्र में और दिगम्बर परम्परा में षटखण्डागम में अर्थात् ईसा की पांचवीं शताब्दी में गुणस्थान की अवधारणा अस्तित्व में आई। उसके पश्चात् कर्म-सिद्धान्त के ग्रन्थों में इसपर विभिन्न अनुयोगद्वारों के माध्यम से चिन्तन हुआ और गुणस्थान की अवधारणा का एक विकसित स्वरूप बना। दिगम्बर परम्परा में षट्खण्डागम के पश्चात् प्राकृत पंचसंग्रह, कसायपाहुड की जयधवला टीका तथा षटखण्डागम की धवला और महाधवला टीकाओं में इसका विकास हुआ। कर्मसिद्धान्त के साथ समन्वित करते हुए इसका पूर्ण विकास दिगम्बर परम्परा के १०वीं शताब्दी में रचित गोम्मटसार में देखा जाता है। उसके पश्चात् इस अवधारणा में कोई
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org