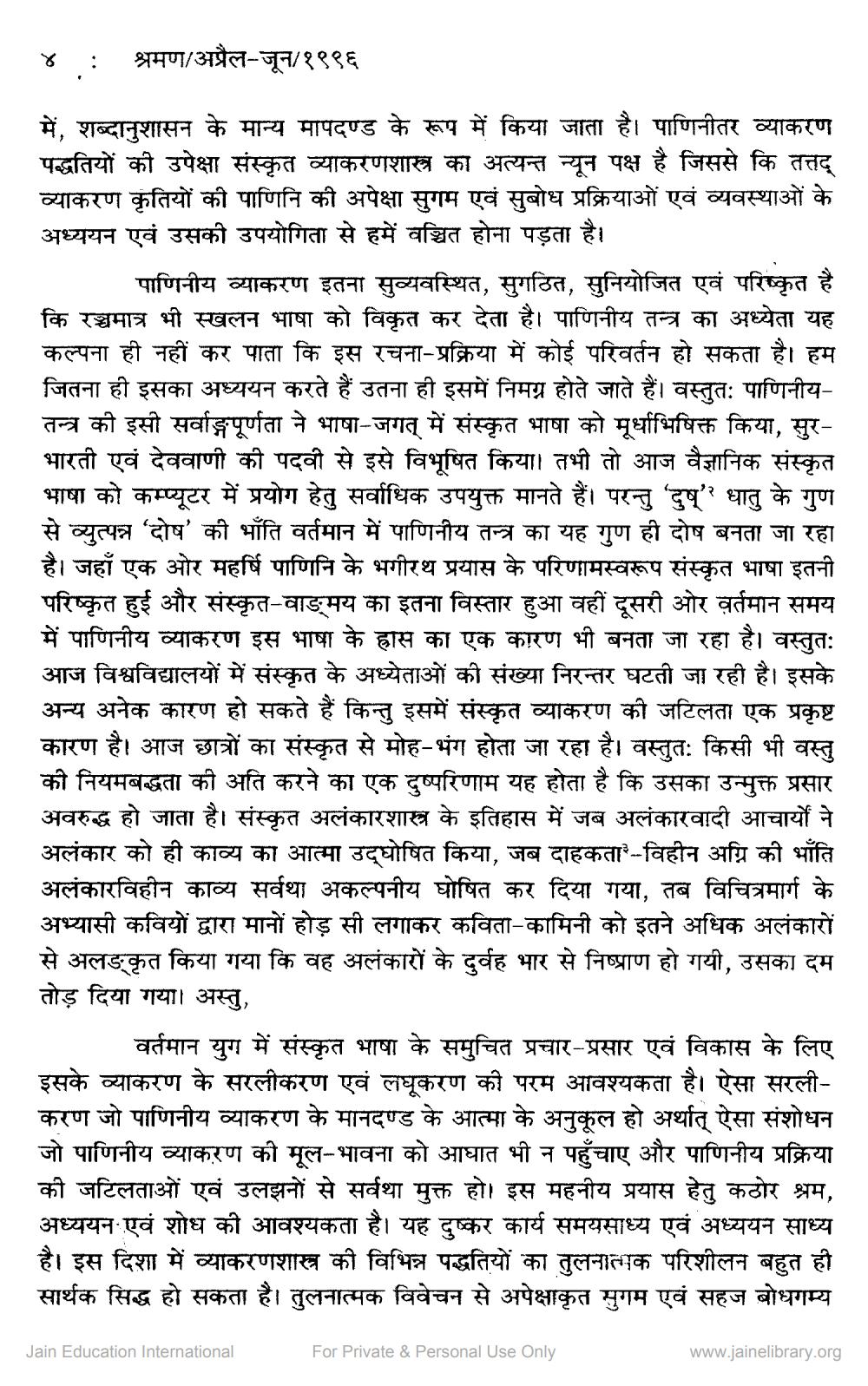________________
४ :
श्रमण/अप्रैल-जून/१९९६
में, शब्दानुशासन के मान्य मापदण्ड के रूप में किया जाता है। पाणिनीतर व्याकरण पद्धतियों की उपेक्षा संस्कृत व्याकरणशास्त्र का अत्यन्त न्यून पक्ष है जिससे कि तत्तद् व्याकरण कृतियों की पाणिनि की अपेक्षा सुगम एवं सुबोध प्रक्रियाओं एवं व्यवस्थाओं के अध्ययन एवं उसकी उपयोगिता से हमें वञ्चित होना पड़ता है।
पाणिनीय व्याकरण इतना सुव्यवस्थित, सुगठित, सुनियोजित एवं परिष्कृत है कि रञ्चमात्र भी स्खलन भाषा को विकृत कर देता है। पाणिनीय तन्त्र का अध्येता यह कल्पना ही नहीं कर पाता कि इस रचना-प्रक्रिया में कोई परिवर्तन हो सकता है। हम जितना ही इसका अध्ययन करते हैं उतना ही इसमें निमग्न होते जाते हैं। वस्तुतः पाणिनीयतन्त्र की इसी सर्वाङ्गपूर्णता ने भाषा-जगत् में संस्कृत भाषा को मूर्धाभिषिक्त किया, सुरभारती एवं देववाणी की पदवी से इसे विभूषित किया। तभी तो आज वैज्ञानिक संस्कृत भाषा को कम्प्यूटर में प्रयोग हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं। परन्तु ‘दुष्' धातु के गुण से व्युत्पन्न 'दोष' की भाँति वर्तमान में पाणिनीय तन्त्र का यह गुण ही दोष बनता जा रहा है। जहाँ एक ओर महर्षि पाणिनि के भगीरथ प्रयास के परिणामस्वरूप संस्कृत भाषा इतनी परिष्कृत हुई और संस्कृत-वाङ्मय का इतना विस्तार हुआ वहीं दूसरी ओर वर्तमान समय में पाणिनीय व्याकरण इस भाषा के ह्रास का एक कारण भी बनता जा रहा है। वस्तुत: आज विश्वविद्यालयों में संस्कृत के अध्येताओं की संख्या निरन्तर घटती जा रही है। इसके अन्य अनेक कारण हो सकते हैं किन्तु इसमें संस्कृत व्याकरण की जटिलता एक प्रकृष्ट कारण है। आज छात्रों का संस्कृत से मोह-भंग होता जा रहा है। वस्तुत: किसी भी वस्तु की नियमबद्धता की अति करने का एक दुष्परिणाम यह होता है कि उसका उन्मुक्त प्रसार अवरुद्ध हो जाता है। संस्कृत अलंकारशास्त्र के इतिहास में जब अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकार को ही काव्य का आत्मा उद्घोषित किया, जब दाहकता-विहीन अग्नि की भाँति अलंकारविहीन काव्य सर्वथा अकल्पनीय घोषित कर दिया गया, तब विचित्रमार्ग के अभ्यासी कवियों द्वारा मानों होड़ सी लगाकर कविता-कामिनी को इतने अधिक अलंकारों से अलङ्कृत किया गया कि वह अलंकारों के दुर्वह भार से निष्प्राण हो गयी, उसका दम तोड़ दिया गया। अस्तु,
वर्तमान युग में संस्कृत भाषा के समुचित प्रचार-प्रसार एवं विकास के लिए इसके व्याकरण के सरलीकरण एवं लघुकरण की परम आवश्यकता है। ऐसा सरलीकरण जो पाणिनीय व्याकरण के मानदण्ड के आत्मा के अनुकूल हो अर्थात् ऐसा संशोधन जो पाणिनीय व्याकरण की मूल-भावना को आघात भी न पहुँचाए और पाणिनीय प्रक्रिया की जटिलताओं एवं उलझनों से सर्वथा मुक्त हो। इस महनीय प्रयास हेतु कठोर श्रम, अध्ययन एवं शोध की आवश्यकता है। यह दुष्कर कार्य समयसाध्य एवं अध्ययन साध्य है। इस दिशा में व्याकरणशास्त्र की विभिन्न पद्धतियों का तुलनात्मक परिशीलन बहुत ही सार्थक सिद्ध हो सकता है। तुलनात्मक विवेचन से अपेक्षाकृत सुगम एवं सहज बोधगम्य
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org