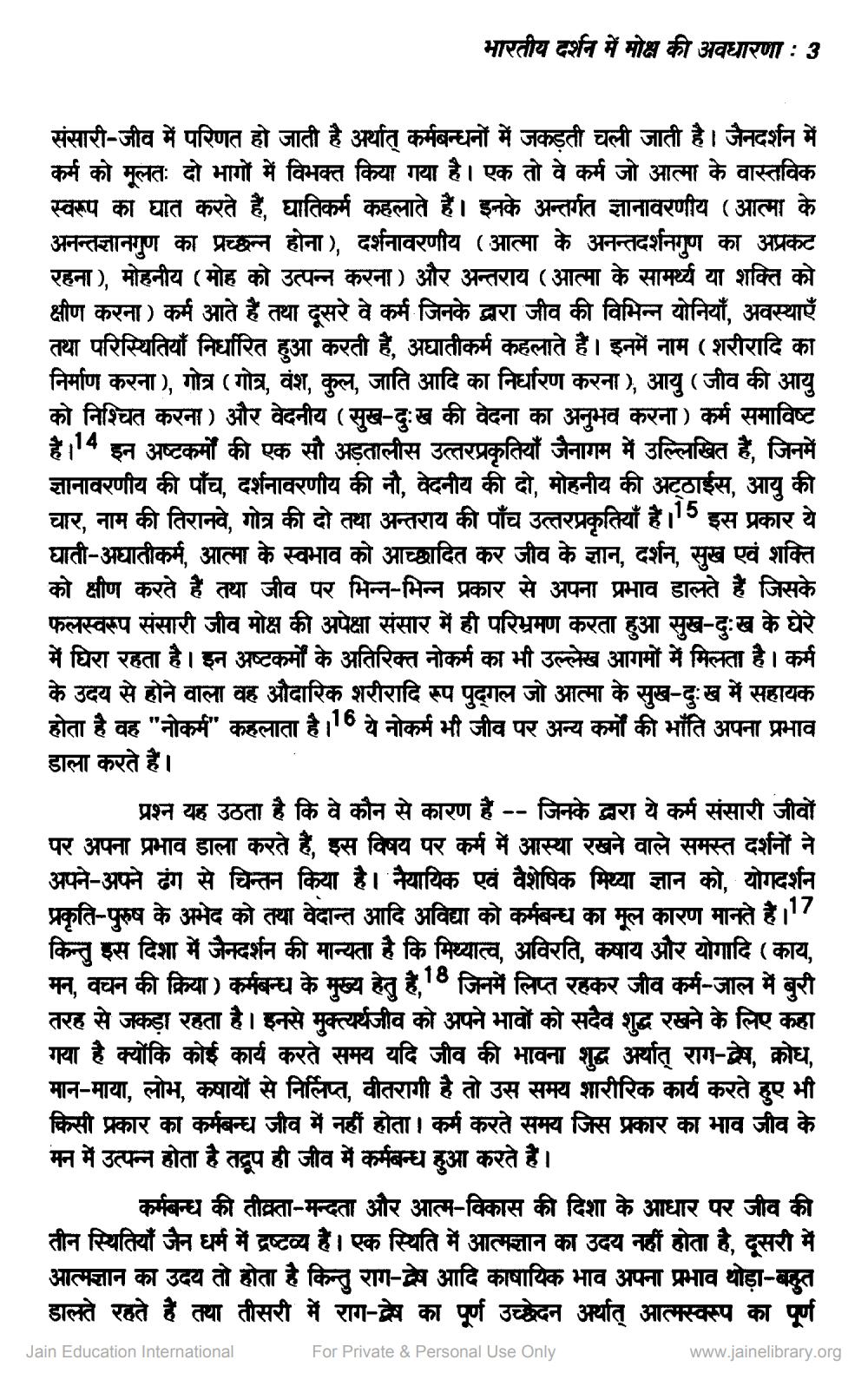________________
भारतीय दर्शन में मोक्ष की अवधारणा : 3
संसारी-जीव में परिणत हो जाती है अर्थात कर्मबन्धनों में जकडती चली जाती है। जैनदर्शन में कर्म को मूलतः दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो वे कर्म जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप का घात करते हैं, घातिकर्म कहलाते हैं। इनके अन्तर्गत ज्ञानावरणीय (आत्मा के अनन्तज्ञानगुण का प्रच्छन्न होना), दर्शनावरणीय (आत्मा के अनन्तदर्शनगुण का अप्रकट रहना), मोहनीय (मोह को उत्पन्न करना) और अन्तराय (आत्मा के सामर्थ्य या शक्ति को क्षीण करना) कर्म आते हैं तथा दूसरे वे कर्म जिनके द्वारा जीव की विभिन्न योनियाँ, अवस्थाएँ तथा परिस्थितियाँ निर्धारित हुआ करती हैं, अघातीकर्म कहलाते हैं। इनमें नाम (शरीरादि का निर्माण करना), गोत्र (गोत्र, वंश, कुल, जाति आदि का निर्धारण करना), आयु (जीव की आयु को निश्चित करना) और वेदनीय (सुख-दुःख की वेदना का अनुभव करना) कर्म समाविष्ट है।14 इन अष्टकर्मों की एक सौ अड़तालीस उत्तरप्रकृतियों जैनागम में उल्लिखित हैं, जिनमें ज्ञानावरणीय की पाँच, दर्शनावरणीय की नौ, वेदनीय की दो, मोहनीय की अट्ठाईस, आयु की चार, नाम की तिरानवे, गोत्र की दो तथा अन्तराय की पाँच उत्तरप्रकृतियाँ हैं। इस प्रकार ये घाती-अघातीकर्म, आत्मा के स्वभाव को आच्छादित कर जीव के ज्ञान, दर्शन, सुख एवं शक्ति को क्षीण करते हैं तथा जीव पर भिन्न-भिन्न प्रकार से अपना प्रभाव डालते है जिसके फलस्वरूप संसारी जीव मोक्ष की अपेक्षा संसार में ही परिभ्रमण करता हुआ सुख-दुःख के घेरे में घिरा रहता है। इन अष्टकर्मों के अतिरिक्त नोकर्म का भी उल्लेख आगमों में मिलता है। कर्म के उदय से होने वाला वह औदारिक शरीरादि स्प पुद्गल जो आत्मा के सुख-दुःख में सहायक होता है वह "नोकर्म" कहलाता है। ये नोकर्म भी जीव पर अन्य कर्मों की भाँति अपना प्रभाव डाला करते हैं।
प्रश्न यह उठता है कि वे कौन से कारण है -- जिनके द्वरा ये कर्म संसारी जीवों पर अपना प्रभाव डाला करते हैं, इस विषय पर कर्म में आस्था रखने वाले समस्त दर्शनों ने अपने-अपने ढंग से चिन्तन किया है। नैयायिक एवं वैशेषिक मिथ्या ज्ञान को, योगदर्शन प्रकृति-पुरुष के अभेद को तथा वेदान्त आदि अविद्या को कर्मबन्ध का मूल कारण मानते हैं।17 किन्तु इस दिशा में जैनदर्शन की मान्यता है कि मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगादि (काय, मन, वचन की क्रिया) कर्मबन्ध के मुख्य हेतु है, जिनमें लिप्त रहकर जीव कर्म-जाल में बुरी तरह से जकड़ा रहता है। इनसे मुक्त्यर्थजीव को अपने भावों को सदैव शुद्ध रखने के लिए कहा गया है क्योंकि कोई कार्य करते समय यदि जीव की भावना शुद्ध अर्थात् राग-द्वेष, क्रोध, मान-माया, लोभ, कषायों से निर्लिप्त, वीतरागी है तो उस समय शारीरिक कार्य करते हुए भी किसी प्रकार का कर्मबन्ध जीव में नहीं होता। कर्म करते समय जिस प्रकार का भाव जीव के मन में उत्पन्न होता है तद्रप ही जीव में कर्मबन्ध हुआ करते हैं।
कर्मबन्ध की तीव्रता-मन्दता और आत्म-विकास की दिशा के आधार पर जीव की तीन स्थितियों जैन धर्म में द्रष्टव्य है। एक स्थिति में आत्मज्ञान का उदय नहीं होता है, दूसरी में आत्मज्ञान का उदय तो होता है किन्तु राग-दो आदि काषायिक भाव अपना प्रभाव थोड़ा-बहुत डालते रहते हैं तथा तीसरी में राग-२ का पूर्ण उच्छेदन अर्थात् आत्मस्वरूप का पूर्ण Jain Education International For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org