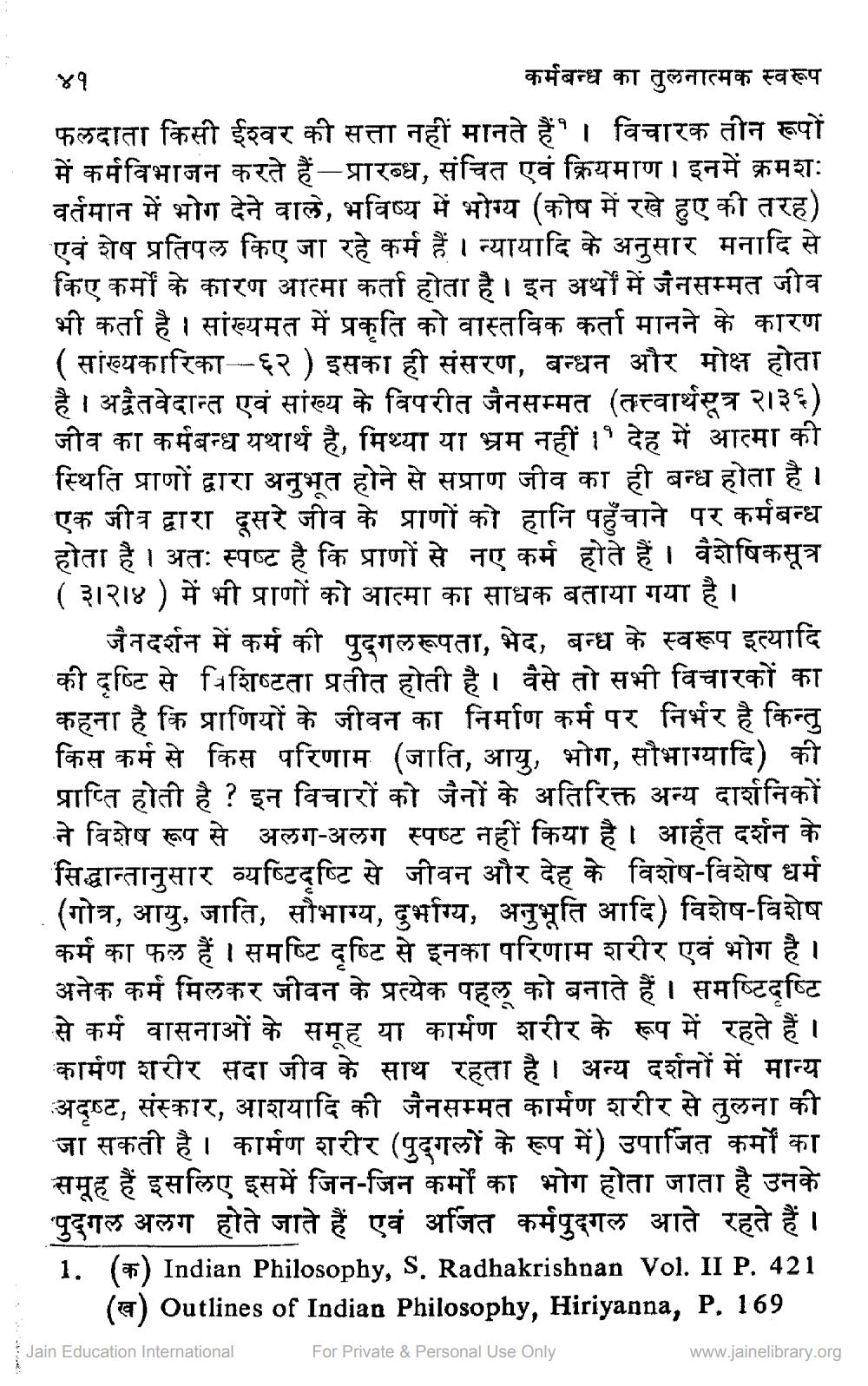________________
४१
कर्मबन्ध का तुलनात्मक स्वरूप फलदाता किसी ईश्वर की सत्ता नहीं मानते हैं। विचारक तीन रूपों में कर्मविभाजन करते हैं प्रारब्ध, संचित एवं क्रियमाण । इनमें क्रमशः वर्तमान में भोग देने वाले, भविष्य में भोग्य (कोष में रखे हुए की तरह) एवं शेष प्रतिपल किए जा रहे कर्म हैं । न्यायादि के अनुसार मनादि से किए कर्मों के कारण आत्मा कर्ता होता है। इन अर्थों में जैनसम्मत जीव भी कर्ता है। सांख्यमत में प्रकृति को वास्तविक कर्ता मानने के कारण ( सांख्यकारिका-६२ ) इसका ही संसरण, बन्धन और मोक्ष होता है। अद्वैतवेदान्त एवं सांख्य के विपरीत जैनसम्मत (तत्त्वार्थसूत्र २।३६) जीव का कर्मबन्ध यथार्थ है, मिथ्या या भ्रम नहीं। देह में आत्मा की स्थिति प्राणों द्वारा अनुभूत होने से सप्राण जीव का ही बन्ध होता है। एक जीव द्वारा दूसरे जीव के प्राणों को हानि पहुँचाने पर कर्मबन्ध होता है। अतः स्पष्ट है कि प्राणों से नए कर्म होते हैं। वैशेषिकसूत्र ( ३।२।४ ) में भी प्राणों को आत्मा का साधक बताया गया है ।
जैनदर्शन में कर्म की पुद्गलरूपता, भेद, बन्ध के स्वरूप इत्यादि की दृष्टि से विशिष्टता प्रतीत होती है। वैसे तो सभी विचारकों का कहना है कि प्राणियों के जीवन का निर्माण कर्म पर निर्भर है किन्तु किस कर्म से किस परिणाम (जाति, आयु, भोग, सौभाग्यादि) की प्राप्ति होती है ? इन विचारों को जैनों के अतिरिक्त अन्य दार्शनिकों ने विशेष रूप से अलग-अलग स्पष्ट नहीं किया है। आर्हत दर्शन के सिद्धान्तानुसार व्यष्टिदृष्टि से जीवन और देह के विशेष-विशेष धर्म (गोत्र, आयु, जाति, सौभाग्य, दुर्भाग्य, अनुभूति आदि) विशेष-विशेष कर्म का फल हैं । समष्टि दृष्टि से इनका परिणाम शरीर एवं भोग है। अनेक कर्म मिलकर जीवन के प्रत्येक पहल को बनाते हैं। समष्टिदृष्टि से कर्म वासनाओं के समूह या कार्मण शरीर के रूप में रहते हैं। कार्मण शरीर सदा जीव के साथ रहता है। अन्य दर्शनों में मान्य अदृष्ट, संस्कार, आशयादि की जैनसम्मत कार्मण शरीर से तुलना की जा सकती है। कार्मण शरीर (पुद्गलों के रूप में) उपार्जित कर्मों का समूह हैं इसलिए इसमें जिन-जिन कर्मों का भोग होता जाता है उनके 'पुद्गल अलग होते जाते हैं एवं अर्जित कर्मपुद्गल आते रहते हैं । 1. (क) Indian Philosophy, S. Radhakrishnan Vol. II P. 421
(a) Outlines of Indian Philosophy, Hiriyanna, P. 169
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org