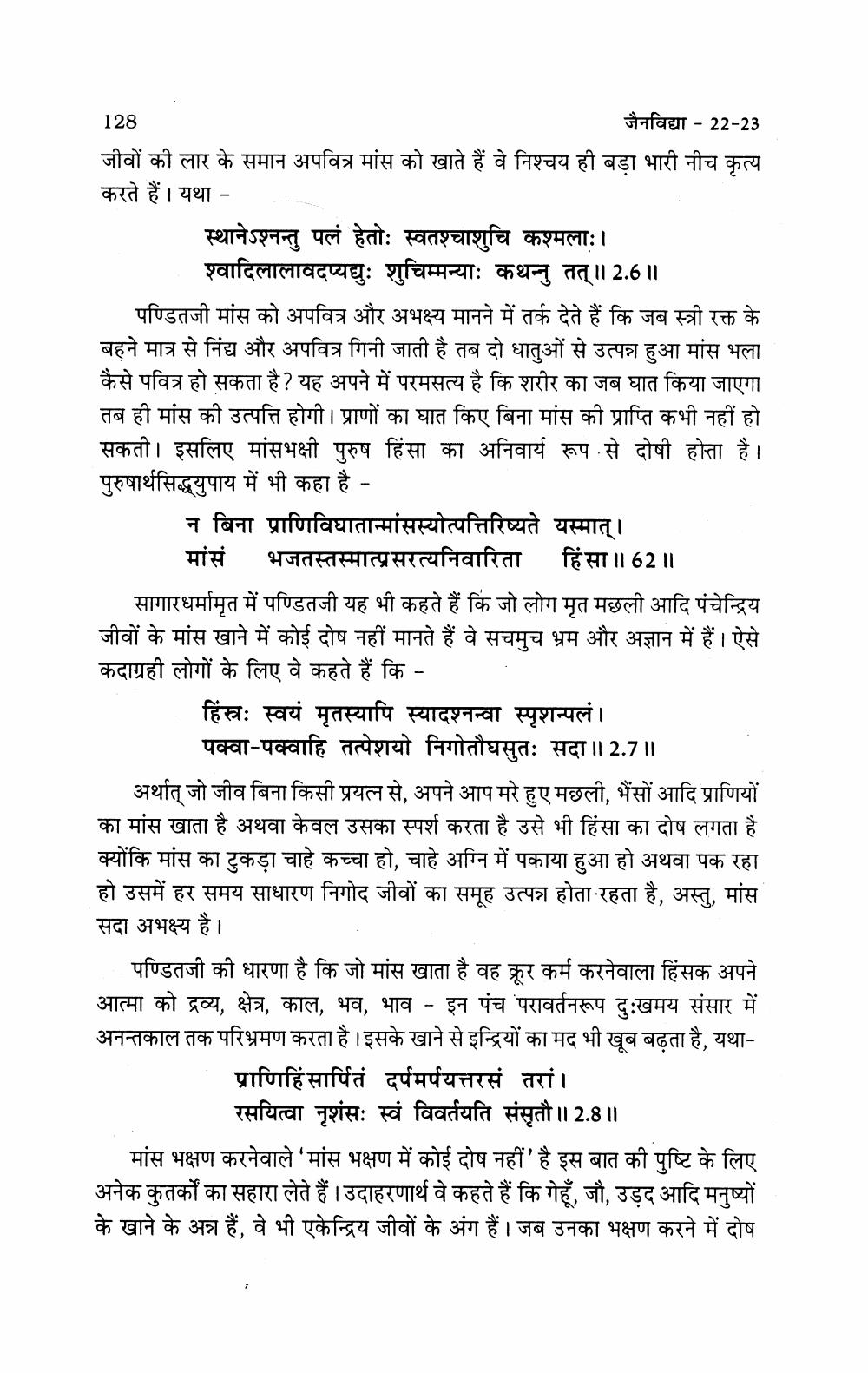________________
128
जैनविद्या - 22-23 जीवों की लार के समान अपवित्र मांस को खाते हैं वे निश्चय ही बड़ा भारी नीच कृत्य करते हैं । यथा -
स्थानेऽश्नन्तु पलं हेतोः स्वतश्चाशुचि कश्मलाः।
श्वादिलालावदप्यधुः शुचिम्मन्याः कथन्नु तत्॥ 2.6॥ पण्डितजी मांस को अपवित्र और अभक्ष्य मानने में तर्क देते हैं कि जब स्त्री रक्त के बहने मात्र से निंद्य और अपवित्र गिनी जाती है तब दो धातुओं से उत्पन्न हुआ मांस भला कैसे पवित्र हो सकता है? यह अपने में परमसत्य है कि शरीर का जब घात किया जाएगा तब ही मांस की उत्पत्ति होगी। प्राणों का घात किए बिना मांस की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए मांसभक्षी पुरुष हिंसा का अनिवार्य रूप से दोषी होता है। पुरुषार्थसिद्धयुपाय में भी कहा है -
न बिना प्राणिविघातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात्।
मांसं भजतस्तस्मात्प्रसरत्यनिवारिता हिंसा॥ 62 ॥ सागारधर्मामृत में पण्डितजी यह भी कहते हैं कि जो लोग मृत मछली आदि पंचेन्द्रिय जीवों के मांस खाने में कोई दोष नहीं मानते हैं वे सचमुच भ्रम और अज्ञान में हैं। ऐसे कदाग्रही लोगों के लिए वे कहते हैं कि -
हिंस्रः स्वयं मृतस्यापि स्यादश्नन्वा स्पृशन्पलं।
पक्वा-पक्वाहि तत्पेशयो निगोतौघसुतः सदा ॥ 2.7 ॥ अर्थात् जो जीव बिना किसी प्रयत्न से, अपने आप मरे हुए मछली, भैंसों आदि प्राणियों का मांस खाता है अथवा केवल उसका स्पर्श करता है उसे भी हिंसा का दोष लगता है क्योंकि मांस का टुकड़ा चाहे कच्चा हो, चाहे अग्नि में पकाया हुआ हो अथवा पक रहा हो उसमें हर समय साधारण निगोद जीवों का समूह उत्पन्न होता रहता है, अस्तु, मांस सदा अभक्ष्य है।
पण्डितजी की धारणा है कि जो मांस खाता है वह क्रूर कर्म करनेवाला हिंसक अपने आत्मा को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव - इन पंच परावर्तनरूप दुःखमय संसार में अनन्तकाल तक परिभ्रमण करता है । इसके खाने से इन्द्रियों का मद भी खूब बढ़ता है, यथा
प्राणिहिंसार्पितं दर्पमर्पयत्तरसं तरां।
रसयित्वा नृशंसः स्वं विवर्तयति संसृतौ ॥ 2.8॥ मांस भक्षण करनेवाले 'मांस भक्षण में कोई दोष नहीं' है इस बात की पुष्टि के लिए अनेक कुतर्कों का सहारा लेते हैं । उदाहरणार्थ वे कहते हैं कि गेहूँ, जौ, उड़द आदि मनुष्यों के खाने के अन्न हैं, वे भी एकेन्द्रिय जीवों के अंग हैं। जब उनका भक्षण करने में दोष