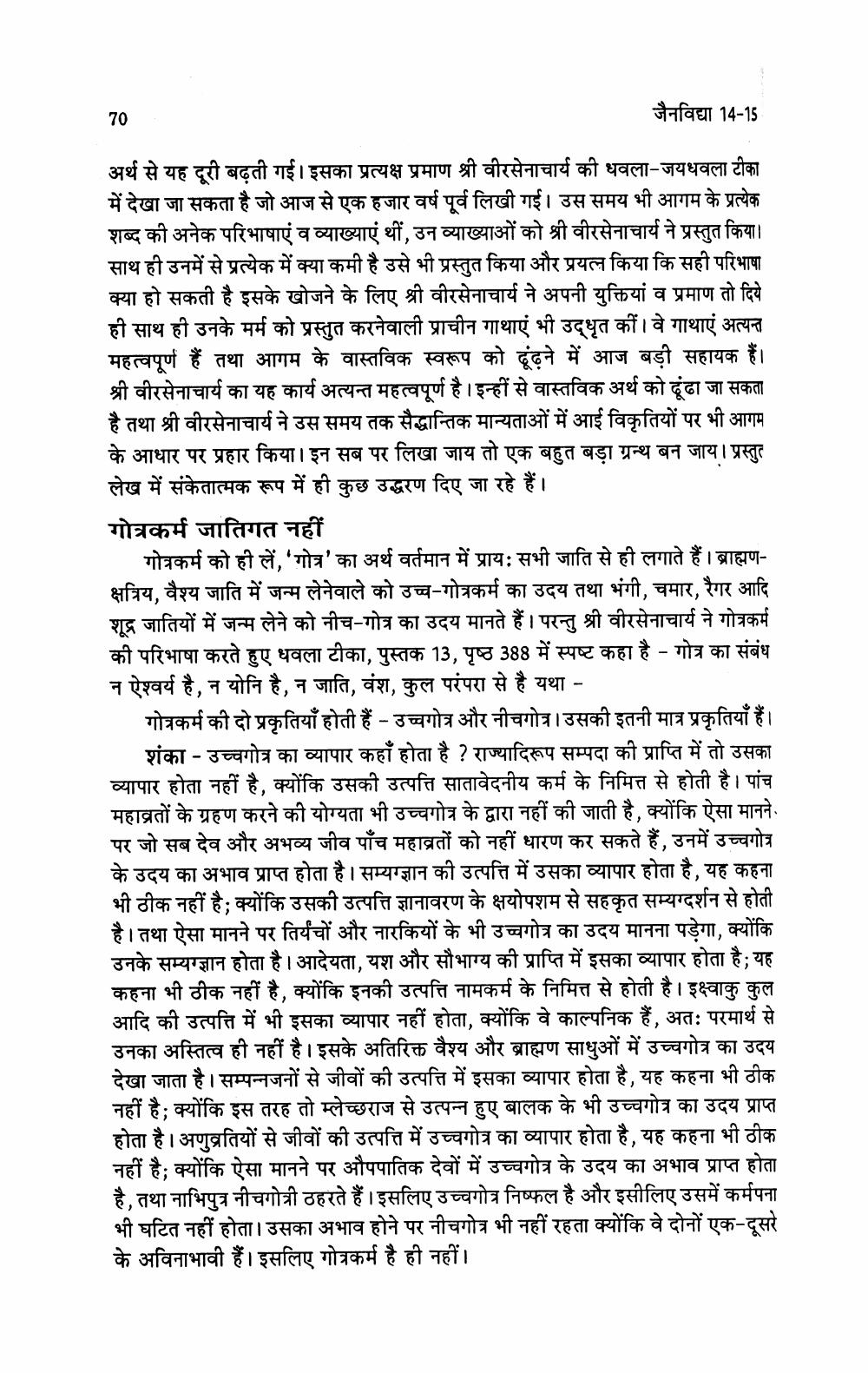________________
70
जैनविद्या 14-15
अर्थ से यह दूरी बढ़ती गई। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण श्री वीरसेनाचार्य की धवला-जयधवला टीका में देखा जा सकता है जो आज से एक हजार वर्ष पूर्व लिखी गई। उस समय भी आगम के प्रत्येक शब्द की अनेक परिभाषाएं व व्याख्याएं थीं, उन व्याख्याओं को श्री वीरसेनाचार्य ने प्रस्तुत किया। साथ ही उनमें से प्रत्येक में क्या कमी है उसे भी प्रस्तुत किया और प्रयत्न किया कि सही परिभाषा क्या हो सकती है इसके खोजने के लिए श्री वीरसेनाचार्य ने अपनी युक्तियां व प्रमाण तो दिये ही साथ ही उनके मर्म को प्रस्तुत करनेवाली प्राचीन गाथाएं भी उद्धृत कीं। वे गाथाएं अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं तथा आगम के वास्तविक स्वरूप को ढूंढने में आज बड़ी सहायक हैं। श्री वीरसेनाचार्य का यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन्हीं से वास्तविक अर्थ को ढूंढा जा सकता है तथा श्री वीरसेनाचार्य ने उस समय तक सैद्धान्तिक मान्यताओं में आई विकृतियों पर भी आगम के आधार पर प्रहार किया। इन सब पर लिखा जाय तो एक बहुत बड़ा ग्रन्थ बन जाय। प्रस्तुत लेख में संकेतात्मक रूप में ही कुछ उद्धरण दिए जा रहे हैं। गोत्रकर्म जातिगत नहीं ___गोत्रकर्म को ही लें, 'गोत्र' का अर्थ वर्तमान में प्रायः सभी जाति से ही लगाते हैं । ब्राह्मणक्षत्रिय, वैश्य जाति में जन्म लेनेवाले को उच्च-गोत्रकर्म का उदय तथा भंगी, चमार, रैगर आदि शूद्र जातियों में जन्म लेने को नीच-गोत्र का उदय मानते हैं। परन्तु श्री वीरसेनाचार्य ने गोत्रकर्म की परिभाषा करते हुए धवला टीका, पुस्तक 13, पृष्ठ 388 में स्पष्ट कहा है - गोत्र का संबंध न ऐश्वर्य है, न योनि है, न जाति, वंश, कुल परंपरा से है यथा -
गोत्रकर्म की दो प्रकृतियाँ होती हैं - उच्चगोत्र और नीचगोत्र । उसकी इतनी मात्र प्रकृतियाँ हैं।
शंका - उच्चगोत्र का व्यापार कहाँ होता है ? राज्यादिरूप सम्पदा की प्राप्ति में तो उसका व्यापार होता नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति सातावेदनीय कर्म के निमित्त से होती है। पांच महाव्रतों के ग्रहण करने की योग्यता भी उच्चगोत्र के द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि ऐसा मानने पर जो सब देव और अभव्य जीव पाँच महाव्रतों को नहीं धारण कर सकते हैं, उनमें उच्चगोत्र के उदय का अभाव प्राप्त होता है। सम्यग्ज्ञान की उत्पत्ति में उसका व्यापार होता है, यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि उसकी उत्पत्ति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से सहकृत सम्यग्दर्शन से होती है। तथा ऐसा मानने पर तिर्यंचों और नारकियों के भी उच्चगोत्र का उदय मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके सम्यग्ज्ञान होता है। आदेयता, यश और सौभाग्य की प्राप्ति में इसका व्यापार होता है; यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति नामकर्म के निमित्त से होती है । इक्ष्वाकु कुल आदि की उत्पत्ति में भी इसका व्यापार नहीं होता, क्योंकि वे काल्पनिक हैं, अतः परमार्थ से उनका अस्तित्व ही नहीं है। इसके अतिरिक्त वैश्य और ब्राह्मण साधुओं में उच्चगोत्र का उदय देखा जाता है। सम्पन्नजनों से जीवों की उत्पत्ति में इसका व्यापार होता है, यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि इस तरह तो म्लेच्छराज से उत्पन्न हुए बालक के भी उच्चगोत्र का उदय प्राप्त होता है। अणुव्रतियों से जीवों की उत्पत्ति में उच्चगोत्र का व्यापार होता है, यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि ऐसा मानने पर औपपातिक देवों में उच्चगोत्र के उदय का अभाव प्राप्त होता है, तथा नाभिपुत्र नीचगोत्री ठहरते हैं। इसलिए उच्चगोत्र निष्फल है और इसीलिए उसमें कर्मपना भी घटित नहीं होता। उसका अभाव होने पर नीचगोत्र भी नहीं रहता क्योंकि वे दोनों एक-दूसरे के अविनाभावी हैं। इसलिए गोत्रकर्म है ही नहीं।