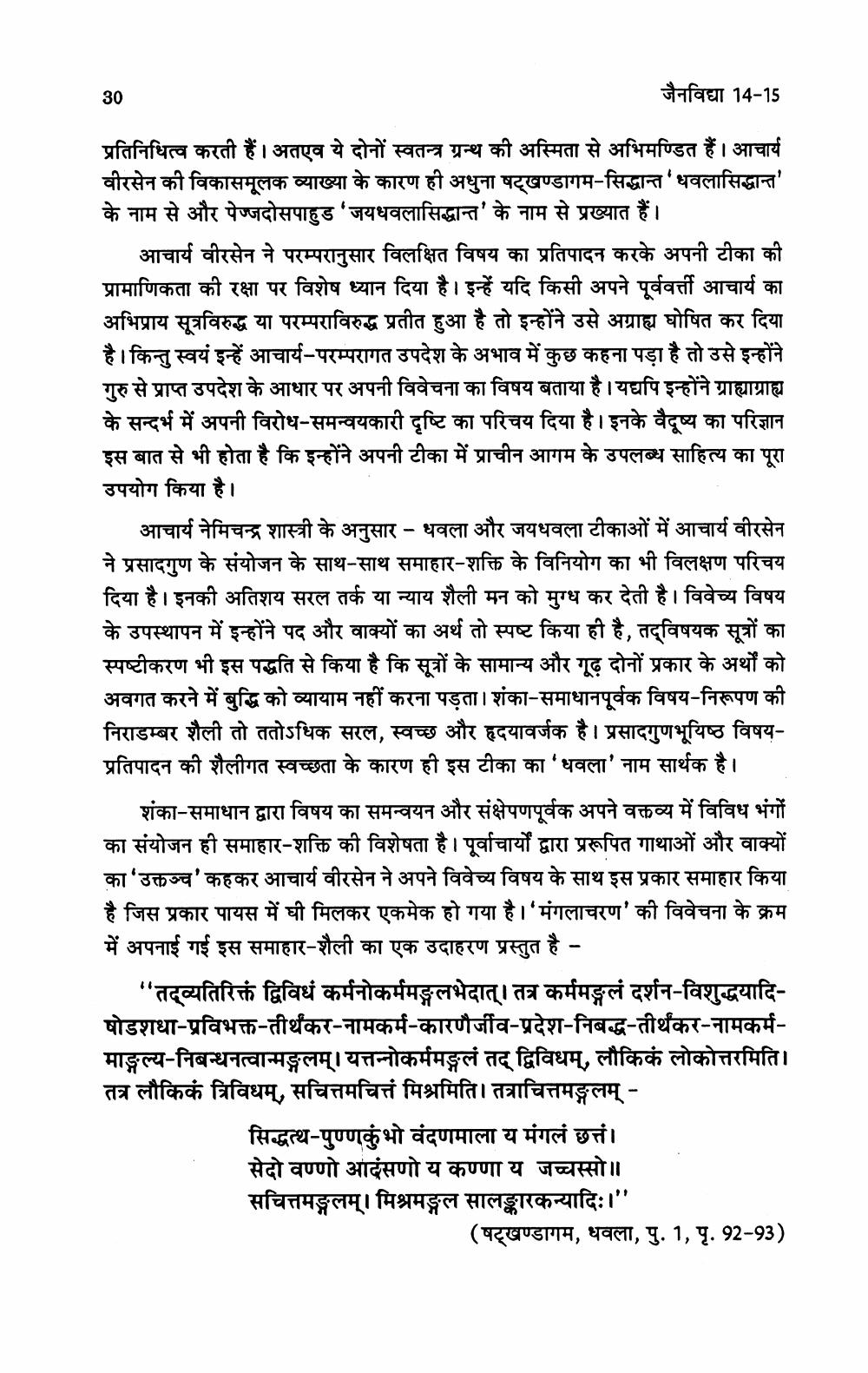________________
30
जैनविद्या 14-15
प्रतिनिधित्व करती हैं। अतएव ये दोनों स्वतन्त्र ग्रन्थ की अस्मिता से अभिमण्डित हैं। आचार्य वीरसेन की विकासमूलक व्याख्या के कारण ही अधुना षट्खण्डागम-सिद्धान्त 'धवलासिद्धान्त' के नाम से और पेज्जदोसपाहुड 'जयधवलासिद्धान्त' के नाम से प्रख्यात हैं। ___ आचार्य वीरसेन ने परम्परानुसार विलक्षित विषय का प्रतिपादन करके अपनी टीका की प्रामाणिकता की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इन्हें यदि किसी अपने पूर्ववर्ती आचार्य का अभिप्राय सूत्रविरुद्ध या परम्पराविरुद्ध प्रतीत हुआ है तो इन्होंने उसे अग्राह्य घोषित कर दिया है। किन्तु स्वयं इन्हें आचार्य-परम्परागत उपदेश के अभाव में कुछ कहना पड़ा है तो उसे इन्होंने गुरु से प्राप्त उपदेश के आधार पर अपनी विवेचना का विषय बताया है। यद्यपि इन्होंने ग्राह्याग्राह्य के सन्दर्भ में अपनी विरोध-समन्वयकारी दृष्टि का परिचय दिया है। इनके वैदूष्य का परिज्ञान इस बात से भी होता है कि इन्होंने अपनी टीका में प्राचीन आगम के उपलब्ध साहित्य का पूरा उपयोग किया है।
आचार्य नेमिचन्द्र शास्त्री के अनुसार - धवला और जयधवला टीकाओं में आचार्य वीरसेन ने प्रसादगुण के संयोजन के साथ-साथ समाहार-शक्ति के विनियोग का भी विलक्षण परिचय दिया है। इनकी अतिशय सरल तर्क या न्याय शैली मन को मुग्ध कर देती है। विवेच्य विषय के उपस्थापन में इन्होंने पद और वाक्यों का अर्थ तो स्पष्ट किया ही है, तद्विषयक सूत्रों का स्पष्टीकरण भी इस पद्धति से किया है कि सूत्रों के सामान्य और गूढ़ दोनों प्रकार के अर्थों को अवगत करने में बुद्धि को व्यायाम नहीं करना पड़ता। शंका-समाधानपूर्वक विषय-निरूपण की निराडम्बर शैली तो ततोऽधिक सरल, स्वच्छ और हृदयावर्जक है। प्रसादगुणभूयिष्ठ विषयप्रतिपादन की शैलीगत स्वच्छता के कारण ही इस टीका का 'धवला' नाम सार्थक है।
शंका-समाधान द्वारा विषय का समन्वयन और संक्षेपणपूर्वक अपने वक्तव्य में विविध भंगों का संयोजन ही समाहार-शक्ति की विशेषता है। पूर्वाचार्यों द्वारा प्ररूपित गाथाओं और वाक्यों का 'उक्तञ्च' कहकर आचार्य वीरसेन ने अपने विवेच्य विषय के साथ इस प्रकार समाहार किया है जिस प्रकार पायस में घी मिलकर एकमेक हो गया है। मंगलाचरण' की विवेचना के क्रम में अपनाई गई इस समाहार-शैली का एक उदाहरण प्रस्तुत है -
"तद्व्यतिरिक्तं द्विविधं कर्मनोकर्ममङ्गलभेदात्। तत्र कर्ममङ्गलं दर्शन-विशुद्धयादिषोडशधा-प्रविभक्त-तीर्थंकर-नामकर्म-कारणैर्जीव-प्रदेश-निबद्ध-तीर्थंकर-नामकर्ममाङ्गल्य-निबन्धनत्वान्मङ्गलम्। यत्तन्नोकर्ममङ्गलं तद् द्विविधम्, लौकिकं लोकोत्तरमिति। तत्र लौकिकं त्रिविधम्, सचित्तमचित्तं मिश्रमिति। तत्राचित्तमङ्गलम् -
सिद्धत्थ-पुण्णकुंभो वंदणमाला य मंगलं छत्तं। सेदो वण्णो आदसणो य कण्णा य जच्चस्सो॥ सचित्तमङ्गलम्। मिश्रमङ्गल सालङ्कारकन्यादिः।"
(षट्खण्डागम, धवला, पु. 1, पृ. 92-93)