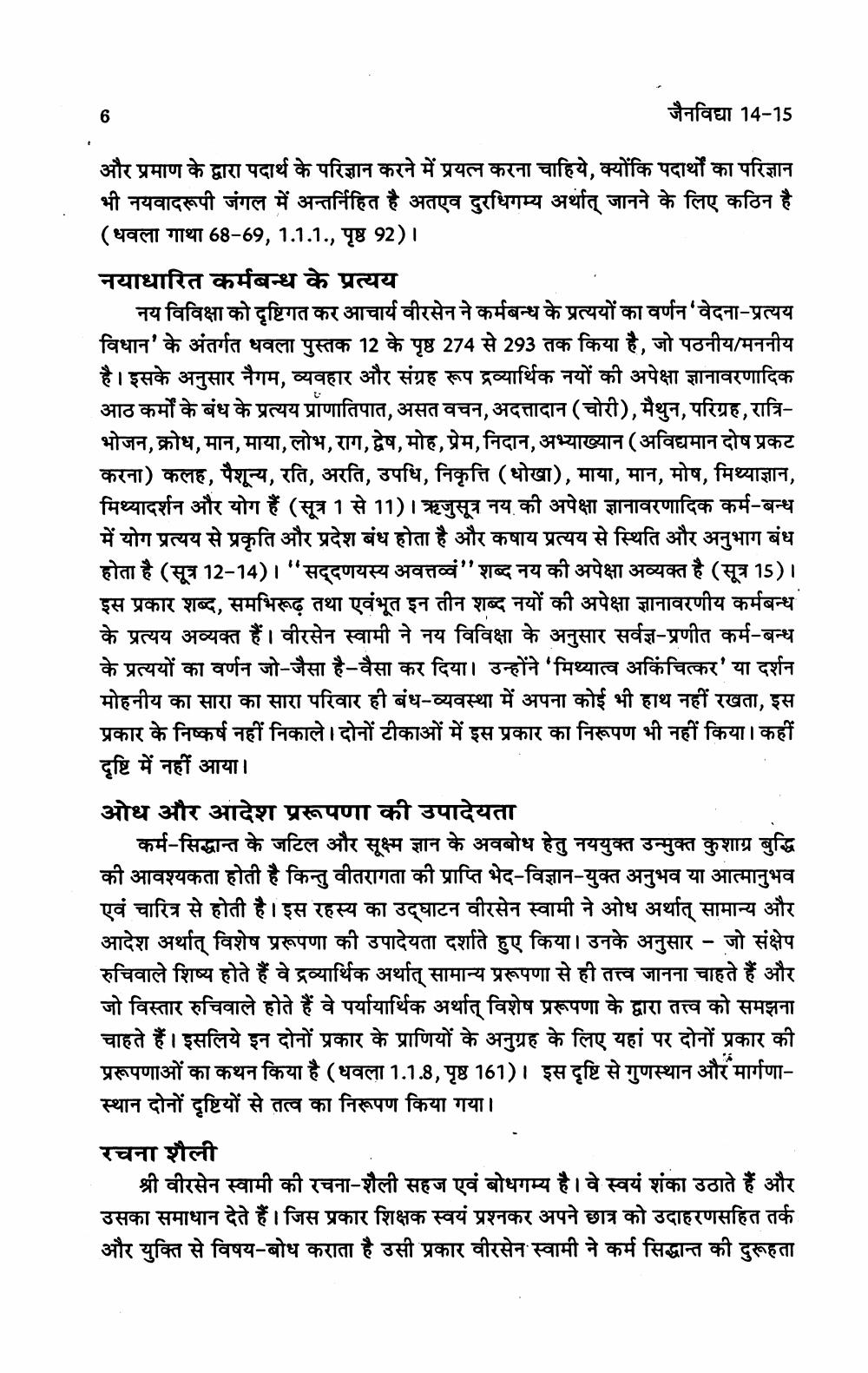________________
जैनविद्या 14-15
और प्रमाण के द्वारा पदार्थ के परिज्ञान करने में प्रयत्न करना चाहिये, क्योंकि पदार्थों का परिज्ञान भी नयवादरूपी जंगल में अन्तर्निहित है अतएव दुरधिगम्य अर्थात् जानने के लिए कठिन है (धवला गाथा 68-69, 1.1.1., पृष्ठ 92)।
6
नयाधारित कर्मबन्ध के प्रत्यय
नय विविक्षा को दृष्टिगत कर आचार्य वीरसेन ने कर्मबन्ध के प्रत्ययों का वर्णन 'वेदना-प्रत्यय विधान' के अंतर्गत धवला पुस्तक 12 के पृष्ठ 274 से 293 तक किया है, जो पठनीय / मननीय है। इसके अनुसार नैगम, व्यवहार और संग्रह रूप द्रव्यार्थिक नयों की अपेक्षा ज्ञानावरणादिक आठ कर्मों के बंध के प्रत्यय प्राणातिपात, असत वचन, अदत्तादान (चोरी), मैथुन, परिग्रह, रात्रिभोजन, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, प्रेम, निदान, अभ्याख्यान (अविद्यमान दोष प्रकट करना) कलह, पैशून्य, रति, अरति, उपधि, निवृत्ति (धोखा), माया, मान, मोष, मिथ्याज्ञान, मिथ्यादर्शन और योग हैं (सूत्र 1 से 11)। ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा ज्ञानावरणादिक कर्म-बन्ध में योग प्रत्यय से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है और कषाय प्रत्यय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है (सूत्र 12-14)। " सद्दणयस्य अवत्तव्वं" शब्द नय की अपेक्षा अव्यक्त है (सूत्र 15)। इस प्रकार शब्द, समभिरूढ़ तथा एवंभूत इन तीन शब्द नयों की अपेक्षा ज्ञानावरणीय कर्मबन्ध के प्रत्यय अव्यक्त हैं। वीरसेन स्वामी ने नय विविक्षा के अनुसार सर्वज्ञ-प्रणीत कर्म - बन्ध के प्रत्ययों का वर्णन जो-जैसा है वैसा कर दिया। उन्होंने 'मिथ्यात्व अकिंचित्कर' या दर्शन मोहनीय का सारा का सारा परिवार ही बंध-व्यवस्था में अपना कोई भी हाथ नहीं रखता, इस प्रकार के निष्कर्ष नहीं निकाले। दोनों टीकाओं में इस प्रकार का निरूपण भी नहीं किया । कहीं दृष्टि में नहीं आया।
ओध और आदेश प्ररूपणा की उपादेयता
कर्म-सिद्धान्त के जटिल और सूक्ष्म ज्ञान के अवबोध हेतु नययुक्त उन्मुक्त कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता होती है किन्तु वीतरागता की प्राप्ति भेद-विज्ञान युक्त अनुभव या आत्मानुभव एवं चारित्र से होती है। इस रहस्य का उद्घाटन वीरसेन स्वामी ने ओध अर्थात् सामान्य और आदेश अर्थात् विशेष प्ररूपणा की उपादेयता दर्शाते हुए किया। उनके अनुसार - जो संक्षेप रुचिवाले शिष्य होते हैं वे द्रव्यार्थिक अर्थात् सामान्य प्ररूपणा से ही तत्त्व जानना चाहते हैं और जो विस्तार रुचिवाले होते हैं वे पर्यायार्थिक अर्थात् विशेष प्ररूपणा के द्वारा तत्त्व को समझना चाहते हैं। इसलिये इन दोनों प्रकार के प्राणियों के अनुग्रह के लिए यहां पर दोनों प्रकार की प्ररूपणाओं का कथन किया है (धवला 1.1.8, पृष्ठ 161 ) । इस दृष्टि से गुणस्थान और मार्गणास्थान दोनों दृष्टियों से तत्व का निरूपण किया गया ।
रचना शैली
श्री वीरसेन स्वामी की रचना - शैली सहज एवं बोधगम्य है । वे स्वयं शंका उठाते हैं और उसका समाधान देते हैं । जिस प्रकार शिक्षक स्वयं प्रश्नकर अपने छात्र को उदाहरणसहित तर्क और युक्ति से विषय-बोध कराता है उसी प्रकार वीरसेन स्वामी ने कर्म सिद्धान्त की दुरूहता