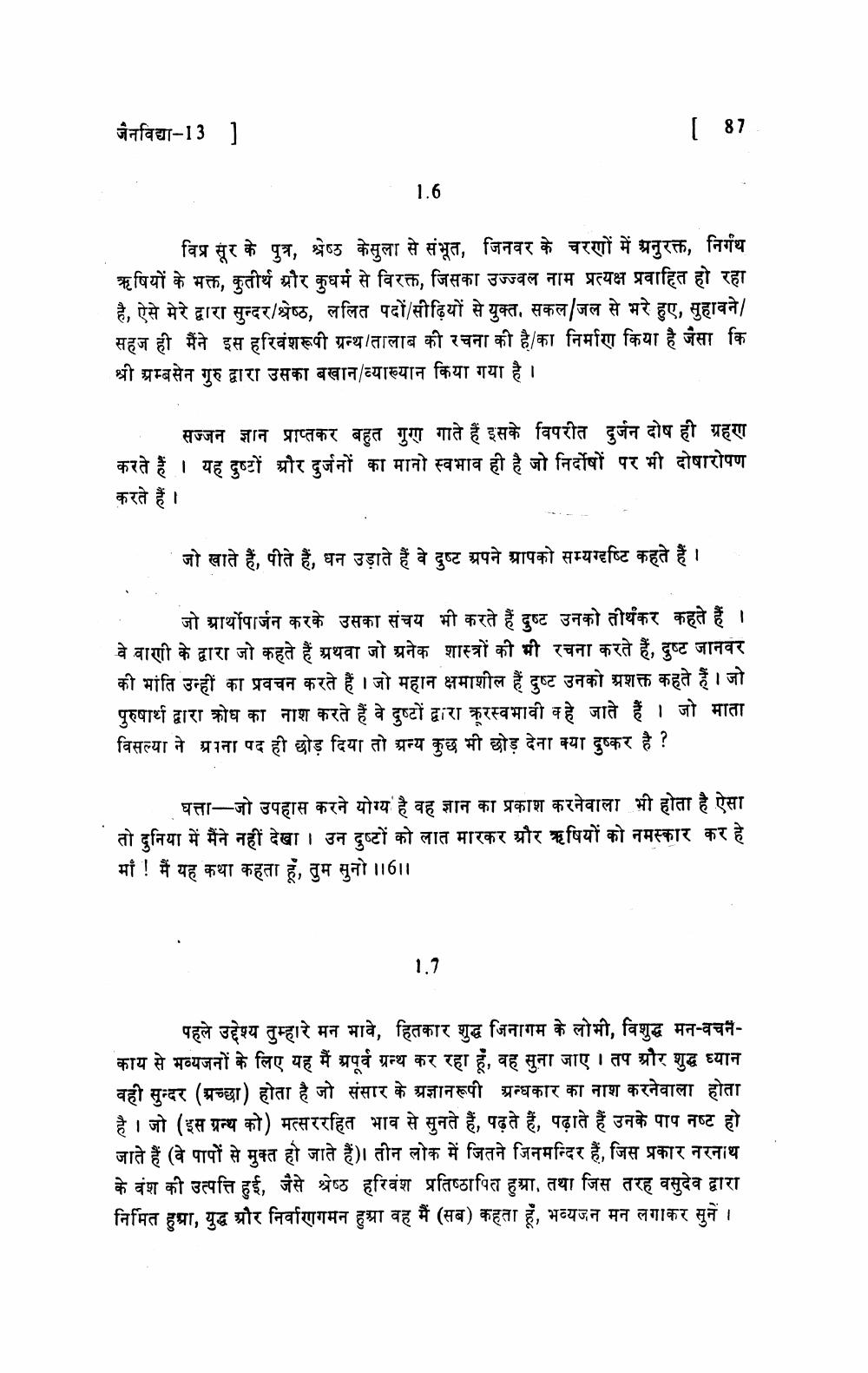________________
जैनविद्या - 13 1
1.6
[87
विप्र सूर के पुत्र, श्रेष्ठ केसुला से संभूत, जिनवर के चरणों में अनुरक्त, निर्बंध ऋषियों के भक्त, कुतीर्थ और कुधर्म से विरक्त, जिसका उज्ज्वल नाम प्रत्यक्ष प्रवाहित हो रहा है, ऐसे मेरे द्वारा सुन्दर / श्रेष्ठ, ललित पदों / सीढ़ियों से युक्त, सकल / जल से भरे हुए, सुहावने / सहज ही मैंने इस हरिवंशरूपी ग्रन्थ / तालाब की रचना की है / का निर्माण किया है जैसा कि श्री बसेन गुरु द्वारा उसका बखान / व्याख्यान किया गया है ।
सज्जन ज्ञान प्राप्तकर बहुत गुण गाते हैं इसके विपरीत दुर्जन दोष ही ग्रहण करते हैं । यह दुष्टों और दुर्जनों का मानो स्वभाव ही है जो निर्दोषों पर भी दोषारोपण करते हैं ।
जो खाते हैं, पीते हैं, धन उड़ाते हैं वे दुष्ट अपने ग्रापको सम्यग्दृष्टि कहते हैं ।
जो आर्थोपार्जन करके उसका संचय भी करते हैं दुष्ट उनको तीर्थंकर कहते हैं । वाणी के द्वारा जो कहते हैं अथवा जो अनेक शास्त्रों की भी रचना करते हैं, दुष्ट जानवर की भांति उन्हीं का प्रवचन करते हैं । जो महान क्षमाशील हैं दुष्ट उनको अशक्त कहते हैं । जो पुरुषार्थ द्वारा क्रोध का नाश करते हैं वे दुष्टों द्वारा क्रूरस्वभावी कहे जाते हैं । जो माता विसल्याने पद ही छोड़ दिया तो अन्य कुछ भी छोड़ देना क्या दुष्कर है ?
घत्ता- जो उपहास करने योग्य है वह ज्ञान का प्रकाश करनेवाला भी होता है ऐसा तो दुनिया में मैंने नहीं देखा । उन दुष्टों को लात मारकर और ऋषियों को नमस्कार कर हे ! मैं यह कथा कहता हूँ, तुम सुनो |16||
1.7
पहले उद्देश्य तुम्हारे मन भावे, हितकार शुद्ध जिनागम के लोभी, विशुद्ध मन-वचन" काय से भव्यजनों के लिए यह मैं अपूर्व ग्रन्थ कर रहा हूँ, वह सुना जाए। तप और शुद्ध ध्यान वही सुन्दर ( अच्छा ) होता है जो संसार के अज्ञानरूपी अन्धकार का नाश करनेवाला होता है । जो ( इस ग्रन्थ को ) मत्सररहित भाव से सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं (वे पापों से मुक्त हो जाते हैं)। तीन लोक में जितने जिनमन्दिर हैं, जिस प्रकार नरनाथ के वंश की उत्पत्ति हुई, जैसे श्रेष्ठ हरिवंश प्रतिष्ठापित हुआ तथा जिस तरह वसुदेव द्वारा निर्मित हुप्रा, युद्ध और निर्वाणगमन हुआ वह मैं (सब) कहता हूँ, भव्यजन मन लगाकर सुनें ।