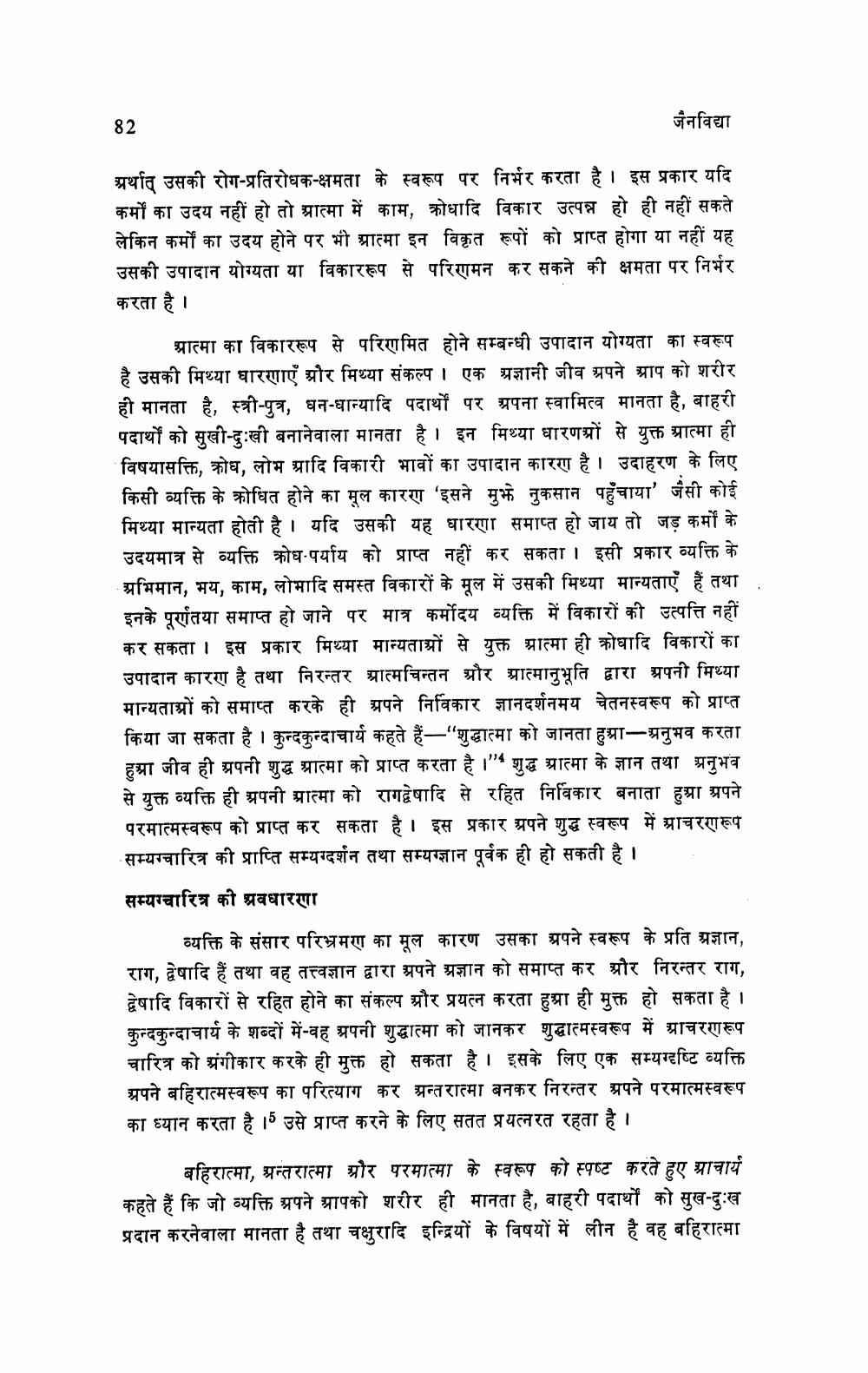________________
जनविद्या
अर्थात् उसकी रोग-प्रतिरोधक-क्षमता के स्वरूप पर निर्भर करता है। इस प्रकार यदि कर्मों का उदय नहीं हो तो आत्मा में काम, क्रोधादि विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकते लेकिन कर्मों का उदय होने पर भी आत्मा इन विकृत रूपों को प्राप्त होगा या नहीं यह उसकी उपादान योग्यता या विकाररूप से परिणमन कर सकने की क्षमता पर निर्भर करता है।
प्रात्मा का विकाररूप से परिणमित होने सम्बन्धी उपादान योग्यता का स्वरूप है उसकी मिथ्या धारणाएँ और मिथ्या संकल्प । एक अज्ञानी जीव अपने आप को शरीर ही मानता है, स्त्री-पुत्र, धन-धान्यादि पदार्थों पर अपना स्वामित्व मानता है, बाहरी पदार्थों को सुखी-दुःखी बनानेवाला मानता है। इन मिथ्या धारणों से युक्त आत्मा ही विषयासक्ति, क्रोध, लोभ आदि विकारी भावों का उपादान कारण है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के क्रोधित होने का मूल कारण 'इसने मुझे नुकसान पहुंचाया' जैसी कोई मिथ्या मान्यता होती है। यदि उसकी यह धारणा समाप्त हो जाय तो जड़ कर्मों के उदयमात्र से व्यक्ति क्रोध-पर्याय को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार व्यक्ति के अभिमान, भय, काम, लोभादि समस्त विकारों के मूल में उसकी मिथ्या मान्यताएं हैं तथा इनके पूर्णतया समाप्त हो जाने पर मात्र कर्मोदय व्यक्ति में विकारों की उत्पत्ति नहीं कर सकता। इस प्रकार मिथ्या मान्यताओं से युक्त प्रात्मा ही क्रोधादि विकारों का उपादान कारण है तथा निरन्तर आत्मचिन्तन और आत्मानुभूति द्वारा अपनी मिथ्या मान्यताओं को समाप्त करके ही अपने निर्विकार ज्ञानदर्शनमय चेतनस्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है । कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं- "शुद्धात्मा को जानता हुअा-अनुभव करता हुआ जीव ही अपनी शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है ।" शुद्ध प्रात्मा के ज्ञान तथा अनुभव से युक्त व्यक्ति ही अपनी आत्मा को रागद्वेषादि से रहित निर्विकार बनाता हुआ अपने परमात्मस्वरूप को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अपने शुद्ध स्वरूप में आचरणरूप सम्यग्चारित्र की प्राप्ति सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान पूर्वक ही हो सकती है। सम्यग्चारित्र को अवधारणा
व्यक्ति के संसार परिभ्रमण का मूल कारण उसका अपने स्वरूप के प्रति अज्ञान, राग, द्वेषादि हैं तथा वह तत्त्वज्ञान द्वारा अपने अज्ञान को समाप्त कर और निरन्तर राग, द्वेषादि विकारों से रहित होने का संकल्प और प्रयत्न करता हुआ ही मुक्त हो सकता है । कुन्दकुन्दाचार्य के शब्दों में-वह अपनी शुद्धात्मा को जानकर शुद्धात्मस्वरूप में आचरणरूप चारित्र को अंगीकार करके ही मुक्त हो सकता है। इसके लिए एक सम्यग्दृष्टि व्यक्ति अपने बहिरात्मस्वरूप का परित्याग कर अन्तरात्मा बनकर निरन्तर अपने परमात्मस्वरूप का ध्यान करता है । उसे प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नरत रहता है ।
बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए प्राचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आपको शरीर ही मानता है, बाहरी पदार्थों को सुख-दुःख प्रदान करनेवाला मानता है तथा चक्षुरादि इन्द्रियों के विषयों में लीन है वह बहिरात्मा