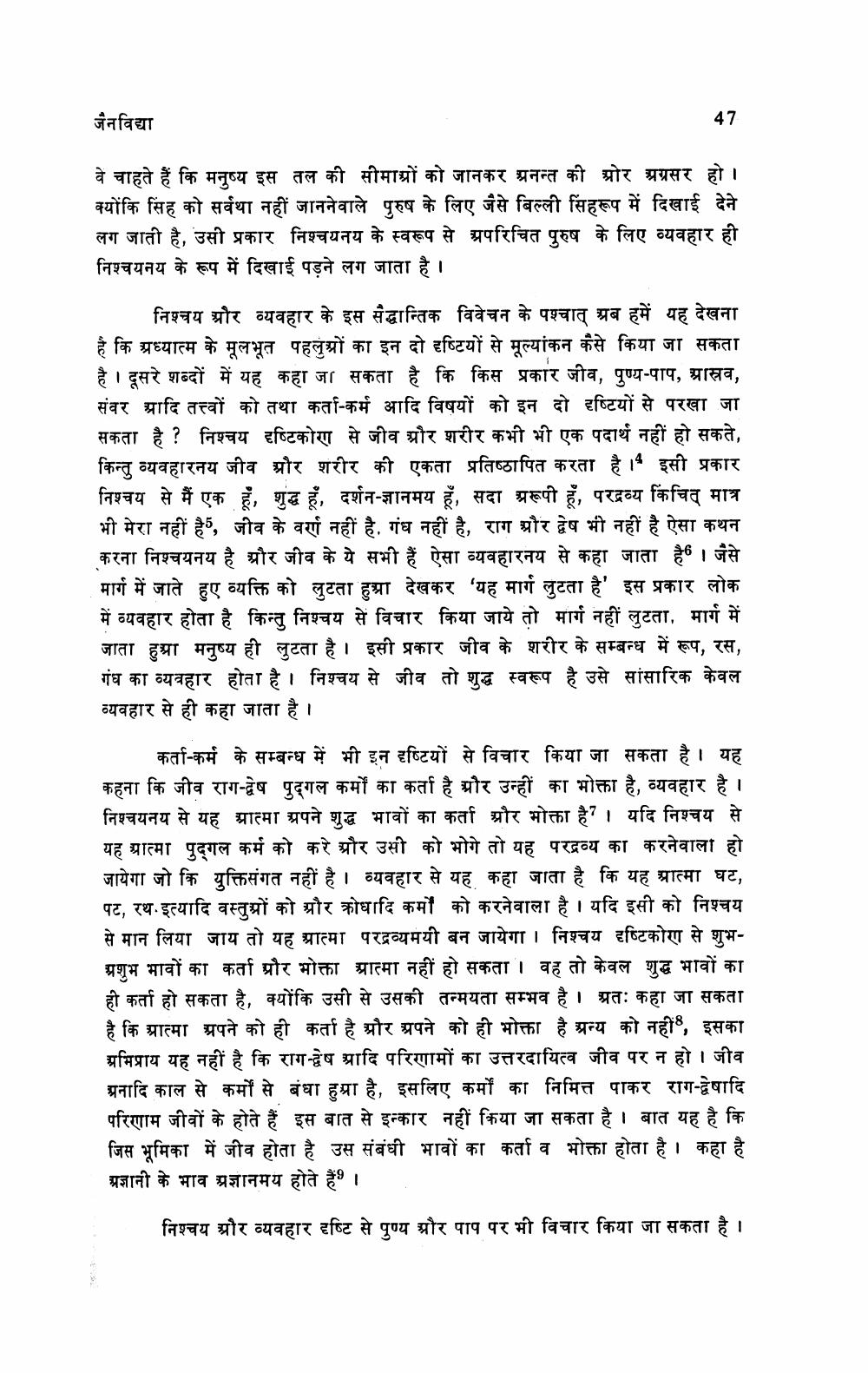________________
जैन विद्या
वे चाहते हैं कि मनुष्य इस तल की सीमाओं को जानकर अनन्त की ओर अग्रसर हो । क्योंकि सिंह को सर्वथा नहीं जाननेवाले पुरुष के लिए जैसे बिल्ली सिंहरूप में दिखाई देने लग जाती है, उसी प्रकार निश्चयनय के स्वरूप से अपरिचित पुरुष के लिए व्यवहार ही निश्चयनय के रूप में दिखाई पड़ने लग जाता है ।
निश्चय और व्यवहार के इस सैद्धान्तिक विवेचन के पश्चात् अब हमें यह देखना है कि अध्यात्म के मूलभूत पहलुओं का इन दो दृष्टियों से मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किस प्रकार जीव, पुण्य-पाप, प्रास्रव, संवर आदि तत्त्वों को तथा कर्ता-कर्म आदि विषयों को इन दो दृष्टियों से परखा जा सकता है ? निश्चय दृष्टिकोण से जीव और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं हो सकते, किन्तु व्यवहारनय जीव और शरीर की एकता प्रतिष्ठापित करता है। इसी प्रकार निश्चय से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन-ज्ञानमय हूँ, सदा अरूपी हूँ, परद्रव्य किंचित् मात्र भी मेरा नहीं है, जीव के वर्ण नहीं है. गंध नहीं है, राग और द्वेष भी नहीं है ऐसा कथन करना निश्चयनय है और जीव के ये सभी हैं ऐसा व्यवहारनय से कहा जाता है । जैसे मार्ग में जाते हुए व्यक्ति को लुटता हुआ देखकर 'यह मार्ग लुटता है' इस प्रकार लोक में व्यवहार होता है किन्तु निश्चय से विचार किया जाये तो मार्ग नहीं लुटता, मार्ग में जाता हुआ मनुष्य ही लुटता है। इसी प्रकार जीव के शरीर के सम्बन्ध में रूप, रस, गंध का व्यवहार होता है। निश्चय से जीव तो शुद्ध स्वरूप है उसे सांसारिक केवल व्यवहार से ही कहा जाता है।
कर्ता-कर्म के सम्बन्ध में भी इन दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। यह कहना कि जीव राग-द्वेष पुद्गल कर्मों का कर्ता है और उन्हीं का भोक्ता है, व्यवहार है । निश्चयनय से यह प्रात्मा अपने शुद्ध भावों का कर्ता और भोक्ता है। यदि निश्चय से यह आत्मा पुद्गल कर्म को करे और उसी को भोगे तो यह परद्रव्य का करनेवाला हो जायेगा जो कि युक्तिसंगत नहीं है। व्यवहार से यह कहा जाता है कि यह आत्मा घट, पट, रथ इत्यादि वस्तुओं को और क्रोधादि कर्मों को करनेवाला है । यदि इसी को निश्चय से मान लिया जाय तो यह आत्मा परद्रव्यमयी बन जायेगा। निश्चय दृष्टिकोण से शुभअशुभ भावों का कर्ता और मोक्ता आत्मा नहीं हो सकता। वह तो केवल शुद्ध भावों का ही कर्ता हो सकता है, क्योंकि उसी से उसकी तन्मयता सम्भव है। अतः कहा जा सकता है कि आत्मा अपने को ही कर्ता है और अपने को ही भोक्ता है अन्य को नहीं, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राग-द्वेष आदि परिणामों का उत्तरदायित्व जीव पर न हो । जीव अनादि काल से कर्मों से बंधा हुआ है, इसलिए कर्मों का निमित्त पाकर राग-द्वेषादि परिणाम जीवों के होते हैं इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है। बात यह है कि जिस भूमिका में जीव होता है उस संबंधी भावों का कर्ता व भोक्ता होता है। कहा है अज्ञानी के भाव अज्ञानमय होते हैं ।
निश्चय और व्यवहार दृष्टि से पुण्य और पाप पर भी विचार किया जा सकता है ।