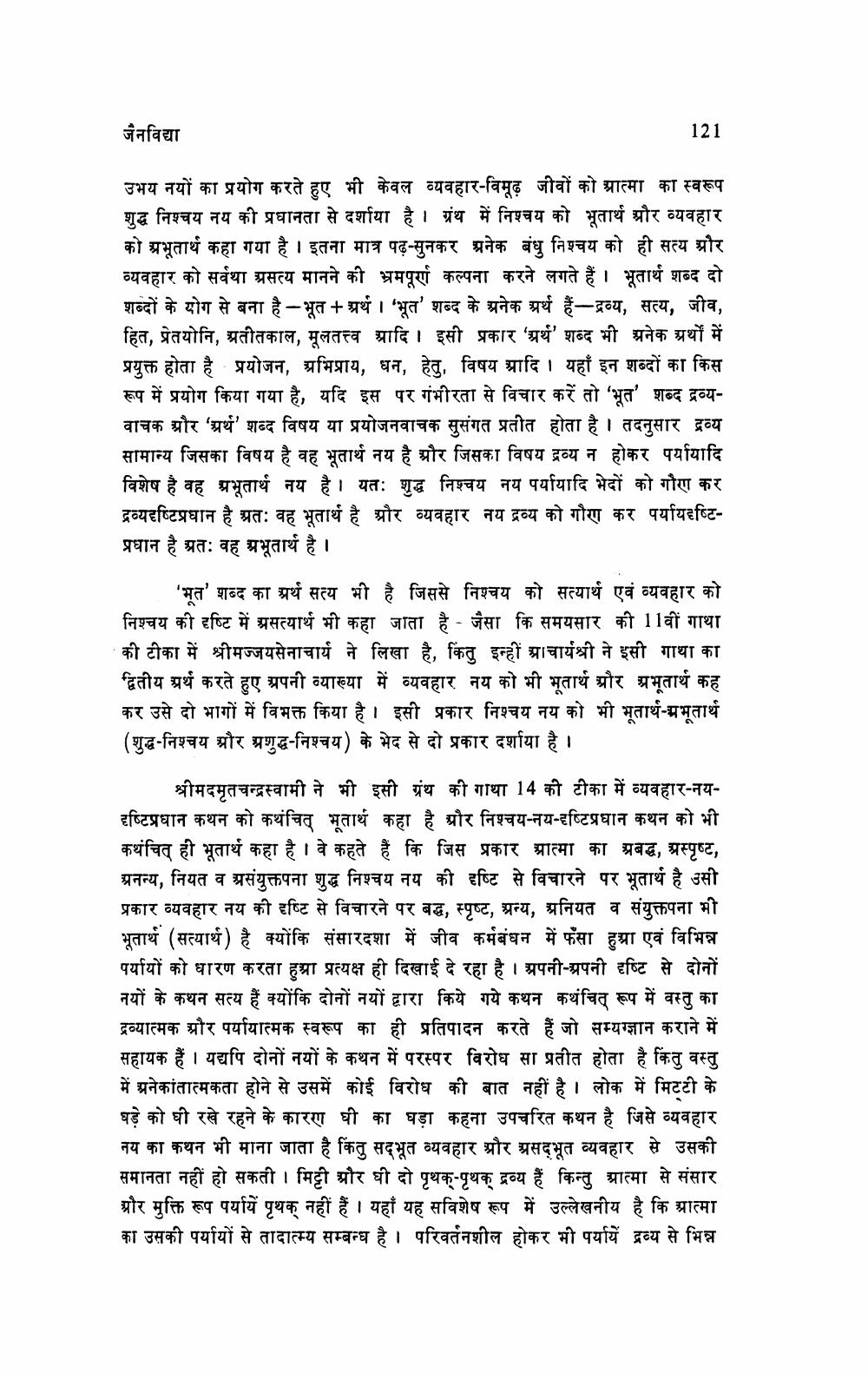________________
जैनविद्या
121
उभय नयों का प्रयोग करते हुए भी केवल व्यवहार-विमूढ़ जीवों को आत्मा का स्वरूप शुद्ध निश्चय नय की प्रधानता से दर्शाया है। ग्रंथ में निश्चय को भूतार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ कहा गया है । इतना मात्र पढ़-सुनकर अनेक बंधु निश्चय को ही सत्य और व्यवहार को सर्वथा असत्य मानने की भ्रमपूर्ण कल्पना करने लगते हैं। भूतार्थ शब्द दो शब्दों के योग से बना है - भूत + अर्थ । 'भूत' शब्द के अनेक अर्थ हैं-द्रव्य, सत्य, जीव, हित, प्रेतयोनि, अतीतकाल, मूलतत्त्व आदि। इसी प्रकार 'अर्थ' शब्द भी अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है प्रयोजन, अभिप्राय, धन, हेतु, विषय आदि । यहाँ इन शब्दों का किस रूप में प्रयोग किया गया है, यदि इस पर गंभीरता से विचार करें तो 'भूत' शब्द द्रव्यवाचक और 'अर्थ' शब्द विषय या प्रयोजनवाचक सुसंगत प्रतीत होता है । तदनुसार द्रव्य सामान्य जिसका विषय है वह भूतार्थ नय है और जिसका विषय द्रव्य न होकर पर्यायादि विशेष है वह अभूतार्थ नय है। यत: शुद्ध निश्चय नय पर्यायादि भेदों को गौण कर द्रव्यदृष्टिप्रधान है अतः वह भूतार्थ है और व्यवहार नय द्रव्य को गौण कर पर्यायष्टिप्रधान है अतः वह अभूतार्थ है।
'भूत' शब्द का अर्थ सत्य भी है जिससे निश्चय को सत्यार्थ एवं व्यवहार को निश्चय की दृष्टि में असत्यार्थ भी कहा जाता है - जैसा कि समयसार की 11वीं गाथा की टीका में श्रीमज्जयसेनाचार्य ने लिखा है, किंतु इन्हीं प्राचार्यश्री ने इसी गाथा का द्वितीय अर्थ करते हुए अपनी व्याख्या में व्यवहार नय को भी भूतार्थ और अभूतार्थ कह कर उसे दो भागों में विभक्त किया है। इसी प्रकार निश्चय नय को भी भूतार्थ-अभूतार्थ (शुद्ध-निश्चय और अशुद्ध-निश्चय) के भेद से दो प्रकार दर्शाया है।
श्रीमदमृतचन्द्रस्वामी ने भी इसी ग्रंथ की गाथा 14 की टीका में व्यवहार-नयदृष्टिप्रधान कथन को कथंचित् भूतार्थ कहा है और निश्चय-नय-दृष्टिप्रधान कथन को भी कथंचित् ही भूतार्थ कहा है । वे कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा का अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत व असंयुक्तपना शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से विचारने पर भूतार्थ है उसी प्रकार व्यवहार नय की दृष्टि से विचारने पर बद्ध, स्पृष्ट, अन्य, अनियत व संयुक्तपना भी भूतार्थ (सत्यार्थ) है क्योंकि संसारदशा में जीव कर्मबंधन में फंसा हुआ एवं विभिन्न पर्यायों को धारण करता हुआ प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा है । अपनी-अपनी दृष्टि से दोनों नयों के कथन सत्य हैं क्योंकि दोनों नयों द्वारा किये गये कथन कथंचित् रूप में वस्तु का द्रव्यात्मक और पर्यायात्मक स्वरूप का ही प्रतिपादन करते हैं जो सम्यग्ज्ञान कराने में सहायक हैं । यद्यपि दोनों नयों के कथन में परस्पर विरोध सा प्रतीत होता है किंतु वस्तु में अनेकांतात्मकता होने से उसमें कोई विरोध की बात नहीं है। लोक में मिटटी के घड़े को घी रखे रहने के कारण घी का घड़ा कहना उपचरित कथन है जिसे व्यवहार नय का कथन भी माना जाता है किंतु सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार से उसकी समानता नहीं हो सकती। मिट्टी और घी दो पृथक्-पृथक् द्रव्य हैं किन्तु आत्मा से संसार और मुक्ति रूप पर्यायें पृथक् नहीं हैं । यहाँ यह सविशेष रूप में उल्लेखनीय है कि प्रात्मा का उसकी पर्यायों से तादात्म्य सम्बन्ध है। परिवर्तनशील होकर भी पर्यायें द्रव्य से भिन्न