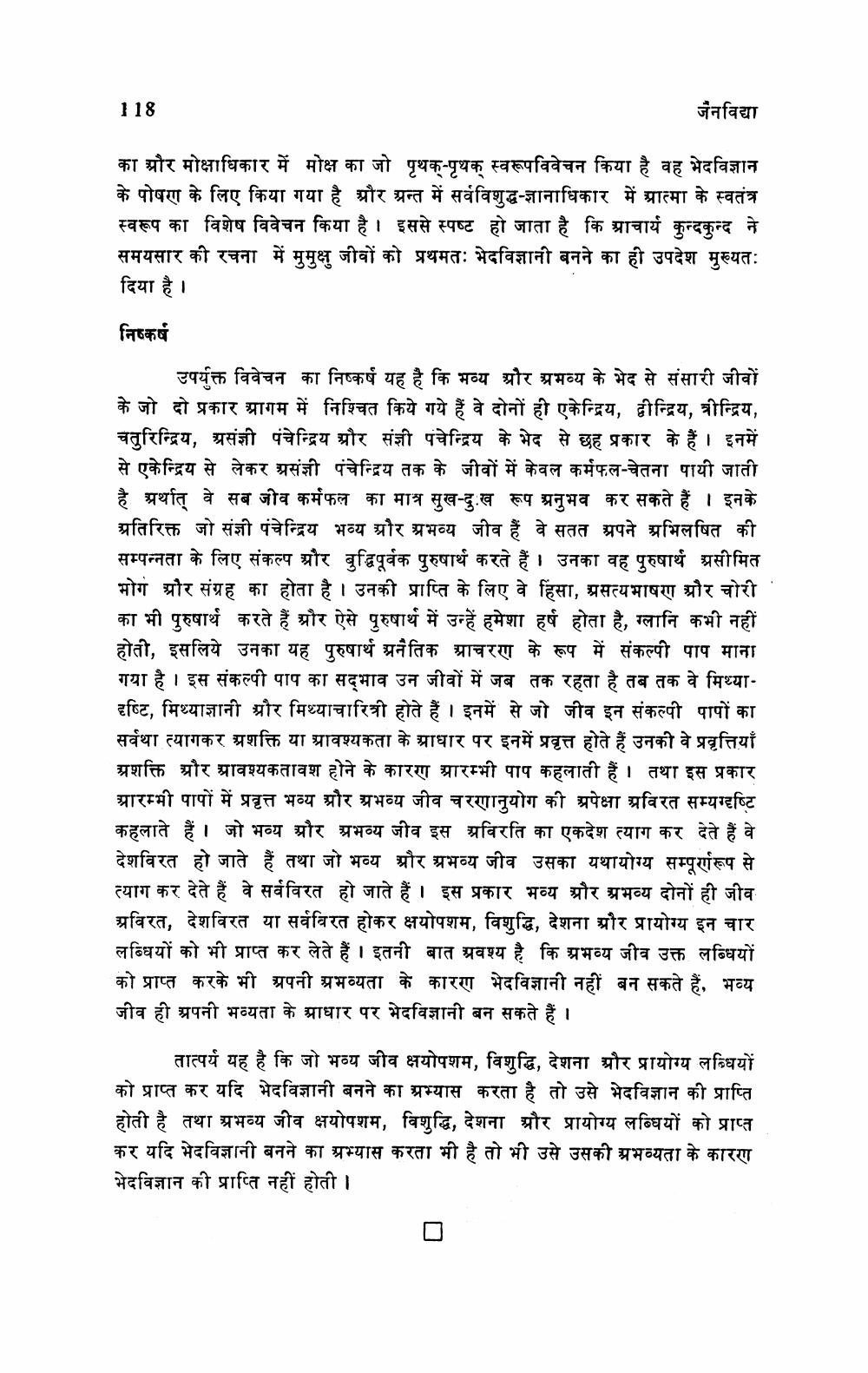________________
118
जैनविद्या
का और मोक्षाधिकार में मोक्ष का जो पृथक्-पृथक् स्वरूपविवेचन किया है वह भेदविज्ञान के पोषण के लिए किया गया है और अन्त में सर्वविशुद्ध-ज्ञानाधिकार में आत्मा के स्वतंत्र स्वरूप का विशेष विवेचन किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राचार्य कुन्दकुन्द ने समयसार की रचना में मुमुक्षु जीवों को प्रथमतः भेदविज्ञानी बनने का ही उपदेश मुख्यतः दिया है।
निष्कर्ष
उपर्युक्त विवेचन का निष्कर्ष यह है कि भव्य और अमव्य के भेद से संसारी जीवों के जो दो प्रकार आगम में निश्चित किये गये हैं वे दोनों ही एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय और संज्ञी पंचेन्द्रिय के भेद से छह प्रकार के हैं। इनमें से एकेन्द्रिय से लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय तक के जीवों में केवल कर्मफल-चेतना पायी जाती है अर्थात् वे सब जीव कर्मफल का मात्र सुख-दुःख रूप अनुभव कर सकते हैं । इनके अतिरिक्त जो संज्ञी पंचेन्द्रिय भव्य और अभव्य जीव हैं वे सतत अपने अभिलषित की सम्पन्नता के लिए संकल्प और बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करते हैं। उनका वह पुरुषार्थ असीमित भोग और संग्रह का होता है । उनकी प्राप्ति के लिए वे हिंसा, असत्यभाषण और चोरी का भी पुरुषार्थ करते हैं और ऐसे पुरुषार्थ में उन्हें हमेशा हर्ष होता है, ग्लानि कभी नहीं होती, इसलिये उनका यह पुरुषार्थ अनैतिक आचरण के रूप में संकल्पी पाप माना गया है । इस संकल्पी पाप का सद्भाव उन जीवों में जब तक रहता है तब तक वे मिथ्या. दृष्टि, मिथ्याज्ञानी और मिथ्याचारित्री होते हैं । इनमें से जो जीव इन संकल्पी पापों का सर्वथा त्यागकर अशक्ति या आवश्यकता के आधार पर इनमें प्रवृत्त होते हैं उनकी वे प्रवृत्तियाँ अशक्ति और आवश्यकतावश होने के कारण प्रारम्भी पाप कहलाती हैं। तथा इस प्रकार प्रारम्भी पापों में प्रवृत्त भव्य और अभव्य जीव चरणानुयोग की अपेक्षा अविरत सम्यग्दृष्टि कहलाते हैं। जो भव्य और अभव्य जीव इस अविरति का एकदेश त्याग कर देते हैं वे देशविरत हो जाते हैं तथा जो भव्य और अभव्य जीव उसका यथायोग्य सम्पूर्णरूप से त्याग कर देते हैं वे सर्वविरत हो जाते हैं। इस प्रकार भव्य और अभव्य दोनों ही जीव अविरत, देशविरत या सर्वविरत होकर क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य इन चार लब्धियों को भी प्राप्त कर लेते हैं । इतनी बात अवश्य है कि अभव्य जीव उक्त लब्धियों को प्राप्त करके भी अपनी अभव्यता के कारण भेदविज्ञानी नहीं बन सकते हैं, भव्य जीव ही अपनी भव्यता के आधार पर भेदविज्ञानी बन सकते हैं।
तात्पर्य यह है कि जो भव्य जीव क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य लब्धियों को प्राप्त कर यदि भेदविज्ञानी बनने का अभ्यास करता है तो उसे भेदविज्ञान की प्राप्ति होती है तथा अभव्य जीव क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य लब्धियों को प्राप्त कर यदि भेदविज्ञानी बनने का अभ्यास करता भी है तो भी उसे उसकी अभव्यता के कारण भेदविज्ञान की प्राप्ति नहीं होती।