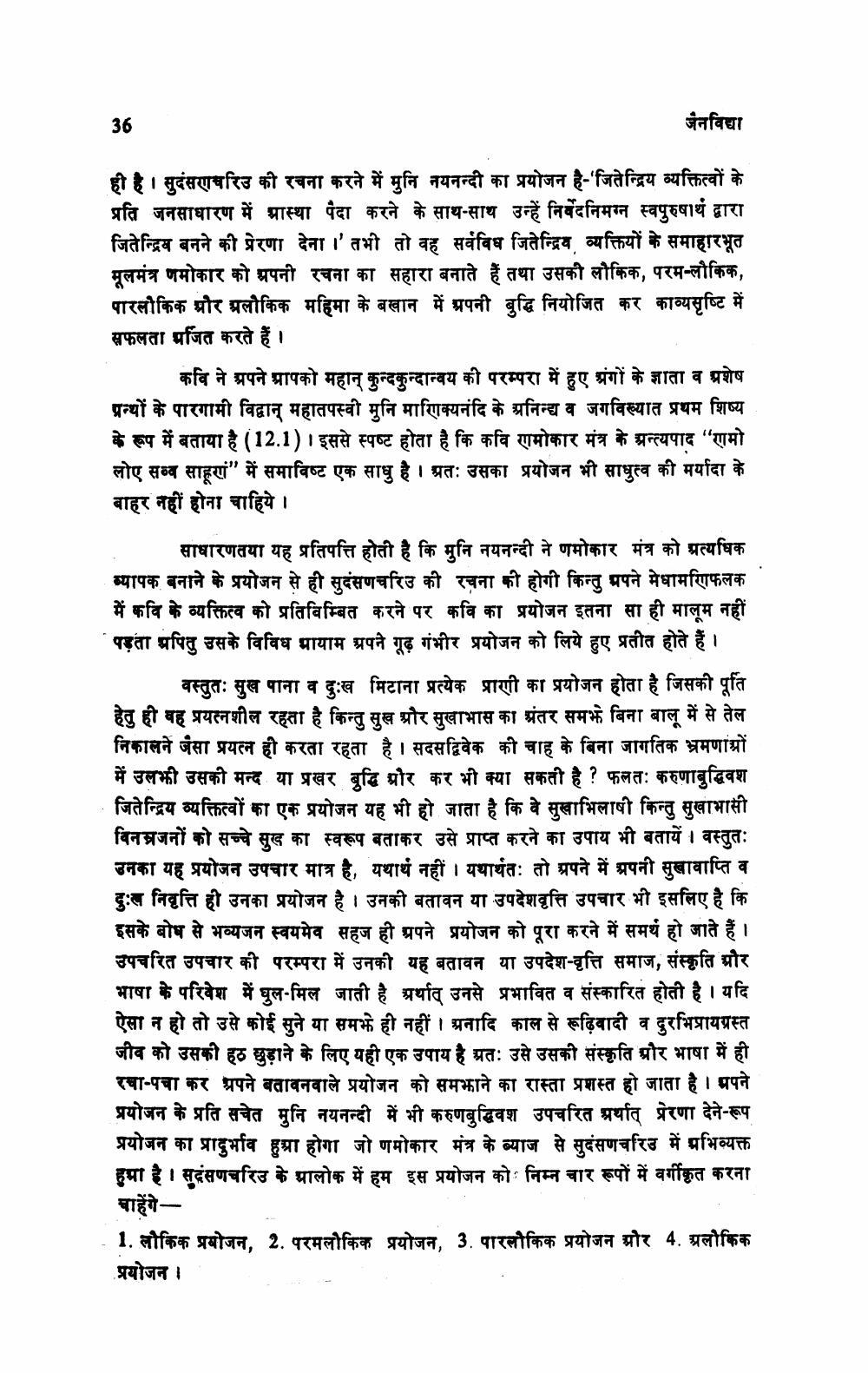________________
जैन विद्या
ही है। सुदंसरणचरिउ की रचना करने में मुनि नयनन्दी का प्रयोजन है - 'जितेन्द्रिय व्यक्तित्वों के प्रति जनसाधारण में प्रास्था पैदा करने के साथ-साथ उन्हें निर्वेदनिमग्न स्वपुरुषार्थं द्वारा जितेन्द्रिय बनने की प्रेरणा देना ।' तभी तो वह सर्वविध जितेन्द्रिय व्यक्तियों के समाहारभूत मूलमंत्र णमोकार को अपनी रचना का सहारा बनाते हैं तथा उसकी लौकिक, परम-लौकिक, पारलौकिक और प्रलौकिक महिमा के बखान में अपनी बुद्धि नियोजित कर काव्यसृष्टि में सफलता भर्जित करते हैं ।
36
afa ने अपने आपको महान् कुन्दकुन्दान्वय की परम्परा में हुए अंगों के ज्ञाता व प्रशेष ग्रन्थों के पारगामी विद्वान् महातपस्वी मुनि माणिक्यनंदि के अनिन्द्य व जगविख्यात प्रथम शिष्य के रूप में बताया है (12.1 ) । इससे स्पष्ट होता है कि कवि णमोकार मंत्र के अन्त्यपाद " णमो लोए सव्व साहूणं" में समाविष्ट एक साधु है । अतः उसका प्रयोजन भी साधुत्व की मर्यादा के बाहर नहीं होना चाहिये ।
साधारणतया यह प्रतिपत्ति होती है कि मुनि नयनन्दी ने णमोकार मंत्र को प्रत्यधिक ब्यापक बनाने के प्रयोजन से ही सुदंसणचरिउ की रचना की होगी किन्तु म्रपने मेधामणिफलक कवि के व्यक्तित्व को प्रतिविम्बित करने पर कवि का प्रयोजन इतना सा ही मालूम नहीं पड़ता अपितु उसके विविध प्रायाम अपने गूढ़ गंभीर प्रयोजन को लिये हुए प्रतीत होते हैं ।
वस्तुतः सुख पाना व दुःख मिटाना प्रत्येक प्राणी का प्रयोजन होता है जिसकी पूर्ति हेतु ही वह प्रयत्नशील रहता है किन्तु सुख और सुखाभास का अंतर समझे बिना बालू में से तेल निकालने जैसा प्रयत्न ही करता रहता है । सदसद्विवेक की चाह के बिना जागतिक भ्रमणात्रों में उलझी उसकी मन्द या प्रखर बुद्धि और कर भी क्या सकती है ? फलतः करुणाबुद्धिवश जितेन्द्रिय व्यक्तित्वों का एक प्रयोजन यह भी हो जाता है कि वे सुखाभिलाषी किन्तु सुखाभासी विनम्रजनों को सच्चे सुख का स्वरूप बताकर उसे प्राप्त करने का उपाय भी बतायें । वस्तुतः उनका यह प्रयोजन उपचार मात्र है, यथार्थं नहीं । यथार्थतः तो अपने में अपनी सुखावाप्ति व दुःख निवृत्ति ही उनका प्रयोजन है। उनकी बतावन या उपदेशवृत्ति उपचार भी इसलिए है कि इसके बोध से भव्यजन स्वयमेव सहज ही अपने प्रयोजन को पूरा करने में समर्थ हो जाते हैं । उपचरित उपचार की परम्परा में उनकी यह बतावन या उपदेश-वृत्ति समाज, संस्कृति और भाषा के परिवेश में घुल-मिल जाती है अर्थात् उनसे प्रभावित व संस्कारित होती है । यदि ऐसा न हो तो उसे कोई सुने या समझे ही नहीं । अनादि काल से रूढ़िवादी व दुरभिप्रायग्रस्त जीव को उसकी हठ छुड़ाने के लिए यही एक उपाय है अतः उसे उसकी संस्कृति और भाषा में ही रचा पचा कर अपने बतावनवाले प्रयोजन को समझाने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है । प्रपने प्रयोजन के प्रति सचेत मुनि नयनन्दी में भी करुणबुद्धिवश उपचरित अर्थात् प्रेरणा देने-रूप प्रयोजन का प्रादुर्भाव हुआ होगा जो णमोकार मंत्र के ब्याज से सुदंसणचरिउ में प्रभिव्यक्त हुआ है। सुदंसणचरिउ के आलोक में हम इस प्रयोजन को निम्न चार रूपों में वर्गीकृत करना चाहेंगे
--
1. लौकिक प्रयोजन, 2. परमलौकिक प्रयोजन, 3. पारलौकिक प्रयोजन और 4 अलौकिक प्रयोजन ।