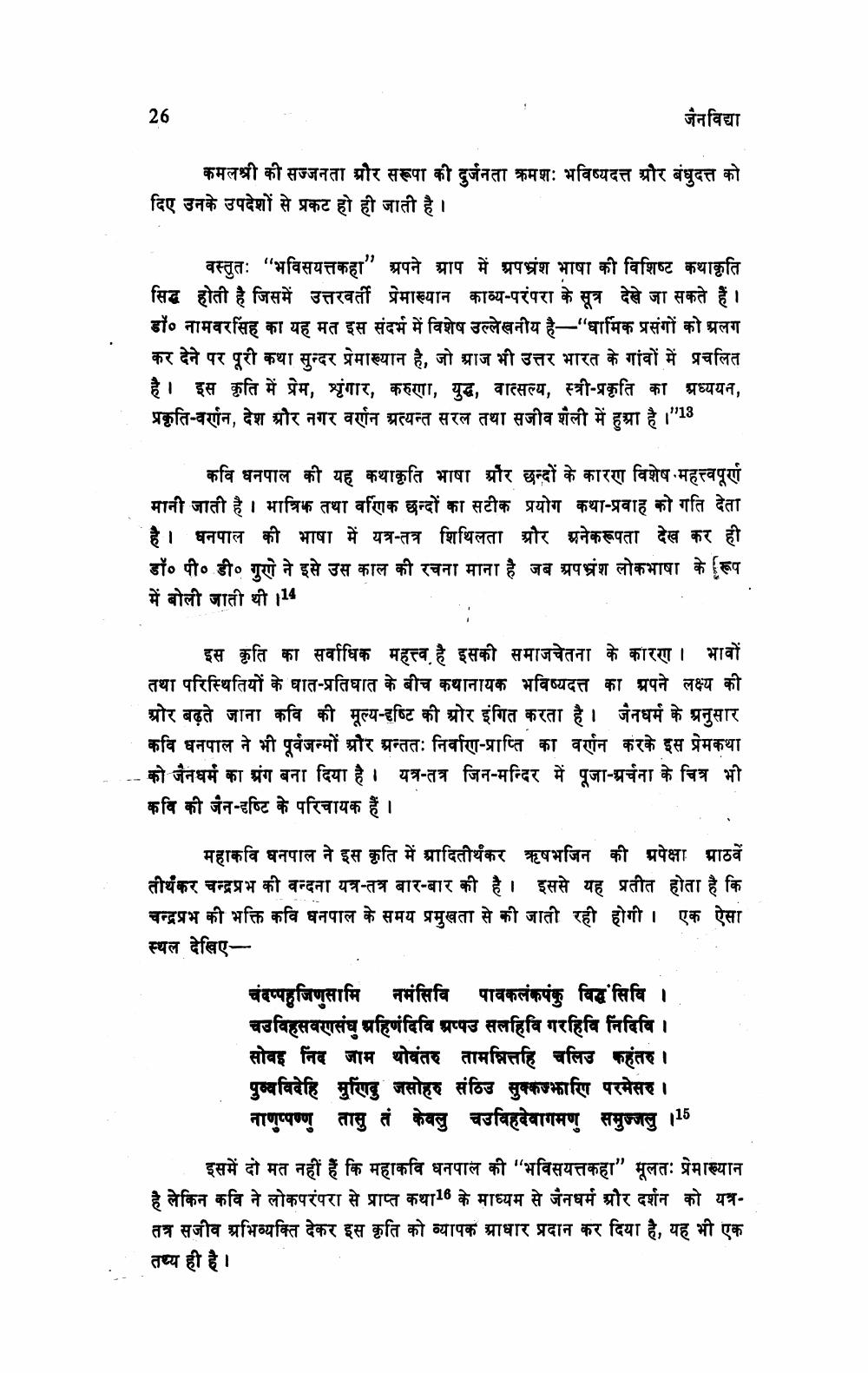________________
जैन विद्या
कमली की सज्जनता और सरूपा की दुर्जनता क्रमशः भविष्यदत्त और बंधुदत्त को दिए उनके उपदेशों से प्रकट हो ही जाती है ।
26
वस्तुतः " भविसयत्तकहा" अपने आप में अपभ्रंश भाषा की विशिष्ट कथाकृति सिद्ध होती है जिसमें उत्तरवर्ती प्रेमाख्यान काव्य-परंपरा के सूत्र देखे जा सकते हैं । डॉ० नामवरसिंह का यह मत इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है - " धार्मिक प्रसंगों को अलग कर देने पर पूरी कथा सुन्दर प्रेमाख्यान है, जो श्राज भी उत्तर भारत के गांवों में प्रचलित है । इस कृति में प्रेम, श्रृंगार, करुणा, युद्ध, वात्सल्य, स्त्री-प्रकृति का अध्ययन, प्रकृति-वर्णन, देश और नगर वर्णन प्रत्यन्त सरल तथा सजीव शैली में हुआ है । 13
कवि धनपाल की यह कथाकृति भाषा और छन्दों के कारण विशेष महत्त्वपूर्ण मानी जाती है । मात्रिक तथा वणिक छन्दों का सटीक प्रयोग कथा - प्रवाह को गति देता है । धनपाल की भाषा में यत्र-तत्र शिथिलता और अनेकरूपता देख कर ही डॉ० पी० डी० गुणे ने इसे उस काल की रचना माना है जब अपभ्रंश लोकभाषा के रूप में बोली जाती थी । 14
इस कृति का सर्वाधिक महत्त्व है इसकी समाजचेतना के कारण । भावों तथा परिस्थितियों के घात-प्रतिघात के बीच कथानायक भविष्यदत्त का अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना कवि की मूल्य-दृष्टि की ओर इंगित करता है। जैनधर्म के अनुसार कवि धनपाल ने भी पूर्वजन्मों और अन्ततः निर्वाण प्राप्ति का वर्णन करके इस प्रेमकथा को जैनधर्म का अंग बना दिया है । यत्र-तत्र जिन मन्दिर में पूजा-अर्चना के चित्र भी कवि की जैन दृष्टि के परिचायक हैं ।
महाकवि धनपाल ने इस कृति में आदितीर्थंकर ऋषभजिन की अपेक्षा पाठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रभ की वन्दना यत्र-तत्र बार-बार की है। इससे यह प्रतीत होता है कि चन्द्रप्रभ की भक्ति कवि धनपाल के समय प्रमुखता से की जाती रही होगी । एक ऐस स्थल देखिए—
चंदप्पहुजिणुसामि
नमंसिवि पावकलंकपंकु विद्ध सिवि ।
च विहसवरणसंघु प्रहिणं दिवि अप्पर सलहिवि गरहिवि निदिवि । सोवइ निंद जाम थोवंतर तामन्नित्तहि चलिउ कहंतर । पुण्वविदेहि मुरिंगवु जसोहरु संठिउ सुक्ककारिण परमेसर । नाणुप्पण्णु तासु तं केवलु चउविहदेवागमण समुज्जलु 115
इसमें दो मत नहीं हैं कि महाकवि धनपाल की " भविसयत्तकहा " मूलतः प्रेमाख्यान
है लेकिन कवि ने लोकपरंपरा से प्राप्त कथा 16 के माध्यम से जैनधर्म और दर्शन को यत्रतत्र सजीव अभिव्यक्ति देकर इस कृति को व्यापक आधार प्रदान कर दिया है, यह भी एक तथ्य ही है ।