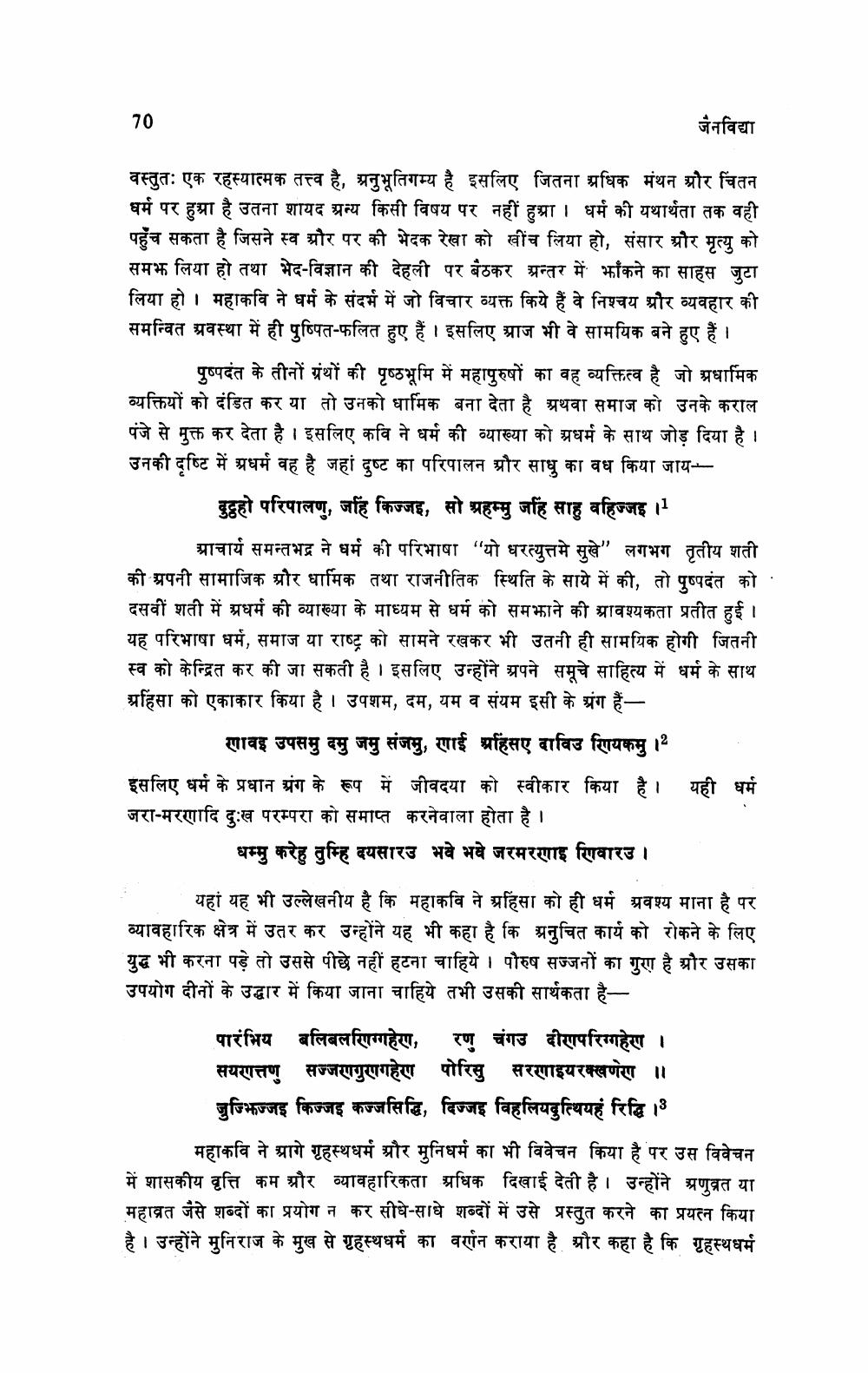________________
जैनविद्या
वस्तुतः एक रहस्यात्मक तत्त्व है, अनुभूतिगम्य है इसलिए जितना अधिक मंथन और चिंतन धर्म पर हुआ है उतना शायद अन्य किसी विषय पर नहीं हुआ । धर्म की यथार्थता तक वही पहुँच सकता है जिसने स्व और पर की भेदक रेखा को खींच लिया हो, संसार और मृत्यु को समझ लिया हो तथा भेद - विज्ञान की देहली पर बैठकर अन्तर में झाँकने का साहस जुटा लिया हो । महाकवि ने धर्म के संदर्भ में जो विचार व्यक्त किये हैं वे निश्चय श्रौर व्यवहार की समन्वित अवस्था में ही पुष्पित- फलित हुए हैं । इसलिए आज भी वे सामयिक बने हुए हैं ।
70
पुष्पदंत के तीनों ग्रंथों की पृष्ठभूमि में महापुरुषों का वह व्यक्तित्व है जो प्रधार्मिक व्यक्तियों को दंडित कर या तो उनको धार्मिक बना देता है अथवा समाज को उनके कराल पंजे से मुक्त कर देता है । इसलिए कवि ने धर्म की व्याख्या को अधर्म के साथ जोड़ दिया है । उनकी दृष्टि में धर्म वह है जहां दुष्ट का परिपालन और साधु का वध किया जाय
हो परिपालणु, जह किज्जइ, सो ग्रहम्मु जहि साहु वहिज्जइ । 1
आचार्य समन्तभद्र ने धर्म की परिभाषा " यो धरत्युत्तमे सुखे" लगभग तृतीय शती की अपनी सामाजिक और धार्मिक तथा राजनीतिक स्थिति के साये में की, तो पुष्पदंत को दसवीं शती में अधर्म की व्याख्या के माध्यम से धर्म को समझाने की आवश्यकता प्रतीत हुई । यह परिभाषा धर्म, समाज या राष्ट्र को सामने रखकर भी उतनी ही सामयिक होगी जितनी स्व को केन्द्रित कर की जा सकती है। इसलिए उन्होंने अपने समूचे साहित्य में धर्म के साथ हिंसा को एकाकार किया है । उपशम, दम, यम व संयम इसी के अंग हैं
गावइ उपसमुदमु जमु संजमु, गाई श्रहिंसए वाविउ यिकमु । 2
इसलिए धर्म के प्रधान अंग के रूप में जरा-मरणादि दुःख परम्परा को समाप्त
जीवदया को स्वीकार किया है । करनेवाला होता है ।
धम्मु करेहु तुम्हि वयसारउ भवे भवे जरमरणाइ शिवारउ ।
यही धर्म
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि महाकवि ने अहिंसा को ही धर्म अवश्य माना है पर व्यावहारिक क्षेत्र में उतर कर उन्होंने यह भी कहा है कि अनुचित कार्य को रोकने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिये । पौरुष सज्जनों का गुरण है और उसका उपयोग दीनों के उद्धार में किया जाना चाहिये तभी उसकी सार्थकता है
पारंभिय बलिबल रिग्गहेण, रणु चंगउ दीरणपरिग्गहेण । सयरणत्तणु सज्जरगुरणगहेण पोरिसु सरगाइयरक्खणे ॥ जुज्झिज्जर किज्जइ कज्जसिद्धि, दिज्जइ विहलियदुत्थियहं रिद्धि | 3
महाकवि ने आगे गृहस्थधर्म और मुनिधर्म का भी विवेचन किया है पर उस विवेचन में शासकीय वृत्ति कम और व्यावहारिकता अधिक दिखाई देती है । उन्होंने अणुव्रत या महाव्रत जैसे शब्दों का प्रयोग न कर सीधे-साधे शब्दों में उसे प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने मुनिराज के मुख से गृहस्थधर्म का वर्णन कराया है और कहा है कि गृहस्थधर्म