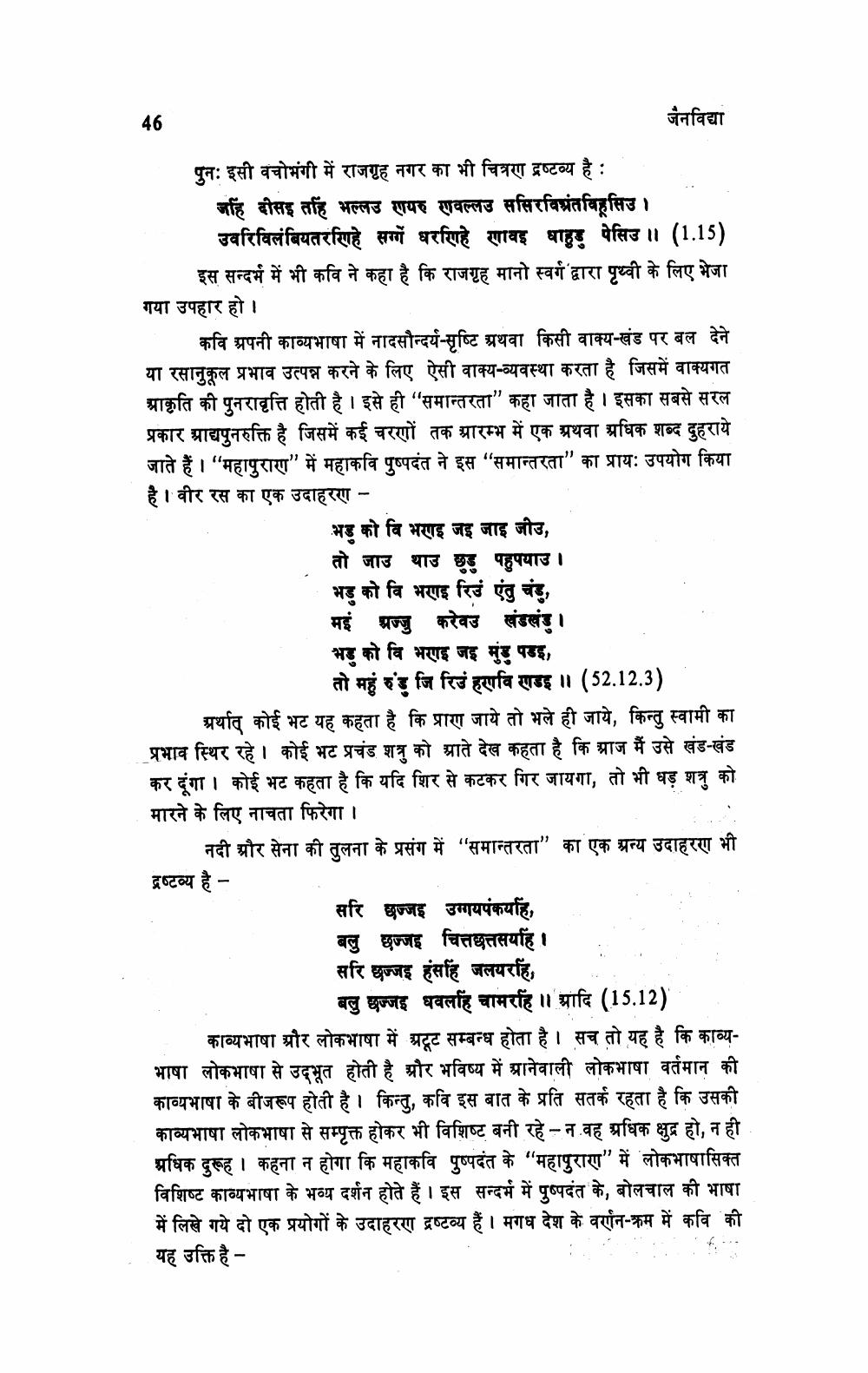________________
46
पुन: इसी वचोभंगी में राजगृह नगर का भी चित्ररण द्रष्टव्य है : जहि बीसइ तह भल्लड गयरु गवल्लउ ससिरविनंत विहूसिउ । उवरिविलं बियतरणिहे सर्गे धरणिहे गाव धाडु पेसिउ ॥ ( 1.15 ) इस सन्दर्भ में भी कवि ने कहा है कि राजगृह मानो स्वर्ग द्वारा पृथ्वी के लिए भेजा गया उपहार हो ।
कवि अपनी काव्यभाषा में नादसौन्दर्य-सृष्टि अथवा किसी वाक्य खंड पर बल देने या रसानुकूल प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ऐसी वाक्य व्यवस्था करता है जिसमें वाक्यगत प्रकृति की पुनरावृत्ति होती है । इसे ही “समान्तरता" कहा जाता है । इसका सबसे सरल प्रकार श्राद्यपुनरुक्ति है जिसमें कई चरणों तक आरम्भ में एक अथवा अधिक शब्द दुहराये जाते हैं । "महापुराण" में महाकवि पुष्पदंत ने इस " समान्तरता" का प्रायः उपयोग किया है । वीर रस का एक उदाहरण
-
जैनविद्या
भको विभर जइ जाइ जीउ, तो जाउ थाउ छुडु पहुपयाउ । भड को वि भरगइ रिडं एंतु चंड,
मई अज्जु करेवउ खंडखंड |
भड़ को वि भरणइ जइ मुंड पडइ,
तो महं रुंड जि रिडं हरवि गडइ ॥ ( 52.12.3)
अर्थात् कोई भट यह कहता है कि प्राण जाये तो भले ही जाये, किन्तु स्वामी का प्रभाव स्थिर रहे । कोई भट प्रचंड शत्रु को आते देख कहता है कि आज मैं उसे खंड-खंड कर दूंगा । कोई भट कहता है कि यदि शिर से कटकर गिर जायगा, तो भी धड़ शत्रु को मारने के लिए नाचता फिरेगा ।
नदी और सेना की तुलना के प्रसंग में "समान्तरता" का एक अन्य उदाहरण भी द्रष्टव्य है -
सरि छज्जइ उग्गयपंकर्याह, बलु छज्जद चित्तछत्तसर्याह । सरि छज्जइ हंसहि जलयहि, बलु छज्जइ धवलह चामह ।
श्रदि (15.12 )
काव्यभाषा और लोकभाषा में अटूट सम्बन्ध होता है। सच तो यह है कि काव्यभाषा लोकभाषा से उद्भूत होती है और भविष्य में आनेवाली लोकभाषा वर्तमान की काव्यभाषा के बीजरूप होती है । किन्तु, कवि इस बात के प्रति सतर्क रहता है कि उसकी काव्यभाषा लोकभाषा से सम्पृक्त होकर भी विशिष्ट बनी रहे - न वह अधिक क्षुद्र हो, न ही अधिक दुरूह । कहना न होगा कि महाकवि पुष्पदंत के " महापुराण" में लोकभाषासिक्त विशिष्ट काव्यभाषा के भव्य दर्शन होते हैं । इस सन्दर्भ में पुष्पदंत के, बोलचाल की भाषा में लिखे गये दो एक प्रयोगों के उदाहरण द्रष्टव्य हैं। मगध देश के वर्णन क्रम में कवि की यह उक्ति है -
-