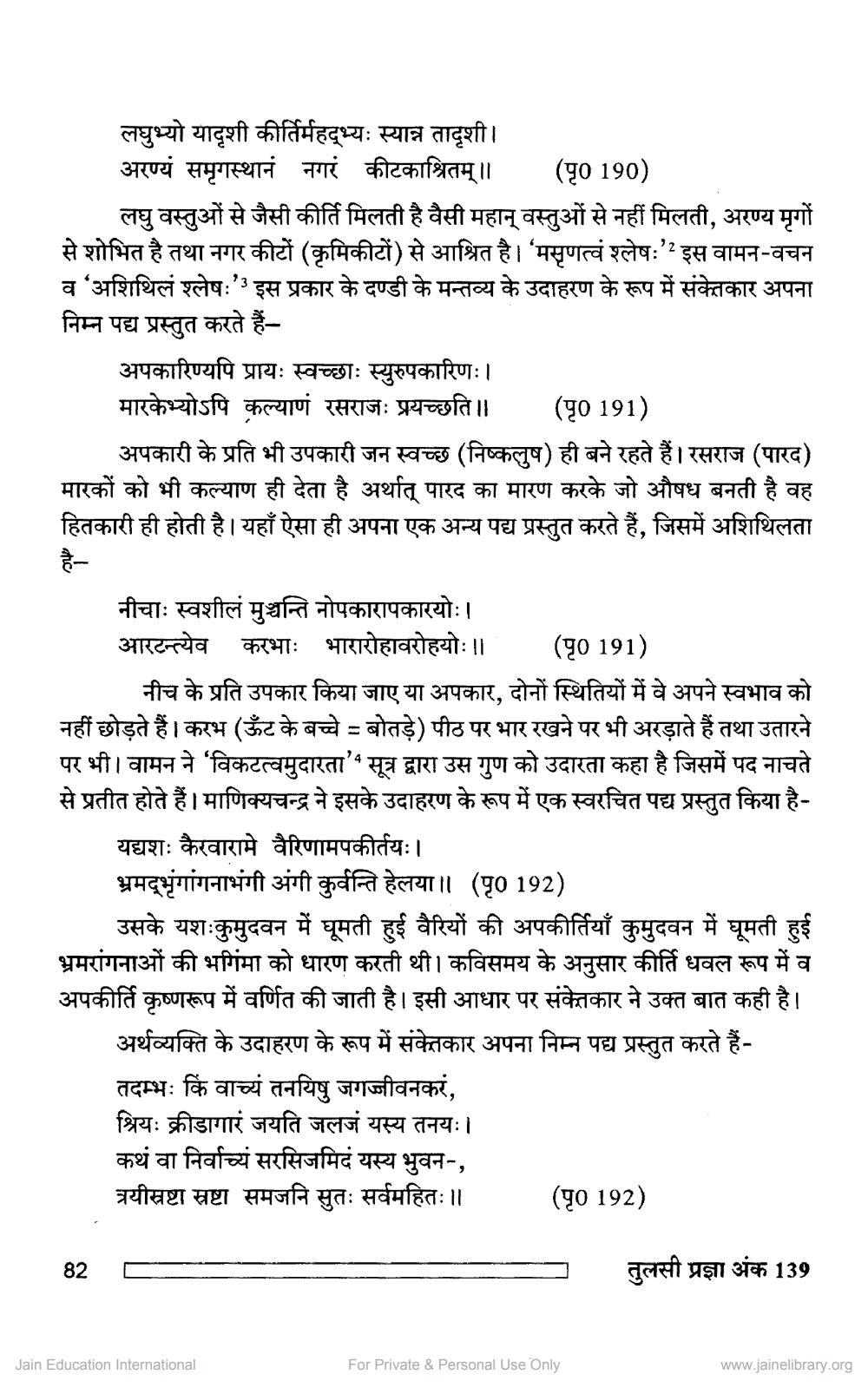________________
लघुभ्यो यादृशी कीर्तिर्महद्भ्यः स्यान्न तादृशी। अरण्यं समृगस्थानं नगरं कीटकाश्रितम्॥ (पृ0 190)
लघु वस्तुओं से जैसी कीर्ति मिलती है वैसी महान् वस्तुओं से नहीं मिलती, अरण्य मृगों से शोभित है तथा नगर कीटों (कृमिकीटों) से आश्रित है। ‘मसृणत्वं श्लेषः' इस वामन-वचन व अशिथिलं श्लेषः' इस प्रकार के दण्डी के मन्तव्य के उदाहरण के रूप में संकेतकार अपना निम्न पद्य प्रस्तुत करते हैं
अपकारिण्यपि प्रायः स्वच्छाः स्युरुपकारिणः। मारकेभ्योऽपि कल्याणं रसराजः प्रयच्छति॥ (पृ0 191)
अपकारी के प्रति भी उपकारी जन स्वच्छ (निष्कलुष) ही बने रहते हैं। रसराज (पारद) मारकों को भी कल्याण ही देता है अर्थात् पारद का मारण करके जो औषध बनती है वह हितकारी ही होती है। यहाँ ऐसा ही अपना एक अन्य पद्य प्रस्तुत करते हैं, जिसमें अशिथिलता
नीचाः स्वशीलं मुञ्चन्ति नोपकारापकारयोः । आरटन्त्येव करभाः भारारोहावरोहयोः।। (पृ0 191)
नीच के प्रति उपकार किया जाए या अपकार, दोनों स्थितियों में वे अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। करभ (ऊँट के बच्चे = बोतड़े) पीठ पर भार रखने पर भी अरड़ाते हैं तथा उतारने पर भी। वामन ने 'विकटत्वमुदारता'' सूत्र द्वारा उस गुण को उदारता कहा है जिसमें पद नाचते से प्रतीत होते हैं। माणिक्यचन्द्र ने इसके उदाहरण के रूप में एक स्वरचित पद्य प्रस्तुत किया है
यद्यशः कैरवारामे वैरिणामपकीर्तयः। भ्रमद्धृगांगनाभंगी अंगी कुर्वन्ति हेलया॥ (पृ0 192)
उसके यशःकुमुदवन में घूमती हुई वैरियों की अपकीर्तियाँ कुमुदवन में घूमती हुई भ्रमरांगनाओं की भगिमा को धारण करती थी। कविसमय के अनुसार कीर्ति धवल रूप में व अपकीर्ति कृष्णरूप में वर्णित की जाती है। इसी आधार पर संकेतकार ने उक्त बात कही है।
अर्थव्यक्ति के उदाहरण के रूप में संकेतकार अपना निम्न पद्य प्रस्तुत करते हैंतदम्भः किं वाच्यं तनयिषु जगजीवनकर, श्रियः क्रीडागारं जयति जलजं यस्य तनयः। कथं वा निर्वाच्यं सरसिजमिदं यस्य भुवन-, त्रयीस्रष्टा स्रष्टा समजनि सुतः सर्वमहितः॥ (पृ0 192)
82
-
-
तुलसी प्रज्ञा अंक 139
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org