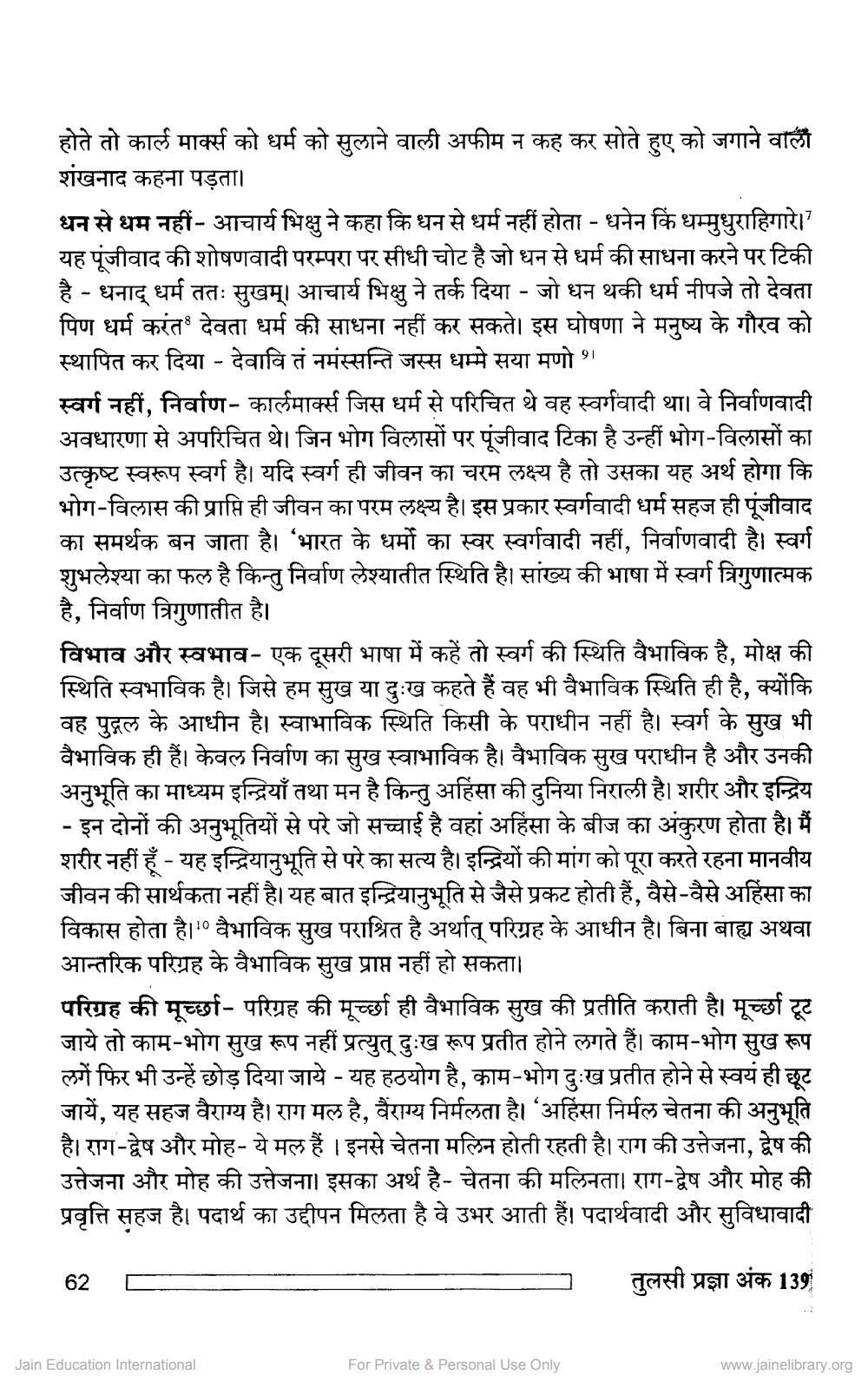________________
होते तो कार्ल मार्क्स को धर्म को सुलाने वाली अफीम न कह कर सोते हुए को जगाने वाली शंखनाद कहना पड़ता। धन से धम नहीं- आचार्य भिक्षु ने कहा कि धन से धर्म नहीं होता - धनेन किं धम्मुधुराहिगारे।' यह पूंजीवाद की शोषणवादी परम्परा पर सीधी चोट है जो धन से धर्म की साधना करने पर टिकी है - धनाद् धर्म ततः सुखम्। आचार्य भिक्षु ने तर्क दिया - जो धन थकी धर्म नीपजे तो देवता पिण धर्म करंत देवता धर्म की साधना नहीं कर सकते। इस घोषणा ने मनुष्य के गौरव को स्थापित कर दिया - देवावि तं नमस्सन्ति जस्स धम्मे सया मणो । स्वर्ग नहीं, निर्वाण- कार्लमार्क्स जिस धर्म से परिचित थे वह स्वर्गवादी था। वे निर्वाणवादी अवधारणा से अपरिचित थे। जिन भोग विलासों पर पूंजीवाद टिका है उन्हीं भोग-विलासों का उत्कृष्ट स्वरूप स्वर्ग है। यदि स्वर्ग ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो उसका यह अर्थ होगा कि भोग-विलास की प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। इस प्रकार स्वर्गवादी धर्म सहज ही पूंजीवाद का समर्थक बन जाता है। भारत के धर्मो का स्वर स्वर्गवादी नहीं, निर्वाणवादी है। स्वर्ग शुभलेश्या का फल है किन्तु निर्वाण लेश्यातीत स्थिति है। सांख्य की भाषा में स्वर्ग त्रिगुणात्मक है, निर्वाण त्रिगुणातीत है। विभाव और स्वभाव- एक दूसरी भाषा में कहें तो स्वर्ग की स्थिति वैभाविक है, मोक्ष की स्थिति स्वभाविक है। जिसे हम सुख या दुःख कहते हैं वह भी वैभाविक स्थिति ही है, क्योंकि वह पुद्गल के आधीन है। स्वाभाविक स्थिति किसी के पराधीन नहीं है। स्वर्ग के सुख भी वैभाविक ही हैं। केवल निर्वाण का सुख स्वाभाविक है। वैभाविक सुख पराधीन है और उनकी अनुभूति का माध्यम इन्द्रियाँ तथा मन है किन्तु अहिंसा की दुनिया निराली है। शरीर और इन्द्रिय - इन दोनों की अनुभूतियों से परे जो सच्चाई है वहां अहिंसा के बीज का अंकुरण होता है। मैं शरीर नहीं हूँ - यह इन्द्रियानुभूति से परे का सत्य है। इन्द्रियों की मांग को पूरा करते रहना मानवीय जीवन की सार्थकता नहीं है। यह बात इन्द्रियानुभूति से जैसे प्रकट होती हैं, वैसे-वैसे अहिंसा का विकास होता है। वैभाविक सुख पराश्रित है अर्थात् परिग्रह के आधीन है। बिना बाह्य अथवा
आन्तरिक परिग्रह के वैभाविक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। परिग्रह की मूर्छा- परिग्रह की मूर्छा ही वैभाविक सुख की प्रतीति कराती है। मूर्छा टूट जाये तो काम-भोग सुख रूप नहीं प्रत्युत् दुःख रूप प्रतीत होने लगते हैं। काम-भोग सुख रूप लगे फिर भी उन्हें छोड़ दिया जाये - यह हठयोग है, काम-भोग दुःख प्रतीत होने से स्वयं ही छूट जायें, यह सहज वैराग्य है। राग मल है, वैराग्य निर्मलता है। 'अहिंसा निर्मल चेतना की अनुभूति है। राग-द्वेष और मोह- ये मल हैं । इनसे चेतना मलिन होती रहती है। राग की उत्तेजना, द्वेष की उत्तेजना और मोह की उत्तेजना। इसका अर्थ है- चेतना की मलिनता। राग-द्वेष और मोह की प्रवृत्ति सहज है। पदार्थ का उद्दीपन मिलता है वे उभर आती हैं। पदार्थवादी और सुविधावादी
62
तुलसी प्रज्ञा अंक 139;
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org