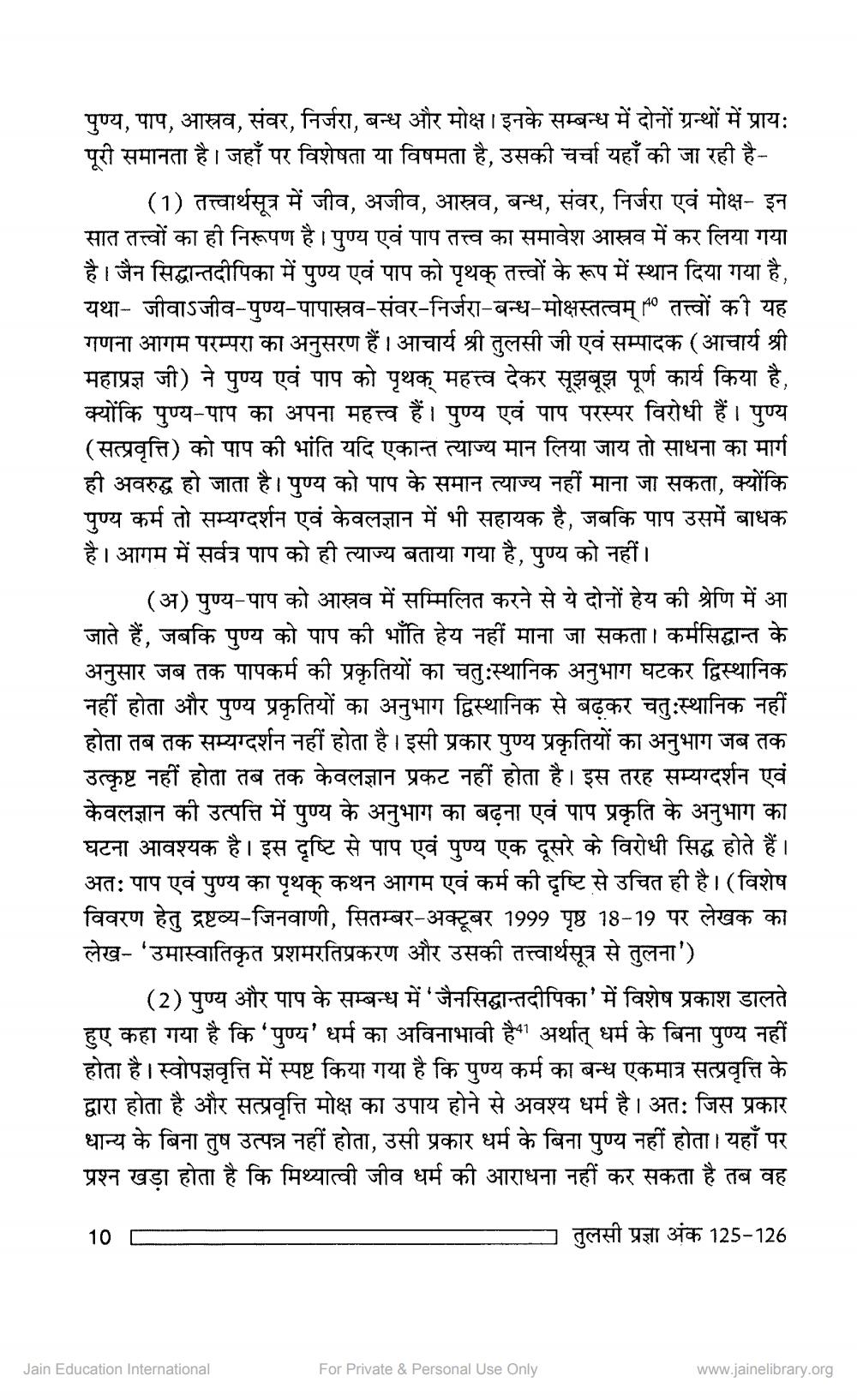________________
पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष । इनके सम्बन्ध में दोनों ग्रन्थों में प्रायः पूरी समानता है । जहाँ पर विशेषता या विषमता है, उसकी चर्चा यहाँ की जा रही है
(1) तत्त्वार्थसूत्र में जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा एवं मोक्ष- इन सात तत्त्वों का ही निरूपण है। पुण्य एवं पाप तत्त्व का समावेश आस्रव में कर लिया गया है। जैन सिद्धान्तदीपिका में पुण्य एवं पाप को पृथक् तत्त्वों के रूप में स्थान दिया गया है, यथा- जीवाऽजीव- - पुण्य-पापास्रव-संवर - निर्जरा- -बन्ध - मोक्षस्तत्वम् | तत्त्वों की यह गणना आगम परम्परा का अनुसरण हैं । आचार्य श्री तुलसी जी एवं सम्पादक (आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी) ने पुण्य एवं पाप को पृथक् महत्त्व देकर सूझबूझ पूर्ण कार्य किया है, क्योंकि पुण्य-पाप का अपना महत्त्व हैं। पुण्य एवं पाप परस्पर विरोधी हैं । पुण्य (सत्प्रवृत्ति) को पाप की भांति यदि एकान्त त्याज्य मान लिया जाय तो साधना का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है। पुण्य को पाप के समान त्याज्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि पुण्य कर्म तो सम्यग्दर्शन एवं केवलज्ञान में भी सहायक है, जबकि पाप उसमें बाधक है । आगम में सर्वत्र पाप को ही त्याज्य बताया गया है, पुण्य को नहीं ।
(अ) पुण्य-पाप को आस्रव में सम्मिलित करने से ये दोनों हेय की श्रेणि में आ जाते हैं, जबकि पुण्य को पाप की भाँति हेय नहीं माना जा सकता । कर्मसिद्धान्त के अनुसार जब तक पापकर्म की प्रकृतियों का चतु:स्थानिक अनुभाग घटकर द्विस्थानिक नहीं होता और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग द्विस्थानिक से बढ़कर चतु:स्थानिक नहीं होता तब तक सम्यग्दर्शन नहीं होता है। इसी प्रकार पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग जब तक उत्कृष्ट नहीं होता तब तक केवलज्ञान प्रकट नहीं होता है । इस तरह सम्यग्दर्शन एवं केवलज्ञान की उत्पत्ति में पुण्य के अनुभाग का बढ़ना एवं पाप प्रकृति के अनुभाग का घटना आवश्यक है । इस दृष्टि से पाप एवं पुण्य एक दूसरे के विरोधी सिद्ध होते हैं । अतः पाप एवं पुण्य का पृथक् कथन आगम एवं कर्म की दृष्टि से उचित ही है । (विशेष विवरण हेतु द्रष्टव्य - जिनवाणी, सितम्बर-अक्टूबर 1999 पृष्ठ 18-19 पर लेखक का लेख- 'उमास्वातिकृत प्रशमरतिप्रकरण और उसकी तत्त्वार्थसूत्र से तुलना ')
(2) पुण्य और पाप के सम्बन्ध में 'जैनसिद्धान्तदीपिका' में विशेष प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि 'पुण्य' धर्म का अविनाभावी है अर्थात् धर्म के बिना पुण्य नहीं होता है । स्वोपज्ञवृत्ति में स्पष्ट किया गया है कि पुण्य कर्म का बन्ध एकमात्र सत्प्रवृत्ति के द्वारा होता है और सत्प्रवृत्ति मोक्ष का उपाय होने से अवश्य धर्म है । अतः जिस प्रकार धान्य के बिना तुष उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार धर्म के बिना पुण्य नहीं होता । यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि मिथ्यात्वी जीव धर्म की आराधना नहीं कर सकता है तब वह
तुलसी प्रज्ञा अंक 125-126
10
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org