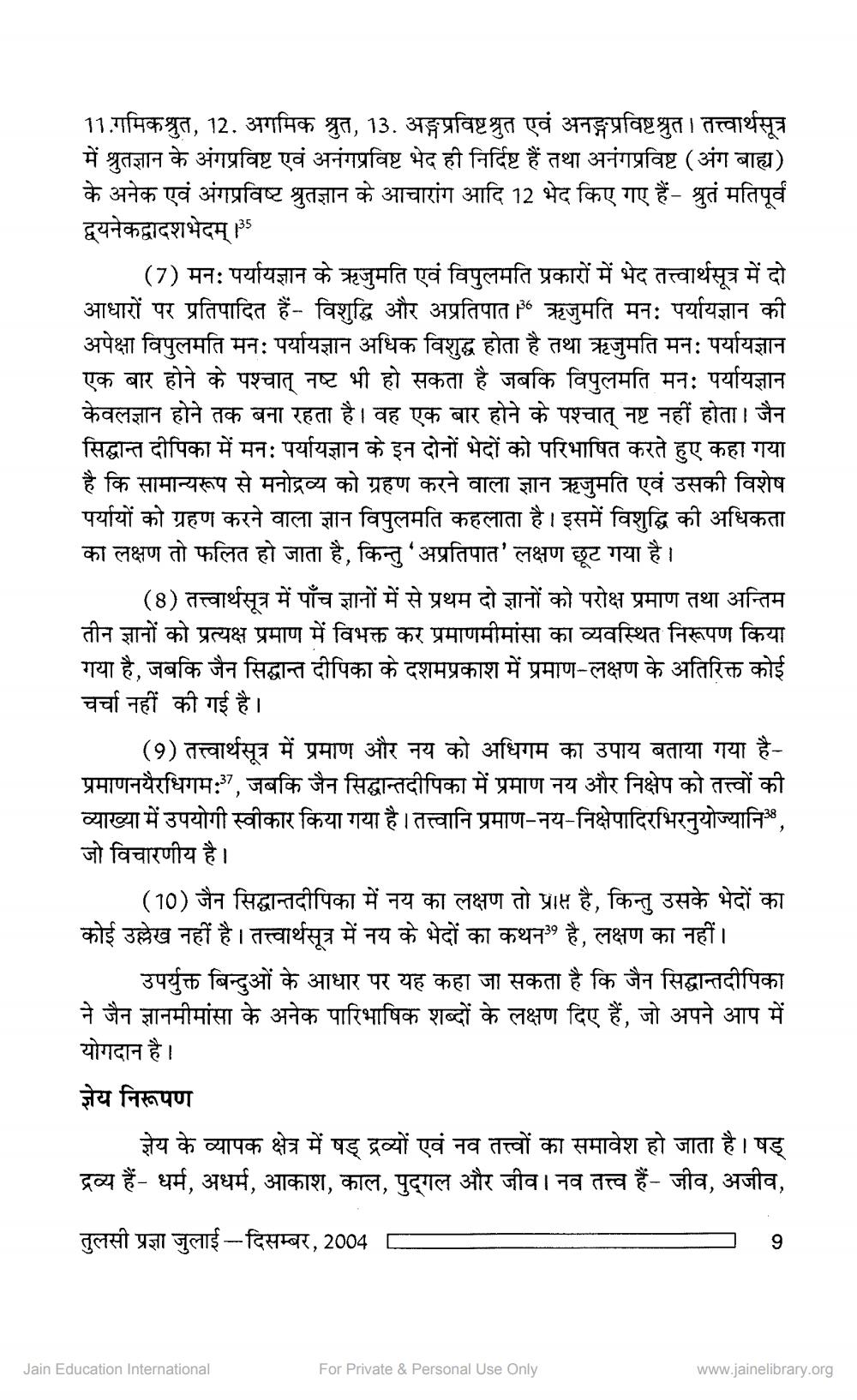________________
11.गमिकश्रुत, 12. अगमिक श्रुत, 13. अङ्गप्रविष्ट श्रुत एवं अनङ्गप्रविष्ट श्रुत। तत्त्वार्थसूत्र में श्रुतज्ञान के अंगप्रविष्ट एवं अनंगप्रविष्ट भेद ही निर्दिष्ट हैं तथा अनंगप्रविष्ट (अंग बाह्य) के अनेक एवं अंगप्रविष्ट श्रुतज्ञान के आचारांग आदि 12 भेद किए गए हैं- श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेकद्वादशभेदम्।
(7) मनः पर्यायज्ञान के ऋजुमति एवं विपुलमति प्रकारों में भेद तत्त्वार्थसूत्र में दो आधारों पर प्रतिपादित हैं- विशुद्धि और अप्रतिपात ऋजुमति मनः पर्यायज्ञान की अपेक्षा विपुलमति मनः पर्यायज्ञान अधिक विशुद्ध होता है तथा ऋजुमति मनः पर्यायज्ञान एक बार होने के पश्चात् नष्ट भी हो सकता है जबकि विपुलमति मनः पर्यायज्ञान केवलज्ञान होने तक बना रहता है। वह एक बार होने के पश्चात् नष्ट नहीं होता। जैन सिद्धान्त दीपिका में मनः पर्यायज्ञान के इन दोनों भेदों को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि सामान्यरूप से मनोद्रव्य को ग्रहण करने वाला ज्ञान ऋजुमति एवं उसकी विशेष पर्यायों को ग्रहण करने वाला ज्ञान विपुलमति कहलाता है। इसमें विशुद्धि की अधिकता का लक्षण तो फलित हो जाता है, किन्तु 'अप्रतिपात' लक्षण छूट गया है।
(8) तत्त्वार्थसूत्र में पाँच ज्ञानों में से प्रथम दो ज्ञानों को परोक्ष प्रमाण तथा अन्तिम तीन ज्ञानों को प्रत्यक्ष प्रमाण में विभक्त कर प्रमाणमीमांसा का व्यवस्थित निरूपण किया गया है, जबकि जैन सिद्धान्त दीपिका के दशमप्रकाश में प्रमाण-लक्षण के अतिरिक्त कोई चर्चा नहीं की गई है।
(9) तत्त्वार्थसूत्र में प्रमाण और नय को अधिगम का उपाय बताया गया हैप्रमाणनयैरधिगमः”, जबकि जैन सिद्धान्तदीपिका में प्रमाण नय और निक्षेप को तत्त्वों की व्याख्या में उपयोगी स्वीकार किया गया है। तत्त्वानि प्रमाण-नय-निक्षेपादिरभिरनुयोज्यानि, जो विचारणीय है।
(10) जैन सिद्धान्तदीपिका में नय का लक्षण तो प्राप्त है, किन्तु उसके भेदों का कोई उल्लेख नहीं है। तत्त्वार्थसूत्र में नय के भेदों का कथन है, लक्षण का नहीं।
उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जैन सिद्धान्तदीपिका ने जैन ज्ञानमीमांसा के अनेक पारिभाषिक शब्दों के लक्षण दिए हैं, जो अपने आप में योगदान है। ज्ञेय निरूपण
ज्ञेय के व्यापक क्षेत्र में षड् द्रव्यों एवं नव तत्त्वों का समावेश हो जाता है। षड् द्रव्य हैं- धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। नव तत्त्व हैं- जीव, अजीव,
तुलसी प्रज्ञा जुलाई-दिसम्बर, 2004
-
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org