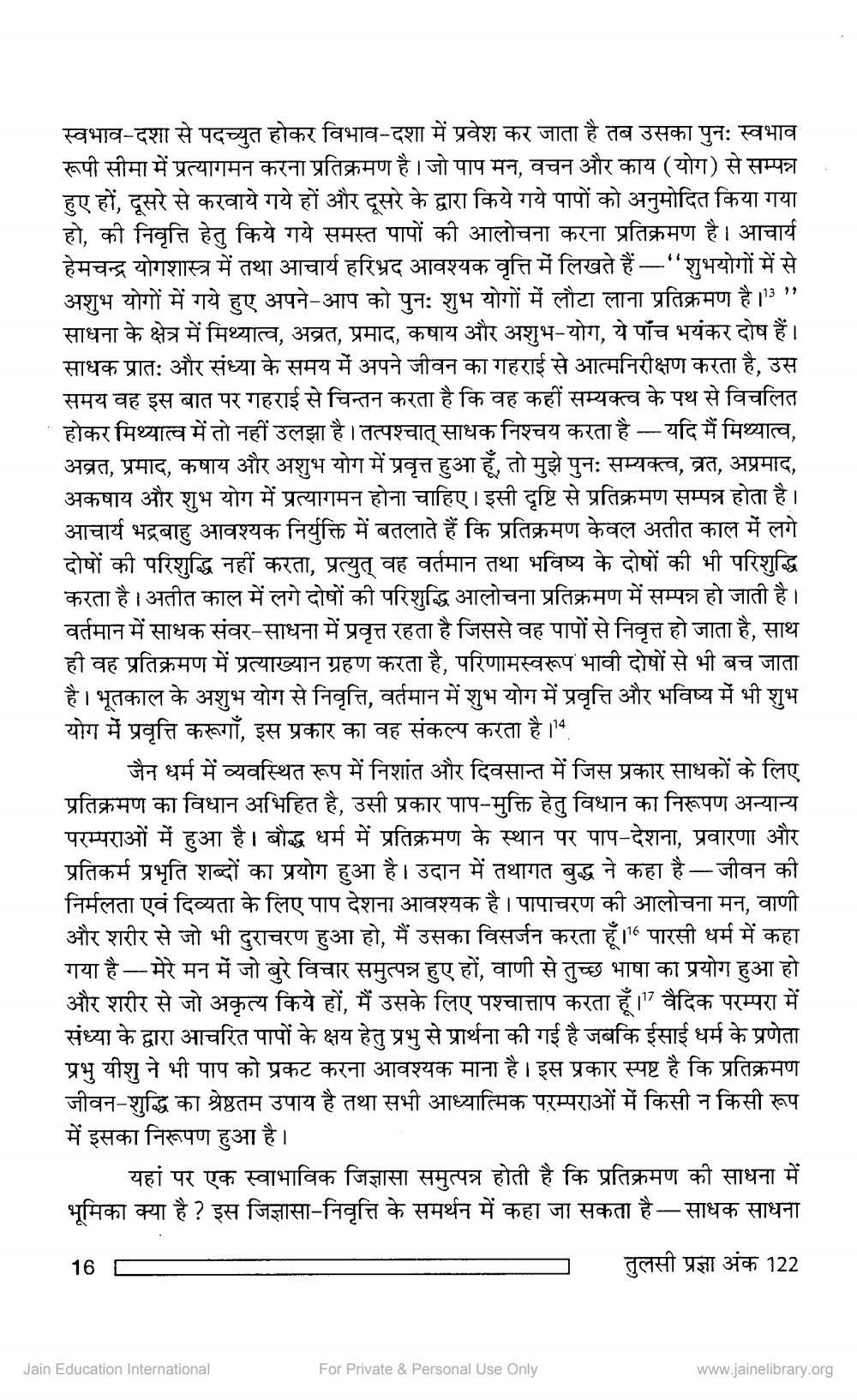________________
I
11
स्वभाव - दशा से पदच्युत होकर विभाव- दशा में प्रवेश कर जाता है तब उसका पुनः स्वभाव रूपी सीमा में प्रत्यागमन करना प्रतिक्रमण है । जो पाप मन, वचन और काय (योग) से सम्पन्न हुए हों, दूसरे से करवाये गये हों और दूसरे के द्वारा किये गये पापों को अनुमोदित किया गया हो, की निवृत्ति हेतु किये गये समस्त पापों की आलोचना करना प्रतिक्रमण है। आचार्य हेमचन्द्र योगशास्त्र में तथा आचार्य हरिभ्रद आवश्यक वृत्ति में लिखते हैं – “शुभयोगों में से अशुभ योगों में गये हुए अपने-आप को पुनः शुभ योगों में लौटा लाना प्रतिक्रमण है। 3 साधना के क्षेत्र में मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग, ये पाँच भयंकर दोष हैं। साधक प्रात: और संध्या के समय में अपने जीवन का गहराई से आत्मनिरीक्षण करता है, उस समय वह इस बात पर गहराई से चिन्तन करता है कि वह कहीं सम्यक्त्व के पथ से विचलित होकर मिथ्यात्व में तो नहीं उलझा है । तत्पश्चात् साधक निश्चय करता है – यदि मैं मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग में प्रवृत्त हुआ हूँ, तो मुझे पुनः सम्यक्त्व, व्रत, अप्रमाद, अकषाय और शुभ योग में प्रत्यागमन होना चाहिए। इसी दृष्टि से प्रतिक्रमण सम्पन्न होता है। आचार्य भद्रबाहु आवश्यक निर्युक्ति में बतलाते हैं कि प्रतिक्रमण केवल अतीत काल में लगे दोषों की परिशुद्धि नहीं करता, प्रत्युत् वह वर्तमान तथा भविष्य के दोषों की भी परिशुद्धि करता है । अतीत काल में लगे दोषों की परिशुद्धि आलोचना प्रतिक्रमण में सम्पन्न हो जाती है । वर्तमान में साधक संवर-साधना में प्रवृत्त रहता है जिससे वह पापों से निवृत्त हो जाता है, साथ ही वह प्रतिक्रमण में प्रत्याख्यान ग्रहण करता है, परिणामस्वरूप भावी दोषों से भी बच जाता भूतकाल के अशुभ योग से निवृत्ति, वर्तमान में शुभ योग में प्रवृत्ति और भविष्य में भी शुभ योग में प्रवृत्ति करूगाँ, इस प्रकार का वह संकल्प करता है। 14.
-
जैन धर्म में व्यवस्थित रूप में निशांत और दिवसान्त में जिस प्रकार साधकों के लिए प्रतिक्रमण का विधान अभिहित है, उसी प्रकार पाप मुक्ति हेतु विधान का निरूपण अन्यान्य परम्पराओं में हुआ है। बौद्ध धर्म में प्रतिक्रमण के स्थान पर पाप - देशना, प्रवारणा और प्रतिकर्म प्रभृति शब्दों का प्रयोग हुआ है । उदान में तथागत बुद्ध ने कहा है – जीवन की निर्मलता एवं दिव्यता के लिए पाप देशना आवश्यक है । पापाचरण की आलोचना मन, वाणी और शरीर से जो भी दुराचरण हुआ हो, मैं उसका विसर्जन करता हूँ ।" पारसी धर्म में कहा गया है – मेरे मन में जो बुरे विचार समुत्पन्न हुए हों, वाणी से तुच्छ भाषा का प्रयोग हुआ हो और शरीर से जो अकृत्य किये हों, मैं उसके लिए पश्चात्ताप करता हूँ।” वैदिक परम्परा में संध्या के द्वारा आचरित पापों के क्षय हेतु प्रभु से प्रार्थना की गई है जबकि ईसाई धर्म के प्रणेता प्रभु यीशु ने भी पाप को प्रकट करना आवश्यक माना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिक्रमण जीवन-शुद्धि का श्रेष्ठतम उपाय है तथा सभी आध्यात्मिक परम्पराओं में किसी न किसी रूप में इसका निरूपण हुआ है।
--
यहां पर एक स्वाभाविक जिज्ञासा समुत्पन्न होती है कि प्रतिक्रमण की साधना में भूमिका क्या है ? इस जिज्ञासा - निवृत्ति के समर्थन में कहा जा सकता है
तुलसी प्रज्ञा अंक 122
16
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
-
- साधक साधना
www.jainelibrary.org