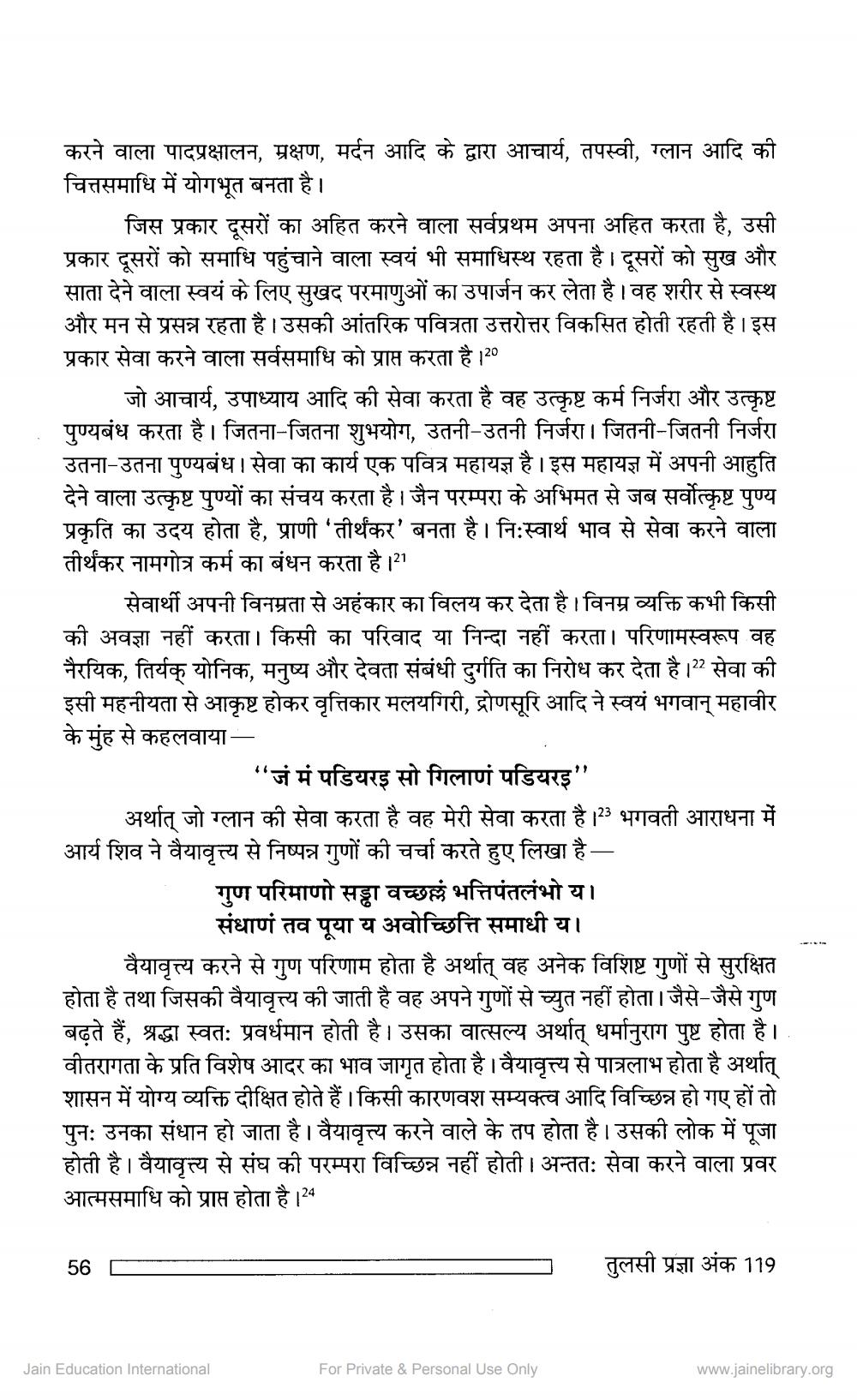________________
करने वाला पादप्रक्षालन, प्रक्षण, मर्दन आदि के द्वारा आचार्य, तपस्वी, ग्लान आदि की चित्तसमाधि में योगभूत बनता है ।
जिस प्रकार दूसरों का अहित करने वाला सर्वप्रथम अपना अहित करता है, उसी प्रकार दूसरों को समाधि पहुंचाने वाला स्वयं भी समाधिस्थ रहता है। दूसरों को सुख और साता देने वाला स्वयं के लिए सुखद परमाणुओं का उपार्जन कर लेता है। वह शरीर से स्वस्थ और मन से प्रसन्न रहता है। उसकी आंतरिक पवित्रता उत्तरोत्तर विकसित होती रहती है । इस प्रकार सेवा करने वाला सर्वसमाधि को प्राप्त करता है | 20
जो आचार्य, उपाध्याय आदि की सेवा करता है वह उत्कृष्ट कर्म निर्जरा और उत्कृष्ट पुण्यबंध करता है । जितना - जितना शुभयोग, उतनी - उतनी निर्जरा । जितनी - जितनी निर्जरा उतना-उतना पुण्यबंध। सेवा का कार्य एक पवित्र महायज्ञ है। इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने वाला उत्कृष्ट पुण्यों का संचय करता है। जैन परम्परा के अभिमत से जब सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति का उदय होता है, प्राणी 'तीर्थंकर' बनता है । निःस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला तीर्थंकर नामगोत्र कर्म का बंधन करता है । 21
सेवार्थी अपनी विनम्रता से अहंकार का विलय कर देता है। विनम्र व्यक्ति कभी किसी की अवज्ञा नहीं करता। किसी का परिवाद या निन्दा नहीं करता । परिणामस्वरूप वह नैरयिक, तिर्यक् योनिक, मनुष्य और देवता संबंधी दुर्गति का निरोध कर देता है। 22 सेवा की महनीयता से आकृष्ट होकर वृत्तिकार मलयगिरी, द्रोणसूरि आदि ने स्वयं भगवान् महावीर के मुंह से कहलवाया
"जं मं पडियरइ सो गिलाणं पडियरइ "
अर्थात् जो ग्लान की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। 23 भगवती आराधना में आर्य शिव ने वैयावृत्त्य से निष्पन्न गुणों की चर्चा करते हुए लिखा है
वैयावृत्त्य करने से गुण परिणाम होता है अर्थात् वह अनेक विशिष्ट गुणों से सुरक्षित होता है तथा जिसकी वैयावृत्त्य की जाती है वह अपने गुणों से च्युत नहीं होता । जैसे-जैसे गुण बढ़ते हैं, श्रद्धा स्वतः प्रवर्धमान होती है । उसका वात्सल्य अर्थात् धर्मानुराग पुष्ट होता है । वीतरागता के प्रति विशेष आदर का भाव जागृत होता है। वैयावृत्त्य से पात्रलाभ होता है अर्थात् शासन में योग्य व्यक्ति दीक्षित होते हैं। किसी कारणवश सम्यक्त्व आदि विच्छिन्न हो गए हों तो पुनः उनका संधान हो जाता है । वैयावृत्त्य करने वाले के तप होता है । उसकी लोक में पूजा होती है। वैयावृत्त्य से संघ की परम्परा विच्छिन्न नहीं होती । अन्ततः सेवा करने वाला प्रवर आत्मसमाधि को प्राप्त होता है। 24
56
गुण परिमाणो सड्ढा वच्छल्लं भत्तिपंतलंभो य । संध व या अवोच्छित्ति समाधी य ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
तुलसी प्रज्ञा अंक 119
www.jainelibrary.org