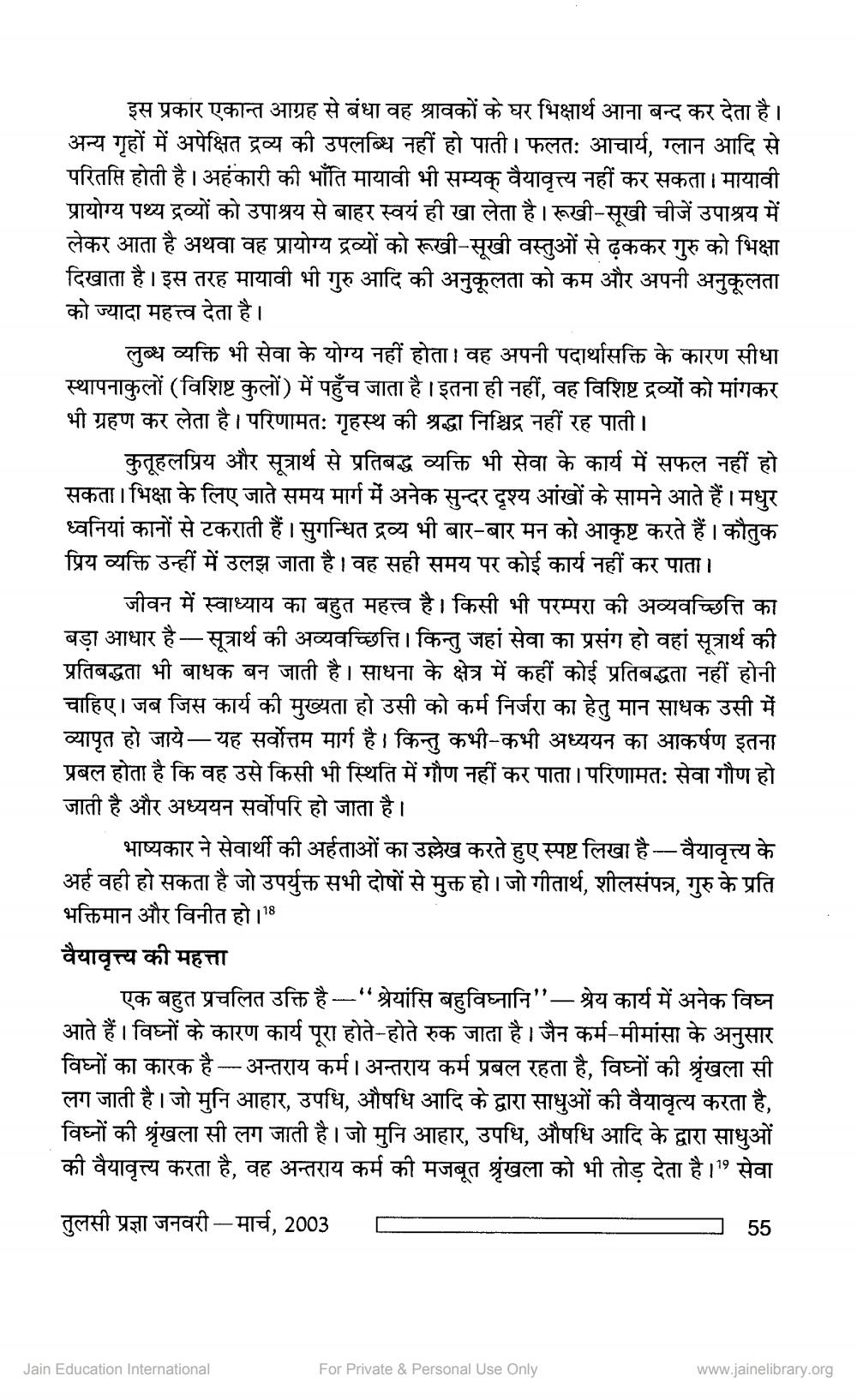________________
इस प्रकार एकान्त आग्रह से बंधा वह श्रावकों के घर भिक्षार्थ आना बन्द कर देता है। अन्य गृहों में अपेक्षित द्रव्य की उपलब्धि नहीं हो पाती। फलतः आचार्य, ग्लान आदि से परितप्ति होती है। अहंकारी की भाँति मायावी भी सम्यक् वैयावृत्त्य नहीं कर सकता। मायावी प्रायोग्य पथ्य द्रव्यों को उपाश्रय से बाहर स्वयं ही खा लेता है। रूखी-सूखी चीजें उपाश्रय में लेकर आता है अथवा वह प्रायोग्य द्रव्यों को रूखी-सूखी वस्तुओं से ढ़ककर गुरु को भिक्षा दिखाता है। इस तरह मायावी भी गुरु आदि की अनुकूलता को कम और अपनी अनुकूलता को ज्यादा महत्त्व देता है।
लुब्ध व्यक्ति भी सेवा के योग्य नहीं होता। वह अपनी पदार्थासक्ति के कारण सीधा स्थापनाकुलों (विशिष्ट कुलों) में पहुँच जाता है। इतना ही नहीं, वह विशिष्ट द्रव्यों को मांगकर भी ग्रहण कर लेता है। परिणामतः गृहस्थ की श्रद्धा निश्चिद्र नहीं रह पाती।
कुतूहलप्रिय और सूत्रार्थ से प्रतिबद्ध व्यक्ति भी सेवा के कार्य में सफल नहीं हो सकता। भिक्षा के लिए जाते समय मार्ग में अनेक सुन्दर दृश्य आंखों के सामने आते हैं। मधुर ध्वनियां कानों से टकराती हैं। सुगन्धित द्रव्य भी बार-बार मन को आकृष्ट करते हैं। कौतुक प्रिय व्यक्ति उन्हीं में उलझ जाता है। वह सही समय पर कोई कार्य नहीं कर पाता।
जीवन में स्वाध्याय का बहुत महत्त्व है। किसी भी परम्परा की अव्यवच्छित्ति का बड़ा आधार है- सूत्रार्थ की अव्यवच्छित्ति। किन्तु जहां सेवा का प्रसंग हो वहां सूत्रार्थ की प्रतिबद्धता भी बाधक बन जाती है। साधना के क्षेत्र में कहीं कोई प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए। जब जिस कार्य की मुख्यता हो उसी को कर्म निर्जरा का हेतु मान साधक उसी में व्याप्त हो जाये- यह सर्वोत्तम मार्ग है। किन्तु कभी-कभी अध्ययन का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि वह उसे किसी भी स्थिति में गौण नहीं कर पाता। परिणामतः सेवा गौण हो जाती है और अध्ययन सर्वोपरि हो जाता है।
भाष्यकार ने सेवार्थी की अर्हताओं का उल्लेख करते हुए स्पष्ट लिखा है- वैयावृत्त्य के अर्ह वही हो सकता है जो उपर्युक्त सभी दोषों से मुक्त हो। जो गीतार्थ, शीलसंपन्न, गुरु के प्रति भक्तिमान और विनीत हो। वैयावृत्त्य की महत्ता
___ एक बहुत प्रचलित उक्ति है --- "श्रेयांसि बहुविघ्नानि"- श्रेय कार्य में अनेक विघ्न आते हैं। विघ्नों के कारण कार्य पूरा होते-होते रुक जाता है। जैन कर्म-मीमांसा के अनुसार विघ्नों का कारक है --- अन्तराय कर्म। अन्तराय कर्म प्रबल रहता है, विघ्नों की श्रृंखला सी लग जाती है। जो मुनि आहार, उपधि, औषधि आदि के द्वारा साधुओं की वैयावृत्य करता है, विघ्नों की श्रृंखला सी लग जाती है। जो मुनि आहार, उपधि, औषधि आदि के द्वारा साधुओं की वैयावृत्त्य करता है, वह अन्तराय कर्म की मजबूत श्रृंखला को भी तोड़ देता है।' सेवा
तुलसी प्रज्ञा जनवरी-मार्च, 2003
-
55
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org