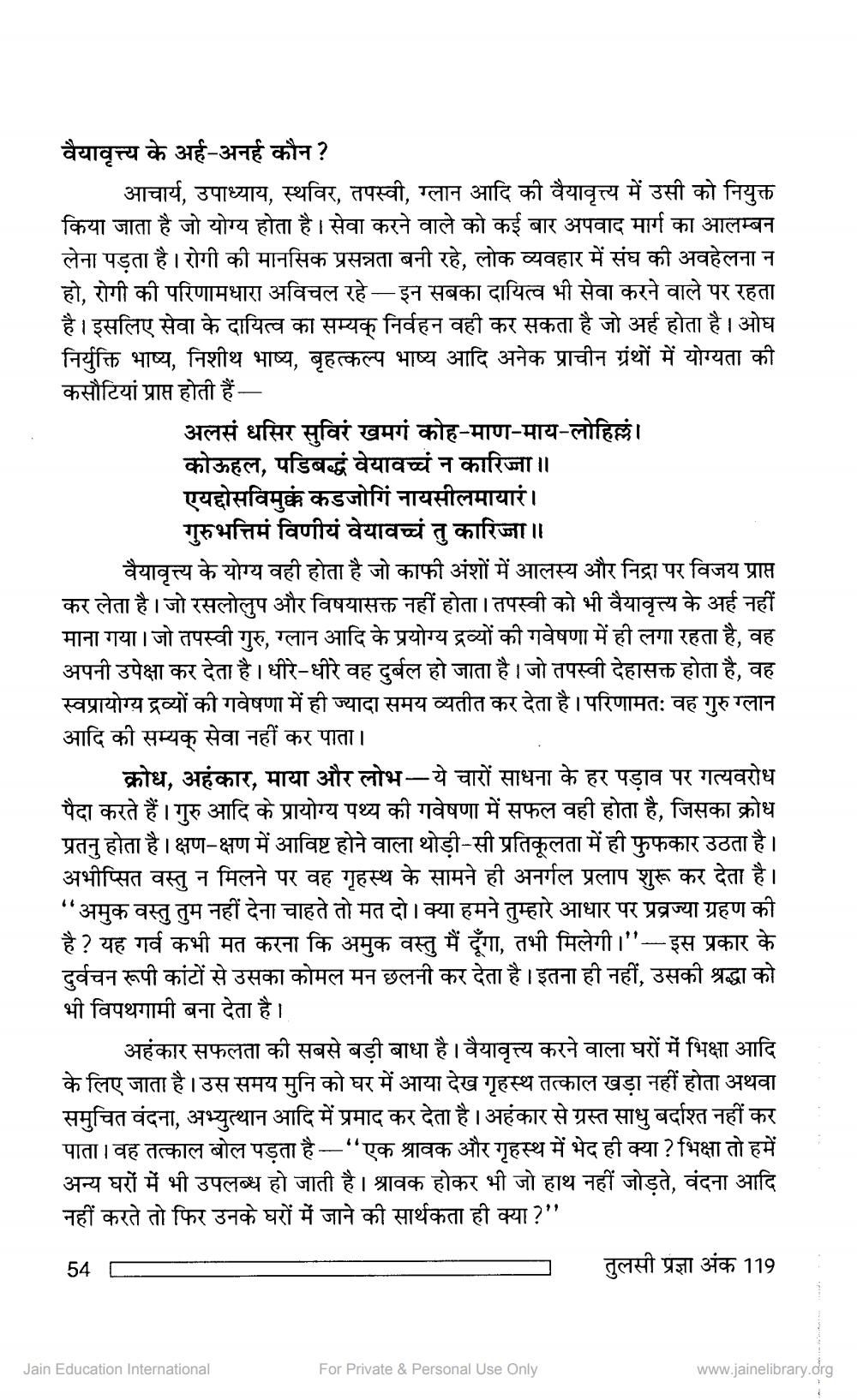________________
वैयावृत्त्य के अर्ह-अनर्ह कौन?
आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, ग्लान आदि की वैयावृत्त्य में उसी को नियुक्त किया जाता है जो योग्य होता है। सेवा करने वाले को कई बार अपवाद मार्ग का आलम्बन लेना पड़ता है। रोगी की मानसिक प्रसन्नता बनी रहे, लोक व्यवहार में संघ की अवहेलना न हो, रोगी की परिणामधारा अविचल रहे- इन सबका दायित्व भी सेवा करने वाले पर रहता है। इसलिए सेवा के दायित्व का सम्यक् निर्वहन वही कर सकता है जो अर्ह होता है । ओघ नियुक्ति भाष्य, निशीथ भाष्य, बृहत्कल्प भाष्य आदि अनेक प्राचीन ग्रंथों में योग्यता की कसौटियां प्राप्त होती हैं
अलसं धसिर सुविरं खमगं कोह-माण-माय-लोहिल्लं। कोऊहल, पडिबद्धं वेयावच्चं न कारिज्जा॥ एयद्दोसविमुक्कं कडजोगिं नायसीलमायारं।
गुरुभत्तिमं विणीयं वेयावच्चं तु कारिजा॥ वैयावृत्त्य के योग्य वही होता है जो काफी अंशों में आलस्य और निद्रा पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो रसलोलुप और विषयासक्त नहीं होता। तपस्वी को भी वैयावृत्त्य के अर्ह नहीं माना गया। जो तपस्वी गुरु, ग्लान आदि के प्रयोग्य द्रव्यों की गवेषणा में ही लगा रहता है, वह अपनी उपेक्षा कर देता है। धीरे-धीरे वह दुर्बल हो जाता है । जो तपस्वी देहासक्त होता है, वह स्वप्रायोग्य द्रव्यों की गवेषणा में ही ज्यादा समय व्यतीत कर देता है। परिणामतः वह गुरु ग्लान आदि की सम्यक् सेवा नहीं कर पाता।।
क्रोध, अहंकार, माया और लोभ-ये चारों साधना के हर पड़ाव पर गत्यवरोध पैदा करते हैं। गुरु आदि के प्रायोग्य पथ्य की गवेषणा में सफल वही होता है, जिसका क्रोध प्रतनु होता है। क्षण-क्षण में आविष्ट होने वाला थोड़ी-सी प्रतिकूलता में ही फुफकार उठता है। अभीप्सित वस्तु न मिलने पर वह गृहस्थ के सामने ही अनर्गल प्रलाप शुरू कर देता है। "अमुक वस्तु तुम नहीं देना चाहते तो मत दो। क्या हमने तुम्हारे आधार पर प्रव्रज्या ग्रहण की है? यह गर्व कभी मत करना कि अमुक वस्तु मैं दूंगा, तभी मिलेगी।"- इस प्रकार के दुर्वचन रूपी कांटों से उसका कोमल मन छलनी कर देता है। इतना ही नहीं, उसकी श्रद्धा को भी विपथगामी बना देता है।
अहंकार सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। वैयावृत्त्य करने वाला घरों में भिक्षा आदि के लिए जाता है। उस समय मुनि को घर में आया देख गृहस्थ तत्काल खड़ा नहीं होता अथवा समुचित वंदना, अभ्युत्थान आदि में प्रमाद कर देता है । अहंकार से ग्रस्त साधु बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह तत्काल बोल पड़ता है -"एक श्रावक और गृहस्थ में भेद ही क्या? भिक्षा तो हमें अन्य घरों में भी उपलब्ध हो जाती है। श्रावक होकर भी जो हाथ नहीं जोड़ते, वंदना आदि नहीं करते तो फिर उनके घरों में जाने की सार्थकता ही क्या?" 540
- तुलसी प्रज्ञा अंक 119
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org