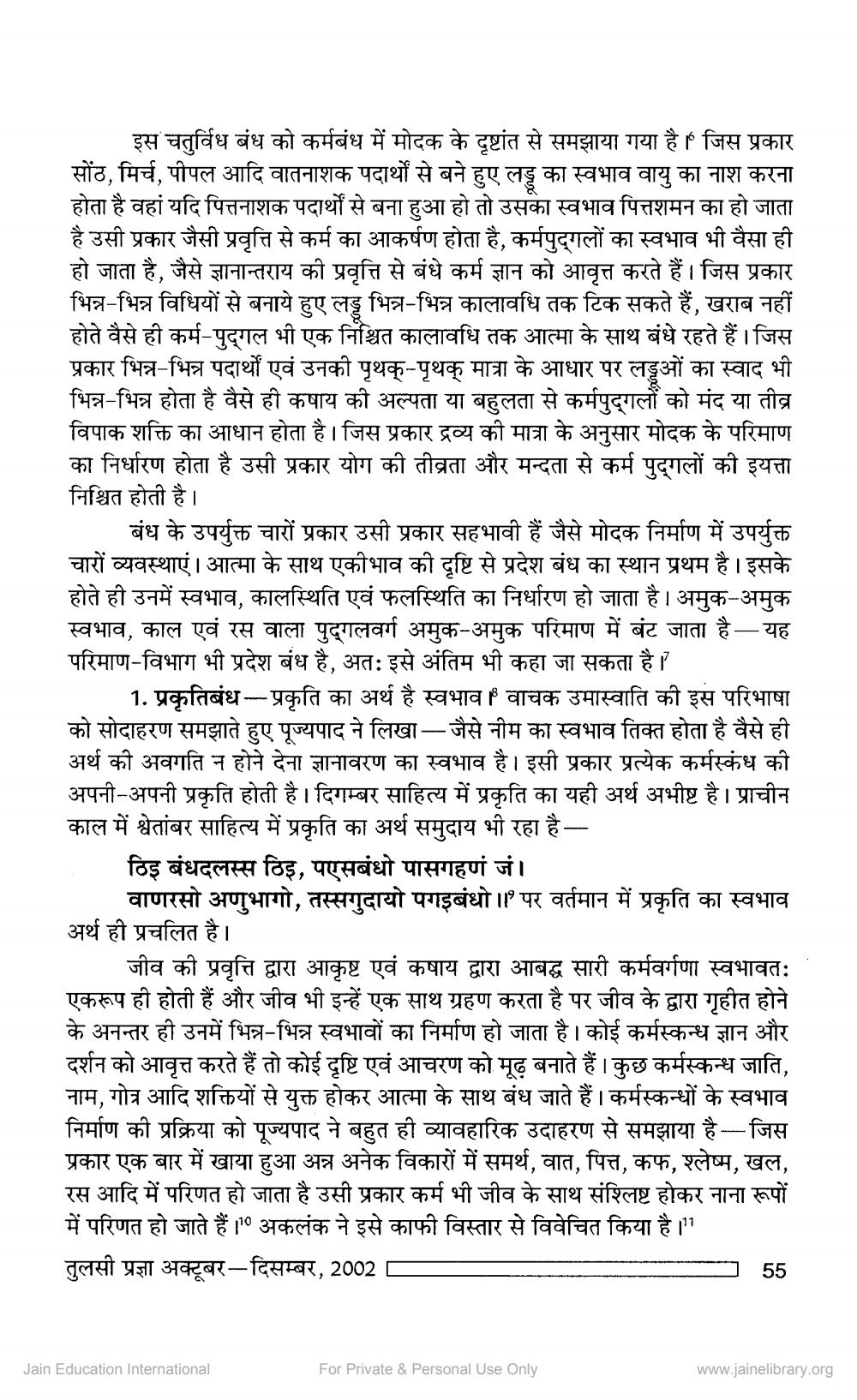________________
इस चतुर्विध बंध को कर्मबंध में मोदक के दृष्टांत से समझाया गया है। जिस प्रकार सोंठ, मिर्च, पीपल आदि वातनाशक पदार्थों से बने हुए लड्ड का स्वभाव वायु का नाश करना होता है वहां यदि पित्तनाशक पदार्थों से बना हुआ हो तो उसका स्वभाव पित्तशमन का हो जाता है उसी प्रकार जैसी प्रवृत्ति से कर्म का आकर्षण होता है, कर्मपुद्गलों का स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है, जैसे ज्ञानान्तराय की प्रवृत्ति से बंधे कर्म ज्ञान को आवृत्त करते हैं। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न विधियों से बनाये हुए लड्ड भिन्न-भिन्न कालावधि तक टिक सकते हैं, खराब नहीं होते वैसे ही कर्म-पुद्गल भी एक निश्चित कालावधि तक आत्मा के साथ बंधे रहते हैं। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न पदार्थों एवं उनकी पृथक्-पृथक् मात्रा के आधार पर लड्डुओं का स्वाद भी भिन्न-भिन्न होता है वैसे ही कषाय की अल्पता या बहुलता से कर्मपुद्गलौ को मंद या तीव्र विपाक शक्ति का आधान होता है। जिस प्रकार द्रव्य की मात्रा के अनुसार मोदक के परिमाण का निर्धारण होता है उसी प्रकार योग की तीव्रता और मन्दता से कर्म पुद्गलों की इयत्ता निश्चित होती है।
बंध के उपर्युक्त चारों प्रकार उसी प्रकार सहभावी हैं जैसे मोदक निर्माण में उपर्युक्त चारों व्यवस्थाएं। आत्मा के साथ एकीभाव की दृष्टि से प्रदेश बंध का स्थान प्रथम है। इसके होते ही उनमें स्वभाव, कालस्थिति एवं फलस्थिति का निर्धारण हो जाता है। अमुक-अमुक स्वभाव, काल एवं रस वाला पुद्गलवर्ग अमुक-अमुक परिमाण में बंट जाता है— यह परिमाण-विभाग भी प्रदेश बंध है, अतः इसे अंतिम भी कहा जा सकता है।
1. प्रकृतिबंध-प्रकृति का अर्थ है स्वभावा वाचक उमास्वाति की इस परिभाषा को सोदाहरण समझाते हुए पूज्यपाद ने लिखा-जैसे नीम का स्वभाव तिक्त होता है वैसे ही अर्थ की अवगति न होने देना ज्ञानावरण का स्वभाव है। इसी प्रकार प्रत्येक कर्मस्कंध की अपनी-अपनी प्रकृति होती है। दिगम्बर साहित्य में प्रकृति का यही अर्थ अभीष्ट है। प्राचीन काल में श्वेतांबर साहित्य में प्रकृति का अर्थ समुदाय भी रहा है
ठिइ बंधदलस्स ठिइ, पएसबंधो पासगहणं जं।
वाणरसो अणुभागो, तस्सगुदायो पगइबंधो॥' पर वर्तमान में प्रकृति का स्वभाव अर्थ ही प्रचलित है।
जीव की प्रवृत्ति द्वारा आकृष्ट एवं कषाय द्वारा आबद्ध सारी कर्मवर्गणा स्वभावतः एकरूप ही होती हैं और जीव भी इन्हें एक साथ ग्रहण करता है पर जीव के द्वारा गृहीत होने के अनन्तर ही उनमें भिन्न-भिन्न स्वभावों का निर्माण हो जाता है। कोई कर्मस्कन्ध ज्ञान और दर्शन को आवृत्त करते हैं तो कोई दृष्टि एवं आचरण को मूढ़ बनाते हैं। कुछ कर्मस्कन्ध जाति, नाम, गोत्र आदि शक्तियों से युक्त होकर आत्मा के साथ बंध जाते हैं। कर्मस्कन्धों के स्वभाव निर्माण की प्रक्रिया को पूज्यपाद ने बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझाया है-जिस प्रकार एक बार में खाया हुआ अन्न अनेक विकारों में समर्थ, वात, पित्त, कफ, श्लेष्म, खल, रस आदि में परिणत हो जाता है उसी प्रकार कर्म भी जीव के साथ संश्लिष्ट होकर नाना रूपों में परिणत हो जाते हैं। अकलंक ने इसे काफी विस्तार से विवेचित किया है।" तुलसी प्रज्ञा अक्टूबर-दिसम्बर, 2002 0
-
55
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org