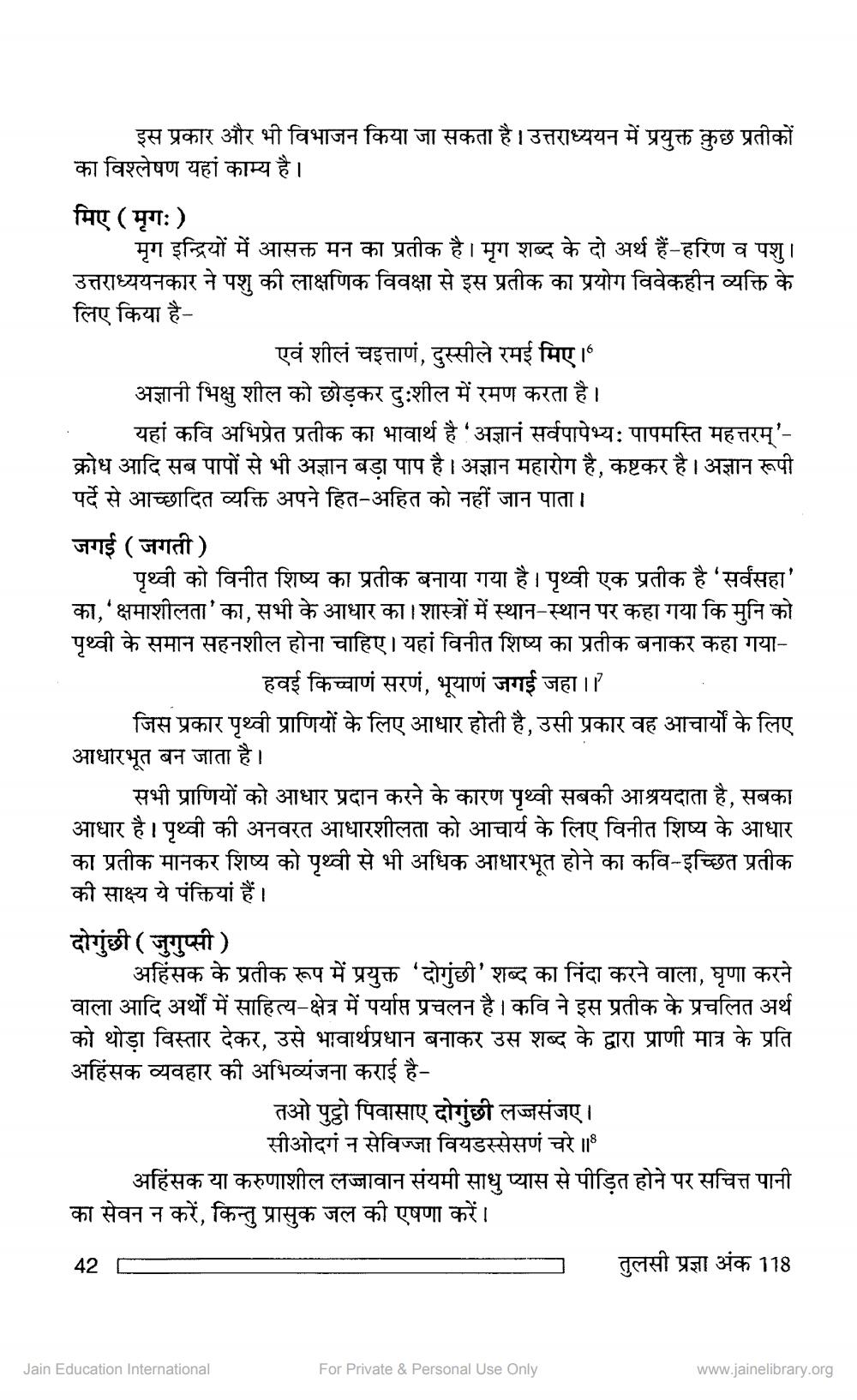________________
इस प्रकार और भी विभाजन किया जा सकता है। उत्तराध्ययन में प्रयुक्त कुछ प्रतीकों का विश्लेषण यहां काम्य है ।
मिए (मृग: )
मृग इन्द्रियों में आसक्त मन का प्रतीक है। मृग शब्द के दो अर्थ हैं - हरिण व पशु । उत्तराध्ययनकार ने पशु की लाक्षणिक विवक्षा से इस प्रतीक का प्रयोग विवेकहीन व्यक्ति के लिए किया है
एवं शीलं चइत्ताणं, दुस्सीले रमई मिए । '
अज्ञानी भिक्षु शील को छोड़कर दुःशील में रमण करता है।
यहां कवि अभिप्रेत प्रतीक का भावार्थ है 'अज्ञानं सर्वपापेभ्यः पापमस्ति महत्तरम्'क्रोध आदि सब पापों से भी अज्ञान बड़ा पाप है। अज्ञान महारोग है, कष्टकर है। अज्ञान रूपी पर्दे से आच्छादित व्यक्ति अपने हित-अहित को नहीं जान पाता ।
जगई (जगती )
पृथ्वी को विनीत शिष्य का प्रतीक बनाया गया है। पृथ्वी एक प्रतीक है 'सर्वंसहा ' का, 'क्षमाशीलता' का, सभी के आधार का । शास्त्रों में स्थान-स्थान पर कहा गया कि मुनि को पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। यहां विनीत शिष्य का प्रतीक बनाकर कहा गयाहवई किच्चाणं सरणं, भूयाणं जगई जहा ।।
जिस प्रकार पृथ्वी प्राणियों के लिए आधार होती है, उसी प्रकार वह आचार्यों के लिए आधारभूत बन जाता है ।
सभी प्राणियों को आधार प्रदान करने के कारण पृथ्वी सबकी आश्रयदाता है, सबका आधार है। पृथ्वी की अनवरत आधारशीलता को आचार्य के लिए विनीत शिष्य के आधार का प्रतीक मानकर शिष्य को पृथ्वी से भी अधिक आधारभूत होने का कवि - इच्छित प्रतीक की साक्ष्य ये पंक्तियां हैं ।
दोगुंछी (जुगुप्सी)
अहिंसक के प्रतीक रूप में प्रयुक्त 'दोगुंछी' शब्द का निंदा करने वाला, घृणा करने वाला आदि अर्थों में साहित्य-क्षेत्र में पर्याप्त प्रचलन है । कवि ने इस प्रतीक के प्रचलित अर्थ को थोड़ा विस्तार देकर, उसे भावार्थप्रधान बनाकर उस शब्द के द्वारा प्राणी मात्र के प्रति अहिंसक व्यवहार की अभिव्यंजना कराई है -
अहिंसक या करुणाशील लज्जावान संयमी साधु प्यास से पीड़ित होने पर सचित्त पानी का सेवन न करें, किन्तु प्रासुक जल की एषणा करें।
42
तओ पुट्ठो पिवासाए दोगुंछी लज्जसंजए । सीओदगं न सेविज्जा वियडस्सेसणं चरे ॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
तुलसी प्रज्ञा अंक 118
www.jainelibrary.org