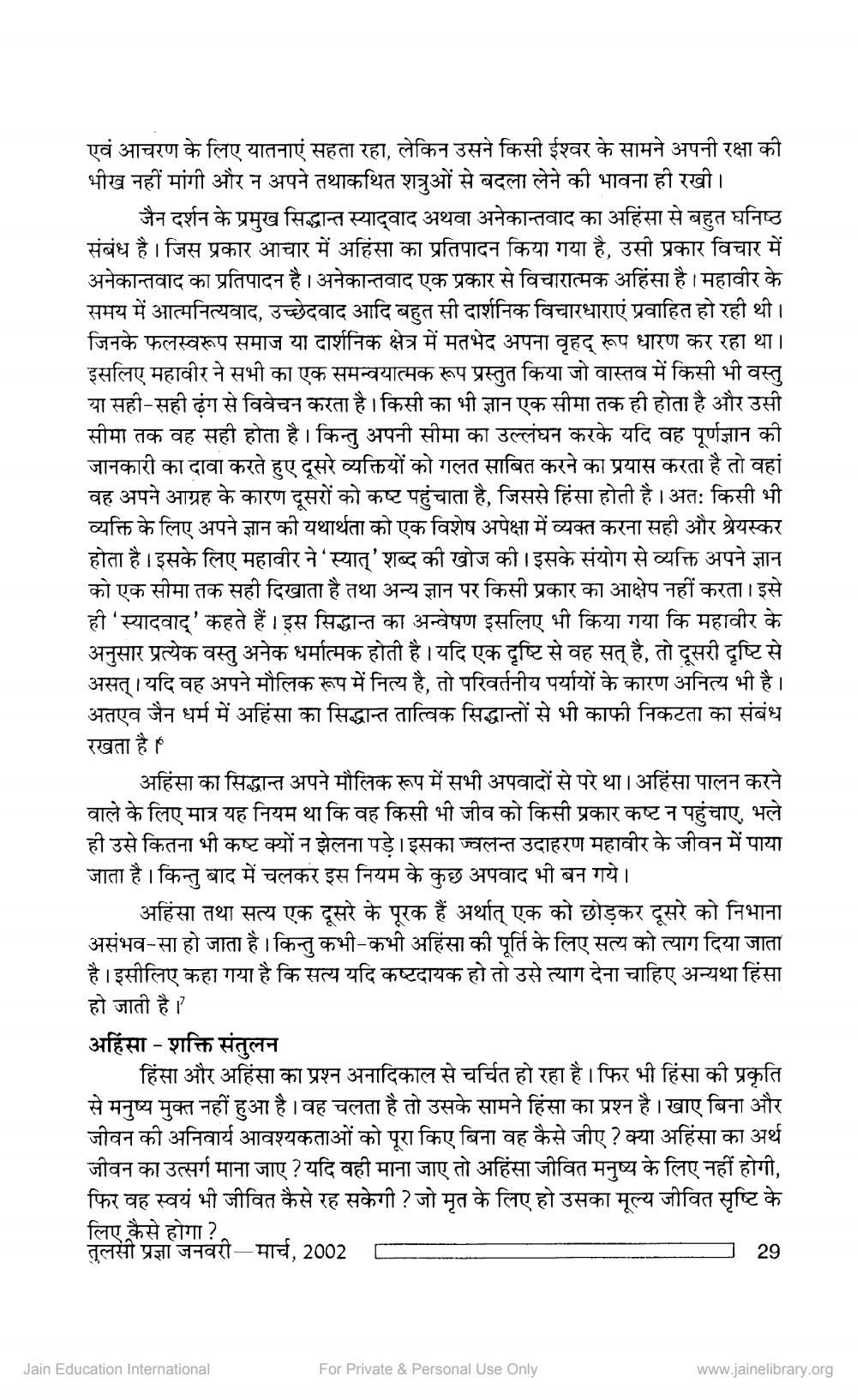________________
एवं आचरण के लिए यातनाएं सहता रहा, लेकिन उसने किसी ईश्वर के सामने अपनी रक्षा की भीख नहीं मांगी और न अपने तथाकथित शत्रुओं से बदला लेने की भावना ही रखी।
जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धान्त स्याद्वाद अथवा अनेकान्तवाद का अहिंसा से बहुत घनिष्ठ संबंध है। जिस प्रकार आचार में अहिंसा का प्रतिपादन किया गया है, उसी प्रकार विचार में अनेकान्तवाद का प्रतिपादन है। अनेकान्तवाद एक प्रकार से विचारात्मक अहिंसा है। महावीर के समय में आत्मनित्यवाद, उच्छेदवाद आदि बहुत सी दार्शनिक विचारधाराएं प्रवाहित हो रही थी । जिनके फलस्वरूप समाज या दार्शनिक क्षेत्र में मतभेद अपना वृहद् रूप धारण कर रहा था । इसलिए महावीर ने सभी का एक समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत किया जो वास्तव में किसी भी वस्तु या सही-सही ढंग से विवेचन करता है। किसी का भी ज्ञान एक सीमा तक ही होता है और उसी सीमा तक वह सही होता है। किन्तु अपनी सीमा का उल्लंघन करके यदि वह पूर्णज्ञान की जानकारी का दावा करते हुए दूसरे व्यक्तियों को गलत साबित करने का प्रयास करता है तो वहां वह अपने आग्रह के कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, जिससे हिंसा होती है। अतः किसी भी व्यक्ति के लिए अपने ज्ञान की यथार्थता को एक विशेष अपेक्षा में व्यक्त करना सही और श्रेयस्कर होता है। इसके लिए महावीर ने 'स्यात्' शब्द की खोज की। इसके संयोग से व्यक्ति अपने ज्ञान को एक सीमा तक सही दिखाता है तथा अन्य ज्ञान पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं करता। इसे ही ' स्यादवाद्' कहते हैं । इस सिद्धान्त का अन्वेषण इसलिए भी किया गया कि महावीर के अनुसार प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है। यदि एक दृष्टि से वह सत् है, तो दूसरी दृष्टि से असत् । यदि वह अपने मौलिक रूप में नित्य है, तो परिवर्तनीय पर्यायों के कारण अनित्य भी है। अतएव जैन धर्म में अहिंसा का सिद्धान्त तात्विक सिद्धान्तों से भी काफी निकटता का संबंध रखता है।
अहिंसा का सिद्धान्त अपने मौलिक रूप में सभी अपवादों से परे था । अहिंसा पालन करने वाले के लिए मात्र यह नियम था कि वह किसी भी जीव को किसी प्रकार कष्ट न पहुंचाए, भले ही उसे कितना भी कष्ट क्यों न झेलना पड़े। इसका ज्वलन्त उदाहरण महावीर के जीवन में पाया जाता है। किन्तु बाद में चलकर इस नियम के कुछ अपवाद भी बन गये ।
अहिंसा तथा सत्य एक दूसरे के पूरक हैं अर्थात् एक को छोड़कर दूसरे को निभाना असंभव-सा हो जाता है । किन्तु कभी-कभी अहिंसा की पूर्ति के लिए सत्य को त्याग दिया जाता है । इसीलिए कहा गया है कि सत्य यदि कष्टदायक हो तो उसे त्याग देना चाहिए अन्यथा हिंसा हो जाती है।
अहिंसा शक्ति संतुलन
हिंसा और अहिंसा का प्रश्न अनादिकाल से चर्चित हो रहा है। फिर भी हिंसा की प्रकृति से मनुष्य मुक्त नहीं हुआ है। वह चलता है तो उसके सामने हिंसा का प्रश्न है । खाए बिना और जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा किए बिना वह कैसे जीए ? क्या अहिंसा का अर्थ जीवन का उत्सर्ग माना जाए ? यदि वही माना जाए तो अहिंसा जीवित मनुष्य के लिए नहीं होगी, फिर वह स्वयं भी जीवित कैसे रह सकेगी ? जो मृत के लिए हो उसका मूल्य जीवित सृष्टि के लिए कैसे होगा ?. तुलसी प्रज्ञा जनवरी-मार्च, 2002
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
29
www.jainelibrary.org