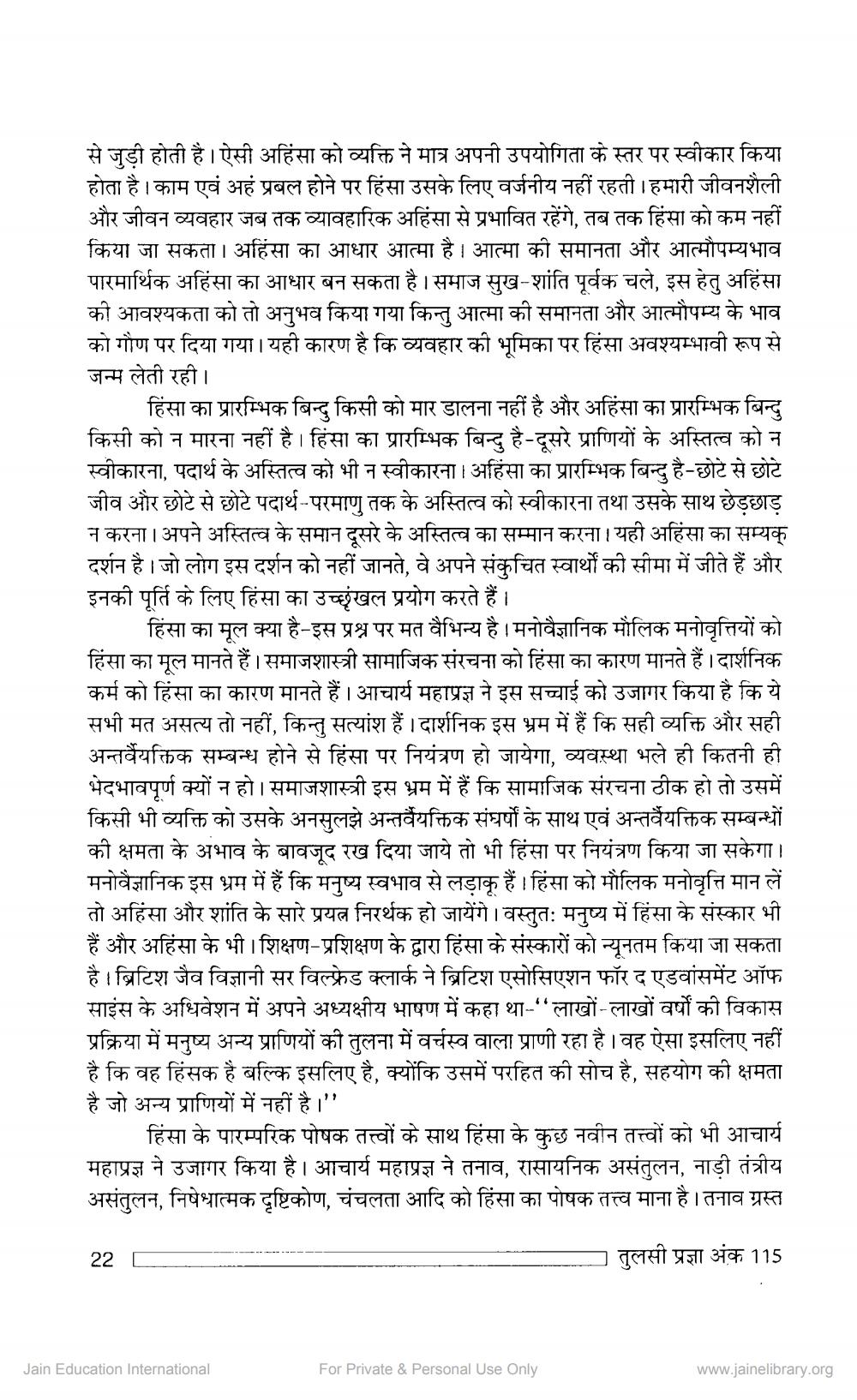________________
से जुड़ी होती है। ऐसी अहिंसा को व्यक्ति ने मात्र अपनी उपयोगिता के स्तर पर स्वीकार किया होता है। काम एवं अहं प्रबल होने पर हिंसा उसके लिए वर्जनीय नहीं रहती। हमारी जीवनशैली और जीवन व्यवहार जब तक व्यावहारिक अहिंसा से प्रभावित रहेंगे, तब तक हिंसा को कम नहीं किया जा सकता । अहिंसा का आधार आत्मा है। आत्मा की समानता और आत्मौपम्यभाव पारमार्थिक अहिंसा का आधार बन सकता है। समाज सुख-शांति पूर्वक चले, इस हेतु अहिंसा
आवश्यकता को तो अनुभव किया गया किन्तु आत्मा की समानता और आत्मौपम्य के भाव को गौण पर दिया गया। यही कारण है कि व्यवहार की भूमिका पर हिंसा अवश्यम्भावी रूप से जन्म लेती रही।
हिंसा का प्रारम्भिक बिन्दु किसी को मार डालना नहीं है और अहिंसा का प्रारम्भिक बिन्दु किसी को न मारना नहीं है। हिंसा का प्रारम्भिक बिन्दु है - दूसरे प्राणियों के अस्तित्व को न स्वीकारना, पदार्थ के अस्तित्व को भी न स्वीकारना । अहिंसा का प्रारम्भिक बिन्दु है-छोटे से छोटे जीव और छोटे से छोटे पदार्थ-परमाणु तक के अस्तित्व को स्वीकारना तथा उसके साथ छेड़छाड़ न करना । अपने अस्तित्व के समान दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करना । यही अहिंसा का सम्यक् दर्शन है । जो लोग इस दर्शन को नहीं जानते, वे अपने संकुचित स्वार्थों की सीमा में जीते हैं और इनकी पूर्ति के लिए हिंसा का उच्छृंखल प्रयोग करते हैं ।
हिंसा का मूल क्या है - इस प्रश्न पर मत वैभिन्य है। मनोवैज्ञानिक मौलिक मनोवृत्तियों को हिंसा का मूल मानते हैं। समाजशास्त्री सामाजिक संरचना को हिंसा का कारण मानते हैं। दार्शनिक कर्म को हिंसा का कारण मानते हैं । आचार्य महाप्रज्ञ ने इस सच्चाई को उजागर किया है कि ये सभी मत असत्य तो नहीं, किन्तु सत्यांश हैं। दार्शनिक इस भ्रम में हैं कि सही व्यक्ति और सही अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध होने से हिंसा पर नियंत्रण हो जायेगा, व्यवस्था भले ही कितनी ही भेदभावपूर्ण क्यों न हो । समाजशास्त्री इस भ्रम में हैं कि सामाजिक संरचना ठीक हो तो उसमें किसी भी व्यक्ति को उसके अनसुलझे अन्तर्वैयक्तिक संघर्षों के साथ एवं अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों की क्षमता के अभाव के बावजूद रख दिया जाये तो भी हिंसा पर नियंत्रण किया जा सकेगा। मनोवैज्ञानिक इस भ्रम में हैं कि मनुष्य स्वभाव से लड़ाकू हैं। हिंसा को मौलिक मनोवृत्ति मान लें तो अहिंसा और शांति के सारे प्रयत्न निरर्थक हो जायेंगे । वस्तुतः मनुष्य में हिंसा के संस्कार भी हैं और अहिंसा के भी। शिक्षण-प्रशिक्षण के द्वारा हिंसा के संस्कारों को न्यूनतम किया जा सकता है। ब्रिटिश जैव विज्ञानी सर विल्फ्रेड क्लार्क ने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था-" लाखों-लाखों वर्षों की विकास प्रक्रिया में मनुष्य अन्य प्राणियों की तुलना में वर्चस्व वाला प्राणी रहा है। वह ऐसा इसलिए नहीं है कि वह हिंसक है बल्कि इसलिए है, क्योंकि उसमें परहित की सोच है, सहयोग की क्षमता है जो अन्य प्राणियों में नहीं है।"
हिंसा के पारम्परिक पोषक तत्त्वों के साथ हिंसा के कुछ नवीन तत्त्वों को भी आचार्य महाप्रज्ञ ने उजागर किया है। आचार्य महाप्रज्ञ ने तनाव, रासायनिक असंतुलन, नाड़ी तंत्रीय असंतुलन, निषेधात्मक दृष्टिकोण, चंचलता आदि को हिंसा का पोषक तत्त्व माना है। तनाव ग्रस्त
तुलसी प्रज्ञा अंक 115
22
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org