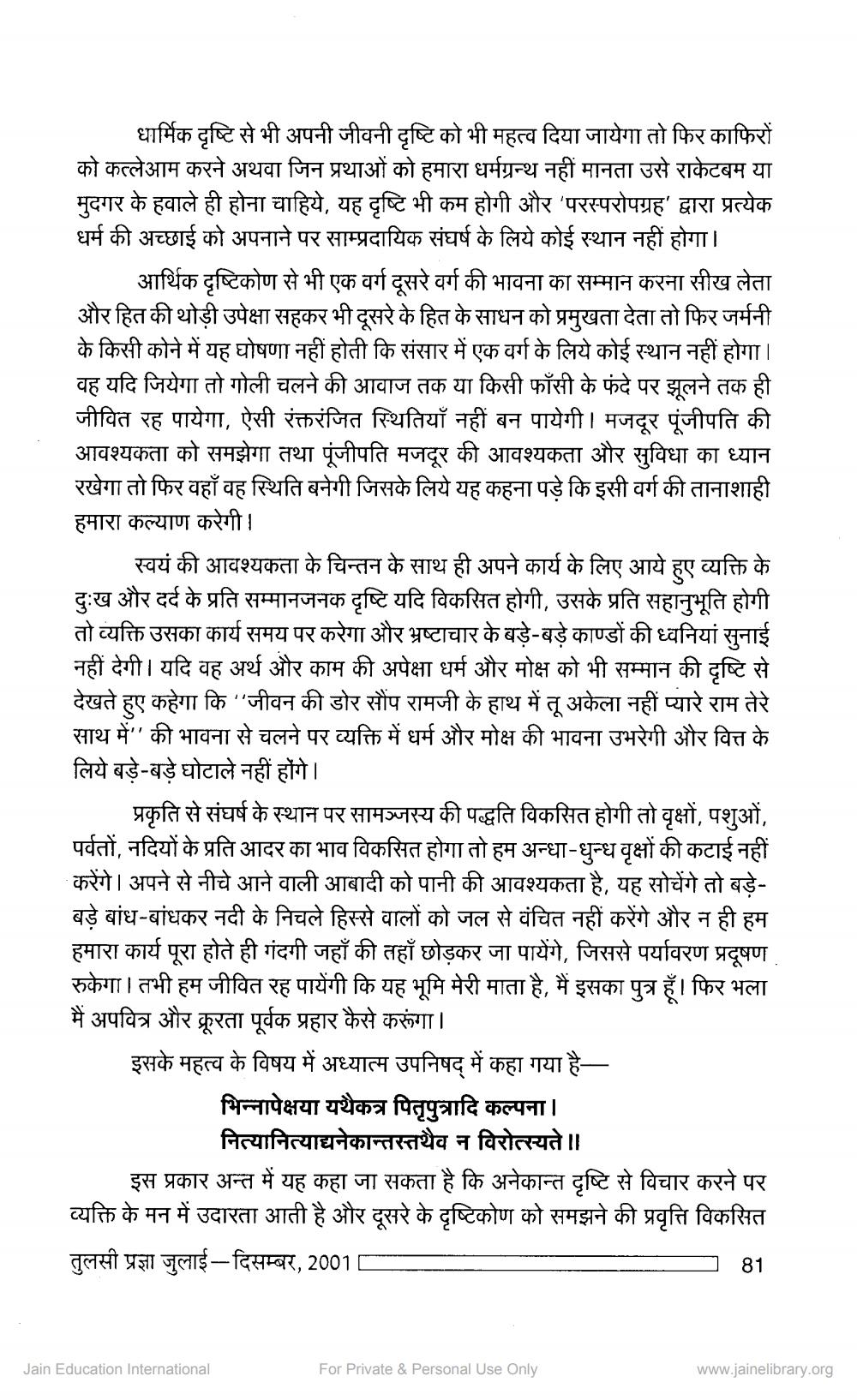________________
धार्मिक दृष्टि से भी अपनी जीवनी दृष्टि को भी महत्व दिया जायेगा तो फिर काफिरों को कत्लेआम करने अथवा जिन प्रथाओं को हमारा धर्मग्रन्थ नहीं मानता उसे राकेटबम या मुदगर के हवाले ही होना चाहिये, यह दृष्टि भी कम होगी और 'परस्परोपग्रह' द्वारा प्रत्येक धर्म की अच्छाई को अपनाने पर साम्प्रदायिक संघर्ष के लिये कोई स्थान नहीं होगा।
__ आर्थिक दृष्टिकोण से भी एक वर्ग दूसरे वर्ग की भावना का सम्मान करना सीख लेता और हित की थोड़ी उपेक्षा सहकर भी दूसरे के हित के साधन को प्रमुखता देता तो फिर जर्मनी के किसी कोने में यह घोषणा नहीं होती कि संसार में एक वर्ग के लिये कोई स्थान नहीं होगा। वह यदि जियेगा तो गोली चलने की आवाज तक या किसी फाँसी के फंदे पर झूलने तक ही जीवित रह पायेगा, ऐसी रक्तरंजित स्थितियाँ नहीं बन पायेगी। मजदूर पूंजीपति की आवश्यकता को समझेगा तथा पूंजीपति मजदूर की आवश्यकता और सुविधा का ध्यान रखेगा तो फिर वहाँ वह स्थिति बनेगी जिसके लिये यह कहना पड़े कि इसी वर्ग की तानाशाही हमारा कल्याण करेगी।
स्वयं की आवश्यकता के चिन्तन के साथ ही अपने कार्य के लिए आये हुए व्यक्ति के दुःख और दर्द के प्रति सम्मानजनक दृष्टि यदि विकसित होगी, उसके प्रति सहानुभूति होगी तो व्यक्ति उसका कार्य समय पर करेगा और भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े काण्डों की ध्वनियां सुनाई नहीं देगी। यदि वह अर्थ और काम की अपेक्षा धर्म और मोक्ष को भी सम्मान की दृष्टि से देखते हुए कहेगा कि ''जीवन की डोर सौंप रामजी के हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में'' की भावना से चलने पर व्यक्ति में धर्म और मोक्ष की भावना उभरेगी और वित्त के लिये बड़े-बड़े घोटाले नहीं होंगे।
__ प्रकृति से संघर्ष के स्थान पर सामञ्जस्य की पद्धति विकसित होगी तो वृक्षों, पशुओं, पर्वतों, नदियों के प्रति आदर का भाव विकसित होगा तो हम अन्धा-धुन्ध वृक्षों की कटाई नहीं करेंगे। अपने से नीचे आने वाली आबादी को पानी की आवश्यकता है, यह सोचेंगे तो बड़ेबड़े बांध-बांधकर नदी के निचले हिस्से वालों को जल से वंचित नहीं करेंगे और न ही हम हमारा कार्य पूरा होते ही गंदगी जहाँ की तहाँ छोड़कर जा पायेंगे, जिससे पर्यावरण प्रदूषण रुकेगा। तभी हम जीवित रह पायेंगी कि यह भूमि मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूँ। फिर भला मैं अपवित्र और क्रूरता पूर्वक प्रहार कैसे करूंगा। इसके महत्व के विषय में अध्यात्म उपनिषद् में कहा गया है
भिन्नापेक्षया यथैकत्र पितृपुत्रादि कल्पना।
नित्यानित्याद्यनेकान्तस्तथैव न विरोत्स्यते॥ इस प्रकार अन्त में यह कहा जा सकता है कि अनेकान्त दृष्टि से विचार करने पर व्यक्ति के मन में उदारता आती है और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की प्रवृत्ति विकसित तुलसी प्रज्ञा जुलाई-दिसम्बर, 20016
81
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org