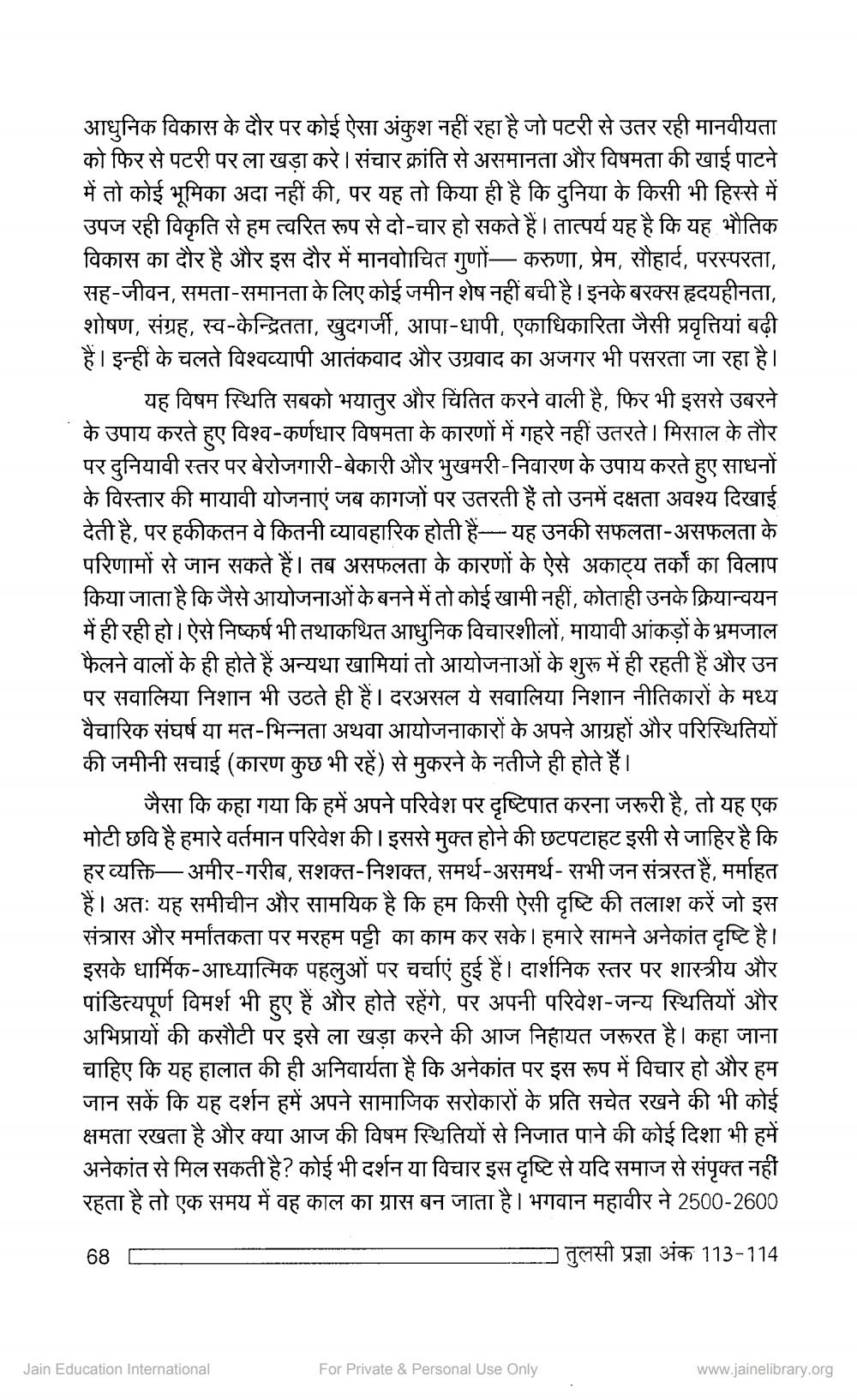________________
आधुनिक विकास के दौर पर कोई ऐसा अंकुश नहीं रहा है जो पटरी से उतर रही मानवीयता को फिर से पटरी पर ला खड़ा करे । संचार क्रांति से असमानता और विषमता की खाई पाटने में तो कोई भूमिका अदा नहीं की, पर यह तो किया ही है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में उपज रही विकृति से हम त्वरित रूप से दो-चार हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि यह भौतिक विकास का दौर है और इस दौर में मानवोचित गुणों- करुणा, प्रेम, सौहार्द, परस्परता, सह-जीवन, समता-समानता के लिए कोई जमीन शेष नहीं बची है। इनके बरक्स हृदयहीनता, शोषण, संग्रह, स्व-केन्द्रितता, खुदगर्जी, आपा-धापी, एकाधिकारिता जैसी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं। इन्हीं के चलते विश्वव्यापी आतंकवाद और उग्रवाद का अजगर भी पसरता जा रहा है।
यह विषम स्थिति सबको भयातुर और चिंतित करने वाली है, फिर भी इससे उबरने के उपाय करते हुए विश्व-कर्णधार विषमता के कारणों में गहरे नहीं उतरते । मिसाल के तौर पर दुनियावी स्तर पर बेरोजगारी-बेकारी और भुखमरी-निवारण के उपाय करते हुए साधनों के विस्तार की मायावी योजनाएं जब कागजों पर उतरती हैं तो उनमें दक्षता अवश्य दिखाई देती है, पर हकीकतन वे कितनी व्यावहारिक होती हैंयह उनकी सफलता-असफलता के परिणामों से जान सकते हैं। तब असफलता के कारणों के ऐसे अकाट्य तर्कों का विलाप किया जाता है कि जैसे आयोजनाओं के बनने में तो कोई खामी नहीं, कोताही उनके क्रियान्वयन में ही रही हो। ऐसे निष्कर्ष भी तथाकथित आधुनिक विचारशीलों, मायावी आंकड़ों के भ्रमजाल फैलने वालों के ही होते हैं अन्यथा खामियां तो आयोजनाओं के शुरू में ही रहती हैं और उन पर सवालिया निशान भी उठते ही हैं। दरअसल ये सवालिया निशान नीतिकारों के मध्य वैचारिक संघर्ष या मत-भिन्नता अथवा आयोजनाकारों के अपने आग्रहों और परिस्थितियों की जमीनी सचाई (कारण कुछ भी रहें) से मुकरने के नतीजे ही होते हैं।
जैसा कि कहा गया कि हमें अपने परिवेश पर दृष्टिपात करना जरूरी है, तो यह एक मोटी छवि है हमारे वर्तमान परिवेश की । इससे मुक्त होने की छटपटाहट इसी से जाहिर है कि हर व्यक्ति- अमीर-गरीब, सशक्त-निशक्त, समर्थ-असमर्थ- सभी जन संत्रस्त हैं, मर्माहत हैं। अतः यह समीचीन और सामयिक है कि हम किसी ऐसी दृष्टि की तलाश करें जो इस संत्रास और मर्मांतकता पर मरहम पट्टी का काम कर सके। हमारे सामने अनेकांत दृष्टि है। इसके धार्मिक-आध्यात्मिक पहलुओं पर चर्चाएं हई हैं। दार्शनिक स्तर पर शास्त्रीय और पांडित्यपूर्ण विमर्श भी हुए हैं और होते रहेंगे, पर अपनी परिवेश-जन्य स्थितियों और अभिप्रायों की कसौटी पर इसे ला खड़ा करने की आज निहायत जरूरत है। कहा जाना चाहिए कि यह हालात की ही अनिवार्यता है कि अनेकांत पर इस रूप में विचार हो और हम जान सकें कि यह दर्शन हमें अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति सचेत रखने की भी कोई क्षमता रखता है और क्या आज की विषम स्थितियों से निजात पाने की कोई दिशा भी हमें अनेकांत से मिल सकती है? कोई भी दर्शन या विचार इस दृष्टि से यदि समाज से संपृक्त नहीं रहता है तो एक समय में वह काल का ग्रास बन जाता है। भगवान महावीर ने 2500-2600 68 -
- तुलसी प्रज्ञा अंक 113-114
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org