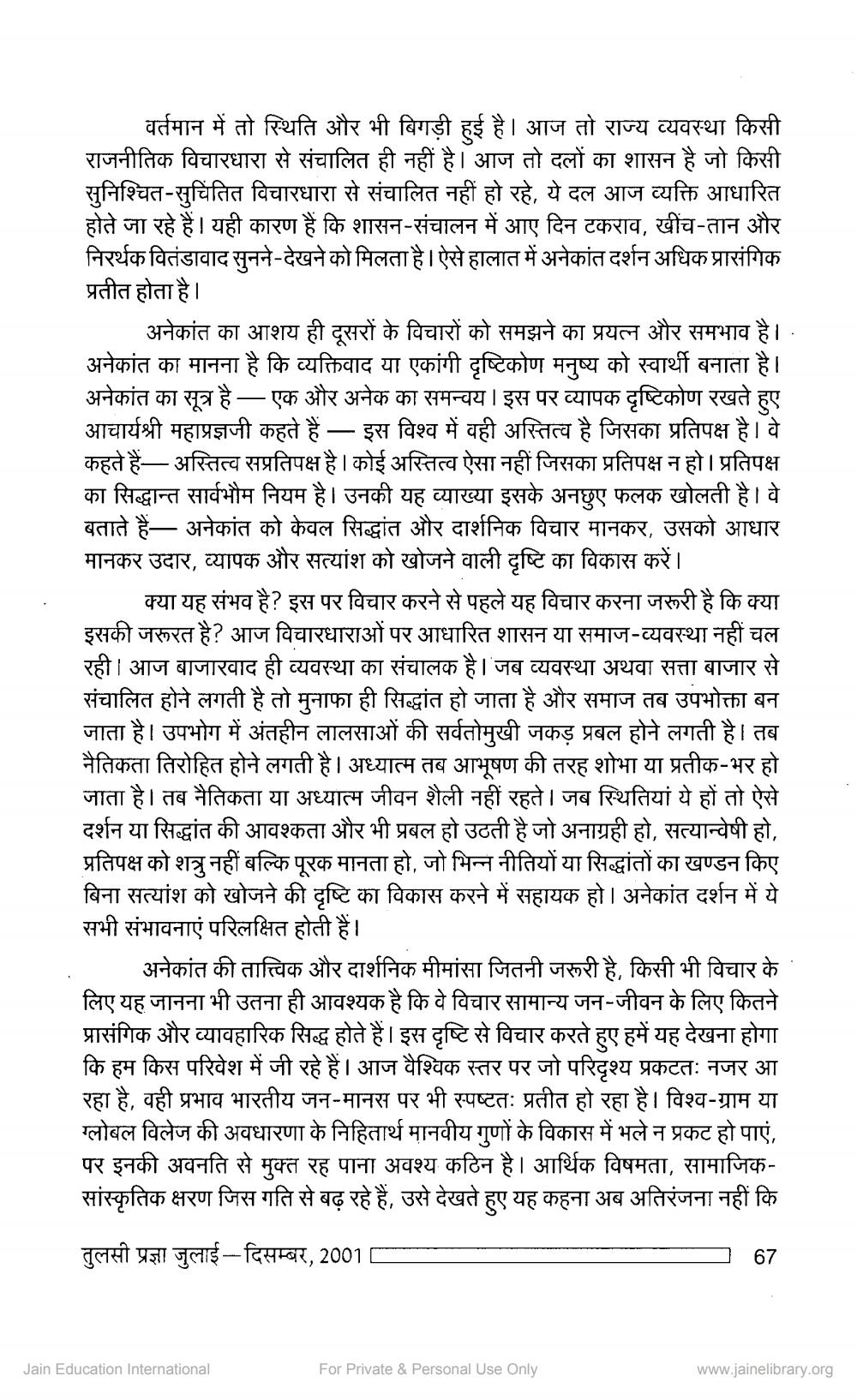________________
वर्तमान में तो स्थिति और भी बिगड़ी हई है। आज तो राज्य व्यवस्था किसी राजनीतिक विचारधारा से संचालित ही नहीं है। आज तो दलों का शासन है जो किसी सुनिश्चित-सुचिंतित विचारधारा से संचालित नहीं हो रहे, ये दल आज व्यक्ति आधारित होते जा रहे हैं। यही कारण है कि शासन-संचालन में आए दिन टकराव, खींच-तान और निरर्थक वितंडावाद सुनने-देखने को मिलता है। ऐसे हालात में अनेकांत दर्शन अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है।
__ अनेकांत का आशय ही दूसरों के विचारों को समझने का प्रयत्न और समभाव है। . अनेकांत का मानना है कि व्यक्तिवाद या एकांगी दृष्टिकोण मनुष्य को स्वार्थी बनाता है। अनेकांत का सूत्र है - एक और अनेक का समन्वय । इस पर व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए आचार्यश्री महाप्रज्ञजी कहते हैं – इस विश्व में वही अस्तित्व है जिसका प्रतिपक्ष है। वे कहते हैं— अस्तित्व सप्रतिपक्ष है। कोई अस्तित्व ऐसा नहीं जिसका प्रतिपक्ष न हो । प्रतिपक्ष का सिद्धान्त सार्वभौम नियम है। उनकी यह व्याख्या इसके अनछुए फलक खोलती है। वे बताते हैं— अनेकांत को केवल सिद्धांत और दार्शनिक विचार मानकर, उसको आधार मानकर उदार, व्यापक और सत्यांश को खोजने वाली दृष्टि का विकास करें।
___क्या यह संभव है? इस पर विचार करने से पहले यह विचार करना जरूरी है कि क्या इसकी जरूरत है? आज विचारधाराओं पर आधारित शासन या समाज-व्यवस्था नहीं चल रही। आज बाजारवाद ही व्यवस्था का संचालक है। जब व्यवस्था अथवा सत्ता बाजार से संचालित होने लगती है तो मुनाफा ही सिद्धांत हो जाता है और समाज तब उपभोक्ता बन जाता है। उपभोग में अंतहीन लालसाओं की सर्वतोमुखी जकड़ प्रबल होने लगती है। तब नैतिकता तिरोहित होने लगती है। अध्यात्म तब आभूषण की तरह शोभा या प्रतीक-भर हो जाता है। तब नैतिकता या अध्यात्म जीवन शैली नहीं रहते । जब स्थितियां ये हों तो ऐसे दर्शन या सिद्धांत की आवश्कता और भी प्रबल हो उठती है जो अनाग्रही हो, सत्यान्वेषी हो, प्रतिपक्ष को शत्रु नहीं बल्कि पूरक मानता हो, जो भिन्न नीतियों या सिद्धांतों का खण्डन किए बिना सत्यांश को खोजने की दृष्टि का विकास करने में सहायक हो। अनेकांत दर्शन में ये सभी संभावनाएं परिलक्षित होती हैं।
अनेकांत की तात्त्विक और दार्शनिक मीमांसा जितनी जरूरी है, किसी भी विचार के लिए यह जानना भी उतना ही आवश्यक है कि वे विचार सामान्य जन-जीवन के लिए कितने प्रासंगिक और व्यावहारिक सिद्ध होते हैं। इस दृष्टि से विचार करते हुए हमें यह देखना होगा कि हम किस परिवेश में जी रहे हैं। आज वैश्विक स्तर पर जो परिदृश्य प्रकटतः नजर आ रहा है, वही प्रभाव भारतीय जन-मानस पर भी स्पष्टतः प्रतीत हो रहा है। विश्व-ग्राम या ग्लोबल विलेज की अवधारणा के निहितार्थ मानवीय गुणों के विकास में भले न प्रकट हो पाएं, पर इनकी अवनति से मुक्त रह पाना अवश्य कठिन है। आर्थिक विषमता, सामाजिकसांस्कृतिक क्षरण जिस गति से बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए यह कहना अब अतिरंजना नहीं कि
तुलसी प्रज्ञा जुलाई-दिसम्बर, 20016
-
67
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org