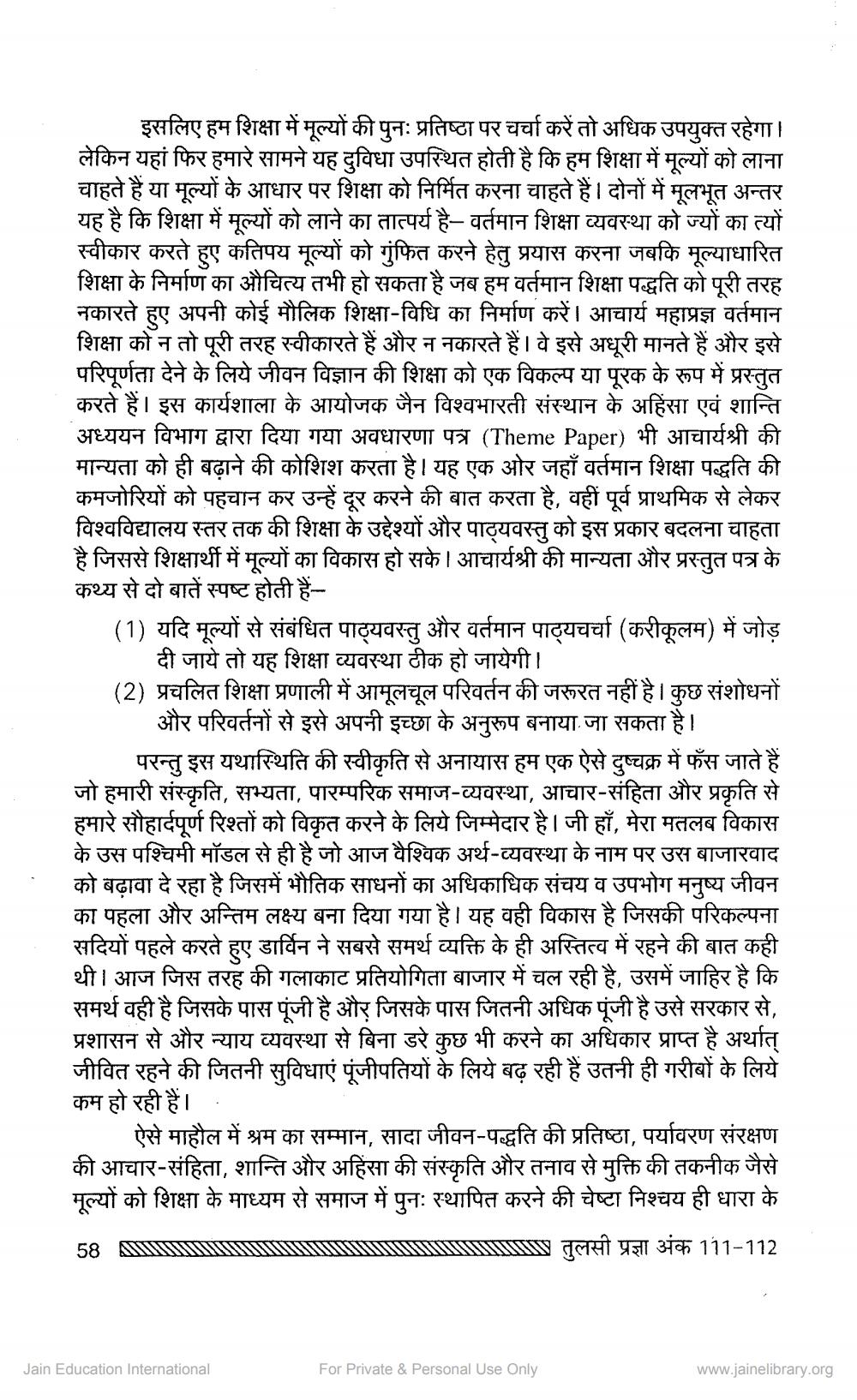________________
इसलिए हम शिक्षा में मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा पर चर्चा करें तो अधिक उपयुक्त रहेगा। लेकिन यहां फिर हमारे सामने यह दुविधा उपस्थित होती है कि हम शिक्षा में मूल्यों को लाना चाहते हैं या मूल्यों के आधार पर शिक्षा को निर्मित करना चाहते हैं। दोनों में मूलभूत अन्तर यह है कि शिक्षा में मूल्यों को लाने का तात्पर्य है- वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्वीकार करते हुए कतिपय मूल्यों को गुंफित करने हेतु प्रयास करना जबकि मूल्याधारित शिक्षा के निर्माण का औचित्य तभी हो सकता है जब हम वर्तमान शिक्षा पद्धति को पूरी तरह नकारते हुए अपनी कोई मौलिक शिक्षा-विधि का निर्माण करें। आचार्य महाप्रज्ञ वर्तमान शिक्षा को न तो पूरी तरह स्वीकारते हैं और न नकारते हैं। वे इसे अधूरी मानते हैं और इसे परिपूर्णता देने के लिये जीवन विज्ञान की शिक्षा को एक विकल्प या पूरक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस कार्यशाला के आयोजक जैन विश्वभारती संस्थान के अहिंसा एवं शान्ति अध्ययन विभाग द्वारा दिया गया अवधारणा पत्र (Theme Paper) भी आचार्यश्री की मान्यता को ही बढ़ाने की कोशिश करता है। यह एक ओर जहाँ वर्तमान शिक्षा पद्धति की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने की बात करता है, वहीं पूर्व प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के उद्देश्यों और पाठ्यवस्तु को इस प्रकार बदलना चाहता है जिससे शिक्षार्थी में मूल्यों का विकास हो सके । आचार्यश्री की मान्यता और प्रस्तुत पत्र के कथ्य से दो बातें स्पष्ट होती है(1) यदि मूल्यों से संबंधित पाठ्यवस्तु और वर्तमान पाठ्यचर्चा (करीकूलम) में जोड़
दी जाये तो यह शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जायेगी। (2) प्रचलित शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत नहीं है। कुछ संशोधनों
और परिवर्तनों से इसे अपनी इच्छा के अनुरूप बनाया जा सकता है। परन्तु इस यथास्थिति की स्वीकृति से अनायास हम एक ऐसे दुष्चक्र में फँस जाते हैं जो हमारी संस्कृति, सभ्यता, पारम्परिक समाज-व्यवस्था, आचार-संहिता और प्रकृति से हमारे सौहार्दपूर्ण रिश्तों को विकृत करने के लिये जिम्मेदार है। जी हाँ, मेरा मतलब विकास के उस पश्चिमी मॉडल से ही है जो आज वैश्विक अर्थ-व्यवस्था के नाम पर उस बाजारवाद को बढ़ावा दे रहा है जिसमें भौतिक साधनों का अधिकाधिक संचय व उपभोग मनुष्य जीवन का पहला और अन्तिम लक्ष्य बना दिया गया है। यह वही विकास है जिसकी परिकल्पना सदियों पहले करते हुए डार्विन ने सबसे समर्थ व्यक्ति के ही अस्तित्व में रहने की बात कही थी। आज जिस तरह की गलाकाट प्रतियोगिता बाजार में चल रही है, उसमें जाहिर है कि समर्थ वही है जिसके पास पूंजी है और जिसके पास जितनी अधिक पूंजी है उसे सरकार से, प्रशासन से और न्याय व्यवस्था से बिना डरे कुछ भी करने का अधिकार प्राप्त है अर्थात् जीवित रहने की जितनी सुविधाएं पूंजीपतियों के लिये बढ़ रही हैं उतनी ही गरीबों के लिये कम हो रही है।
ऐसे माहौल में श्रम का सम्मान, सादा जीवन-पद्धति की प्रतिष्ठा, पर्यावरण संरक्षण की आचार-संहिता, शान्ति और अहिंसा की संस्कृति और तनाव से मुक्ति की तकनीक जैसे मूल्यों को शिक्षा के माध्यम से समाज में पुनः स्थापित करने की चेष्टा निश्चय ही धारा के 58 AIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII तल
IIIII तुलसी प्रज्ञा अंक 111-112
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org