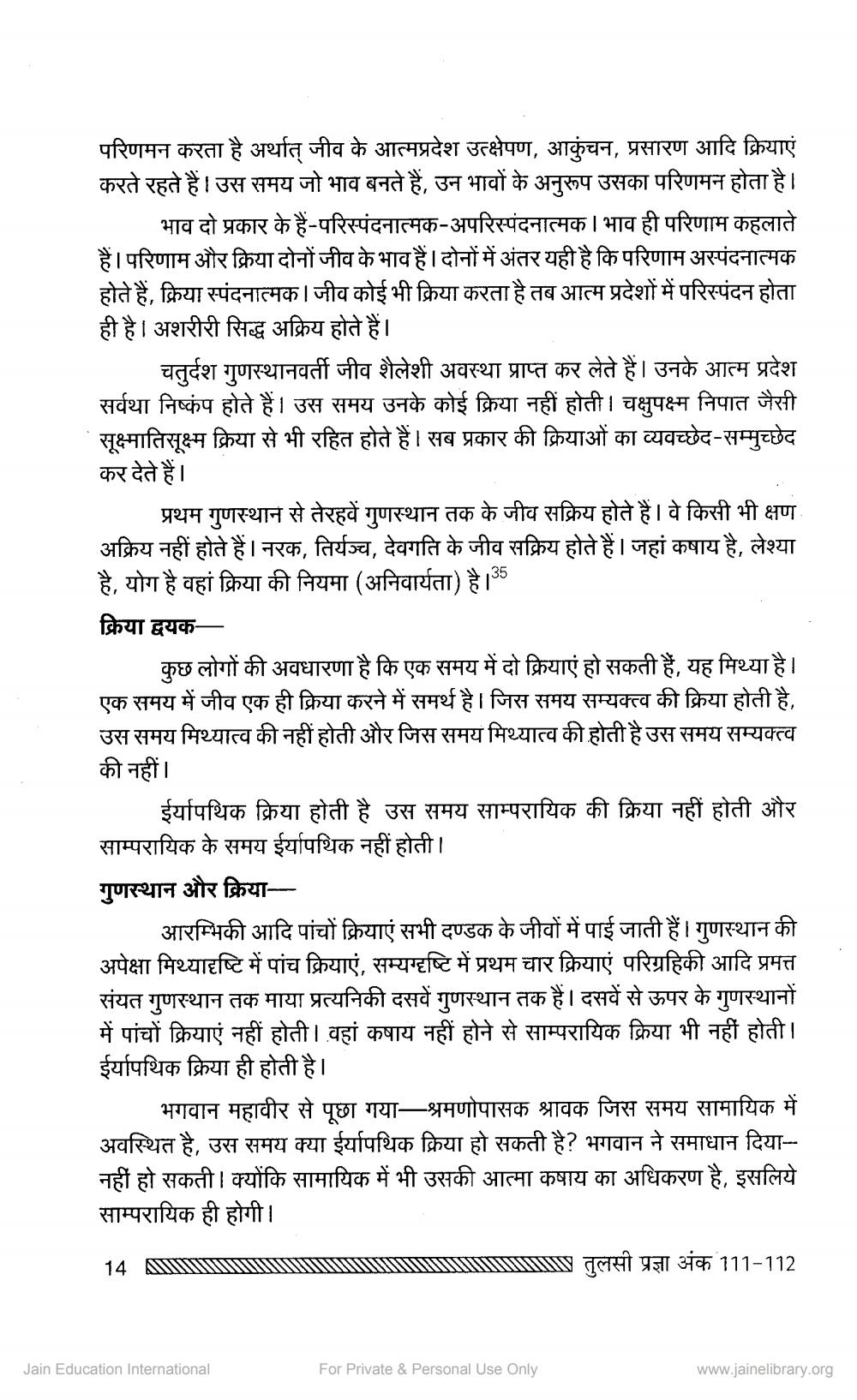________________
परिणमन करता है अर्थात् जीव के आत्मप्रदेश उत्क्षेपण, आकुंचन, प्रसारण आदि क्रियाएं करते रहते हैं । उस समय जो भाव बनते हैं, उन भावों के अनुरूप उसका परिणमन होता है।
भाव दो प्रकार के हैं- परिस्पंदनात्मक - अपरिस्पंदनात्मक । भाव ही परिणाम कहलाते हैं। परिणाम और क्रिया दोनों जीव के भाव हैं। दोनों में अंतर यही है कि परिणाम अस्पंदनात्मक होते हैं, क्रिया स्पंदनात्मक । जीव कोई भी क्रिया करता है तब आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता ही है। अशरीरी सिद्ध अक्रिय होते हैं।
चतुर्दश गुणस्थानवर्ती जीव शैलेशी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। उनके आत्म प्रदेश सर्वथा निष्कंप होते हैं। उस समय उनके कोई क्रिया नहीं होती । चक्षुपक्ष्म निपात जैसी सूक्ष्मातिसूक्ष्म क्रिया से भी रहित होते हैं । सब प्रकार की क्रियाओं का व्यवच्छेद- सम्मुच्छेद कर देते हैं ।
प्रथम गुणस्थान से तेरहवें गुणस्थान तक के जीव सक्रिय होते हैं । वे किसी भी क्षण अक्रिय नहीं होते हैं। नरक, तिर्यञ्च देवगति के जीव सक्रिय होते हैं। जहां कषाय है, लेश्या है, योग है वहां क्रिया की नियमा (अनिवार्यता ) है | 35
क्रिया द्वयक
कुछ लोगों की अवधारणा है कि एक समय में दो क्रियाएं हो सकती हैं, यह मिथ्या है। एक समय में जीव एक ही क्रिया करने में समर्थ है। जिस समय सम्यक्त्व की क्रिया होती है, उस समय मिथ्यात्व की नहीं होती और जिस समय मिथ्यात्व की होती है उस समय सम्यक्त्व की नहीं ।
ईर्यापथिक क्रिया होती है उस समय साम्परायिक की क्रिया नहीं होती और साम्परायिक के समय ईर्यापथिक नहीं होती।
गुणस्थान और क्रिया
आरम्भिकी आदि पांचों क्रियाएं सभी दण्डक के जीवों में पाई जाती हैं। गुणस्थान की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि में पांच क्रियाएं, सम्यग्दृष्टि में प्रथम चार क्रियाएं परिग्रहिकी आदि प्रमत्त संयत गुणस्थान तक माया प्रत्यनिकी दसवें गुणस्थान तक हैं। दसवें से ऊपर के गुणस्थानों में पांचों क्रियाएं नहीं होती। वहां कषाय नहीं होने से साम्परायिक क्रिया भी नहीं होती । ईर्यापथिक क्रिया ही होती है ।
भगवान महावीर से पूछा गया - श्रमणोपासक श्रावक जिस समय सामायिक में अवस्थित है, उस समय क्या ईर्यापथिक क्रिया हो सकती है ? भगवान ने समाधान दियानहीं हो सकती। क्योंकि सामायिक में भी उसकी आत्मा कषाय का अधिकरण है, इसलिये साम्परायिक ही होगी।
14
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
WWW तुलसी प्रज्ञा अंक 111-112
www.jainelibrary.org