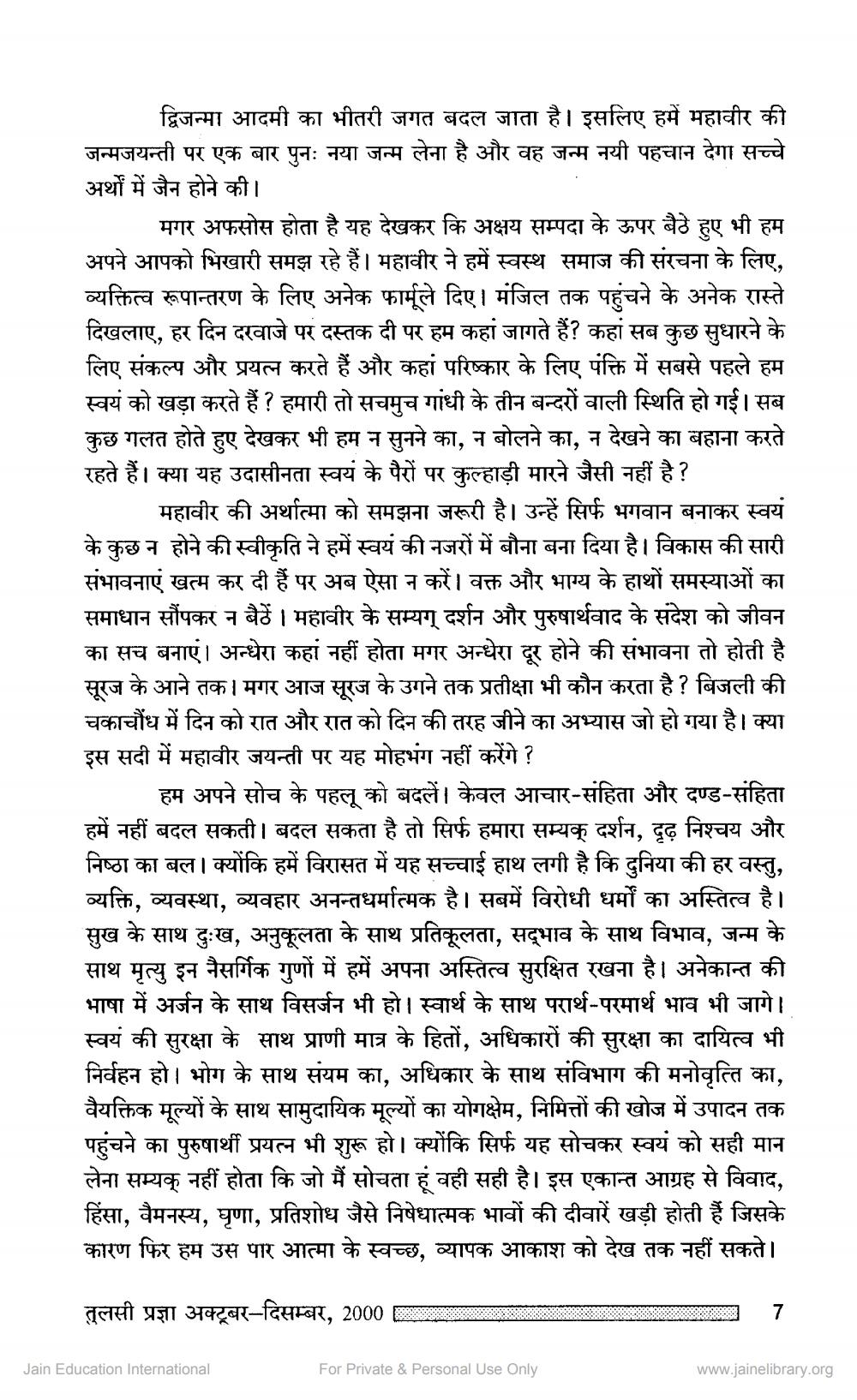________________
द्विजन्मा आदमी का भीतरी जगत बदल जाता है। इसलिए हमें महावीर की जन्मजयन्ती पर एक बार पुनः नया जन्म लेना है और वह जन्म नयी पहचान देगा सच्चे अर्थों में जैन होने की।
मगर अफसोस होता है यह देखकर कि अक्षय सम्पदा के ऊपर बैठे हुए भी हम अपने आपको भिखारी समझ रहे हैं। महावीर ने हमें स्वस्थ समाज की संरचना के लिए, व्यक्तित्व रूपान्तरण के लिए अनेक फार्मूले दिए। मंजिल तक पहुंचने के अनेक रास्ते दिखलाए, हर दिन दरवाजे पर दस्तक दी पर हम कहां जागते हैं? कहां सब कुछ सुधारने के लिए संकल्प और प्रयत्न करते हैं और कहां परिष्कार के लिए पंक्ति में सबसे पहले हम स्वयं को खड़ा करते हैं ? हमारी तो सचमुच गांधी के तीन बन्दरों वाली स्थिति हो गई। सब कुछ गलत होते हुए देखकर भी हम न सुनने का, न बोलने का, न देखने का बहाना करते रहते हैं। क्या यह उदासीनता स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी नहीं है?
महावीर की अर्थात्मा को समझना जरूरी है। उन्हें सिर्फ भगवान बनाकर स्वयं के कुछ न होने की स्वीकृति ने हमें स्वयं की नजरों में बौना बना दिया है। विकास की सारी संभावनाएं खत्म कर दी हैं पर अब ऐसा न करें। वक्त और भाग्य के हाथों समस्याओं का समाधान सौंपकर न बैठें । महावीर के सम्यग् दर्शन और पुरुषार्थवाद के संदेश को जीवन का सच बनाएं। अन्धेरा कहां नहीं होता मगर अन्धेरा दूर होने की संभावना तो होती है सूरज के आने तक । मगर आज सूरज के उगने तक प्रतीक्षा भी कौन करता है ? बिजली की चकाचौंध में दिन को रात और रात को दिन की तरह जीने का अभ्यास जो हो गया है। क्या इस सदी में महावीर जयन्ती पर यह मोहभंग नहीं करेंगे?
हम अपने सोच के पहलू को बदलें। केवल आचार-संहिता और दण्ड-संहिता हमें नहीं बदल सकती। बदल सकता है तो सिर्फ हमारा सम्यक् दर्शन, दृढ़ निश्चय और निष्ठा का बल। क्योंकि हमें विरासत में यह सच्चाई हाथ लगी है कि दुनिया की हर वस्तु, व्यक्ति, व्यवस्था, व्यवहार अनन्तधर्मात्मक है। सबमें विरोधी धर्मों का अस्तित्व है। सुख के साथ दुःख, अनुकूलता के साथ प्रतिकूलता, सद्भाव के साथ विभाव, जन्म के साथ मृत्यु इन नैसर्गिक गुणों में हमें अपना अस्तित्व सुरक्षित रखना है। अनेकान्त की भाषा में अर्जन के साथ विसर्जन भी हो । स्वार्थ के साथ परार्थ-परमार्थ भाव भी जागे। स्वयं की सुरक्षा के साथ प्राणी मात्र के हितों, अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व भी निर्वहन हो। भोग के साथ संयम का, अधिकार के साथ संविभाग की मनोवृत्ति का, वैयक्तिक मूल्यों के साथ सामुदायिक मूल्यों का योगक्षेम, निमित्तों की खोज में उपादन तक पहुंचने का पुरुषार्थी प्रयत्न भी शुरू हो। क्योंकि सिर्फ यह सोचकर स्वयं को सही मान लेना सम्यक नहीं होता कि जो मैं सोचता हूं वही सही है। इस एकान्त आग्रह से विवाद, हिंसा, वैमनस्य, घृणा, प्रतिशोध जैसे निषेधात्मक भावों की दीवारें खड़ी होती हैं जिसके कारण फिर हम उस पार आत्मा के स्वच्छ, व्यापक आकाश को देख तक नहीं सकते।
तुलसी प्रज्ञा अक्टूबर-दिसम्बर, 2000
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org