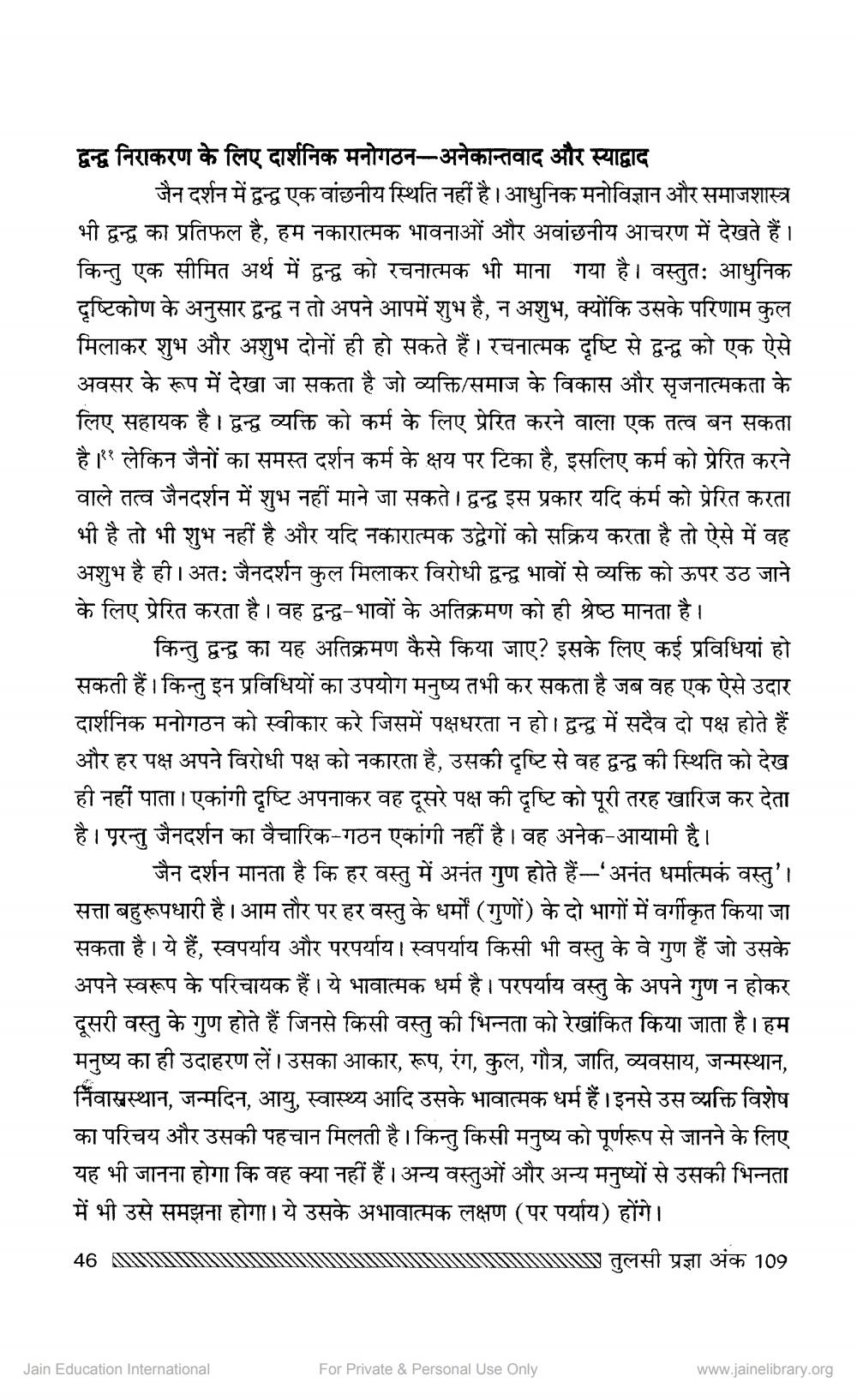________________
द्वन्द्व निराकरण के लिए दार्शनिक मनोगठन - अनेकान्तवाद और स्याद्वाद
जैन दर्शन में द्वन्द्व एक वांछनीय स्थिति नहीं है । आधुनिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र भी द्वन्द्व का प्रतिफल है, हम नकारात्मक भावनाओं और अवांछनीय आचरण में देखते हैं । किन्तु एक सीमित अर्थ में द्वन्द्व को रचनात्मक भी माना गया है। वस्तुतः आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार द्वन्द्व न तो अपने आपमें शुभ है, न अशुभ, क्योंकि उसके परिणाम कुल मिलाकर शुभ और अशुभ दोनों ही हो सकते हैं । रचनात्मक दृष्टि से द्वन्द्व को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जा सकता है जो व्यक्ति / समाज के विकास और सृजनात्मकता के लिए सहायक है । द्वन्द्व व्यक्ति को कर्म के लिए प्रेरित करने वाला एक तत्व बन सकता है । लेकिन जैनों का समस्त दर्शन कर्म के क्षय पर टिका है, इसलिए कर्म को प्रेरित करने वाले तत्व जैनदर्शन में शुभ नहीं माने जा सकते। द्वन्द्व इस प्रकार यदि कर्म को प्रेरित करता भी है तो भी शुभ नहीं है और यदि नकारात्मक उद्वेगों को सक्रिय करता है तो ऐसे में वह अशुभ है ही । अत: जैनदर्शन कुल मिलाकर विरोधी द्वन्द्व भावों से व्यक्ति को ऊपर उठ जाने लिए प्रेरित करता है । वह द्वन्द्व - भावों के अतिक्रमण को ही श्रेष्ठ मानता है ।
किन्तु द्वन्द्व का यह अतिक्रमण कैसे किया जाए? इसके लिए कई प्रविधियां हो सकती हैं। किन्तु इन प्रविधियों का उपयोग मनुष्य तभी कर सकता है जब वह एक ऐसे उदार दार्शनिक मनोगठन को स्वीकार करे जिसमें पक्षधरता न हो । द्वन्द्व में सदैव दो पक्ष होते हैं और हर पक्ष अपने विरोधी पक्ष को नकारता है, उसकी दृष्टि से वह द्वन्द्व की स्थिति को देख ही नहीं पाता । एकांगी दृष्टि अपनाकर वह दूसरे पक्ष की दृष्टि को पूरी तरह खारिज कर देता
है । परन्तु जैनदर्शन का वैचारिक- गठन एकांगी नहीं है । वह अनेक आयामी है ।
1
जैन दर्शन मानता है कि हर वस्तु में अनंत गुण होते हैं - 'अनंत धर्मात्मकं वस्तु' । सत्ता बहुरूपधारी है। आम तौर पर हर वस्तु के धर्मों (गुणों) के दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये हैं, स्वपर्याय और परपर्याय । स्वपर्याय किसी भी वस्तु के वे गुण हैं जो उसके अपने स्वरूप के परिचायक हैं । ये भावात्मक धर्म है । परपर्याय वस्तु के अपने गुण न होकर दूसरी वस्तु के गुण होते हैं जिनसे किसी वस्तु की भिन्नता को रेखांकित किया जाता है। ह मनुष्य का ही उदाहरण लें। उसका आकार, रूप, रंग, कुल, गौत्र, जाति, व्यवसाय, जन्मस्थान, निवास्वस्थान, जन्मदिन, आयु, स्वास्थ्य आदि उसके भावात्मक धर्म हैं। इनसे उस व्यक्ति विशेष का परिचय और उसकी पहचान मिलती है। किन्तु किसी मनुष्य को पूर्णरूप से जानने के लिए यह भी जानना होगा कि वह क्या नहीं हैं । अन्य वस्तुओं और अन्य मनुष्यों से उसकी भिन्नता में भी उसे समझना होगा। ये उसके अभावात्मक लक्षण (पर पर्याय) होंगे।
\\\\\\\\ तुलसी प्रज्ञा अंक 109
46 N
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org