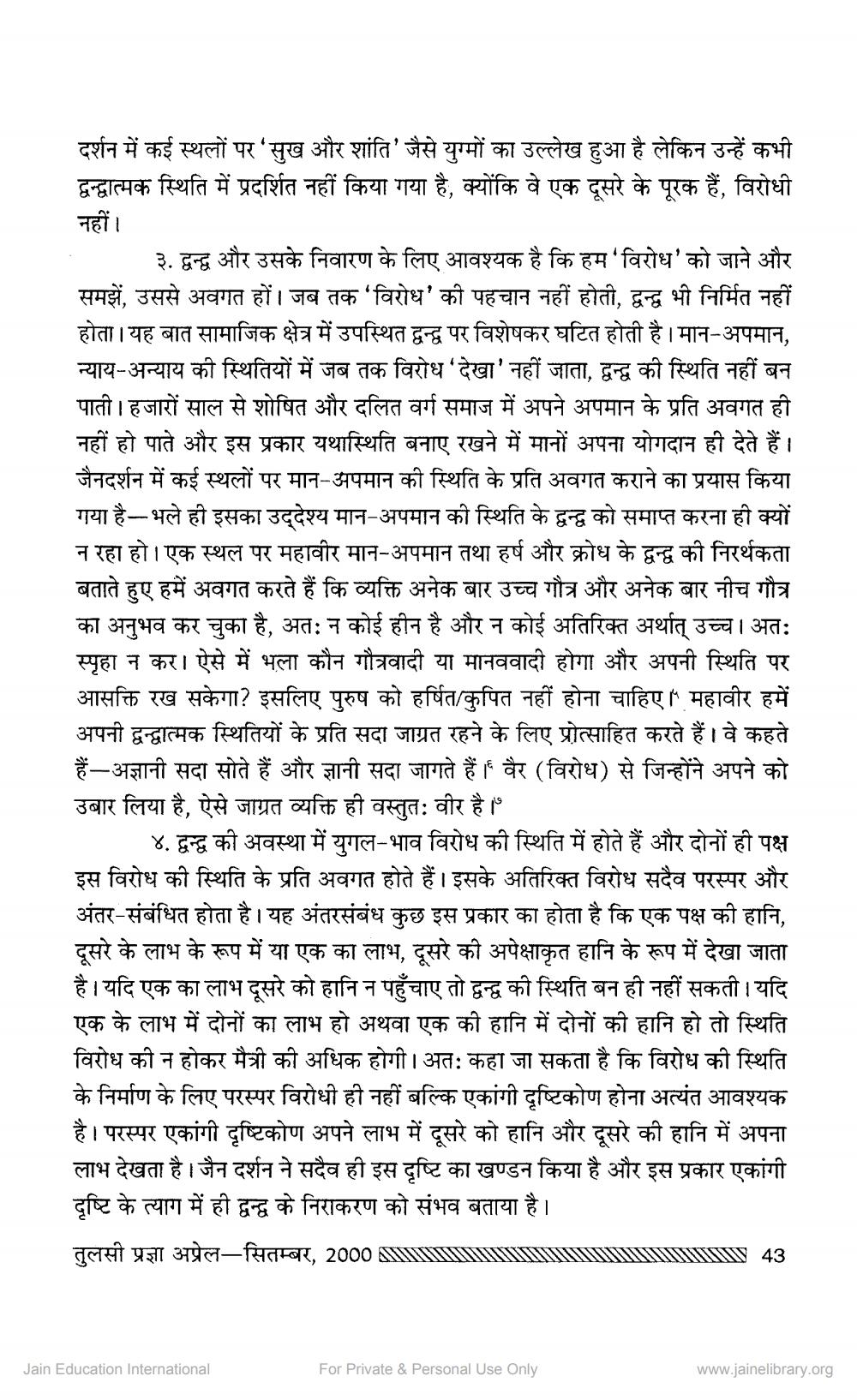________________
दर्शन में कई स्थलों पर 'सुख और शांति' जैसे युग्मों का उल्लेख हुआ है लेकिन उन्हें कभी द्वन्द्वात्मक स्थिति में प्रदर्शित नहीं किया गया है, क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं।
३. द्वन्द्व और उसके निवारण के लिए आवश्यक है कि हम विरोध' को जाने और समझें, उससे अवगत हों। जब तक 'विरोध' की पहचान नहीं होती, द्वन्द्व भी निर्मित नहीं होता। यह बात सामाजिक क्षेत्र में उपस्थित द्वन्द्व पर विशेषकर घटित होती है। मान-अपमान, न्याय-अन्याय की स्थितियों में जब तक विरोध देखा' नहीं जाता, द्वन्द्व की स्थिति नहीं बन पाती। हजारों साल से शोषित और दलित वर्ग समाज में अपने अपमान के प्रति अवगत ही नहीं हो पाते और इस प्रकार यथास्थिति बनाए रखने में मानों अपना योगदान ही देते हैं। जैनदर्शन में कई स्थलों पर मान-अपमान की स्थिति के प्रति अवगत कराने का प्रयास किया गया है- भले ही इसका उद्देश्य मान-अपमान की स्थिति के द्वन्द्व को समाप्त करना ही क्यों न रहा हो। एक स्थल पर महावीर मान-अपमान तथा हर्ष और क्रोध के द्वन्द्व की निरर्थकता बताते हुए हमें अवगत करते हैं कि व्यक्ति अनेक बार उच्च गौत्र और अनेक बार नीच गौत्र का अनुभव कर चुका है, अतः न कोई हीन है और न कोई अतिरिक्त अर्थात् उच्च । अतः स्पृहा न कर। ऐसे में भला कौन गौत्रवादी या मानववादी होगा और अपनी स्थिति पर आसक्ति रख सकेगा? इसलिए पुरुष को हर्षित/कुपित नहीं होना चाहिए। महावीर हमें अपनी द्वन्द्वात्मक स्थितियों के प्रति सदा जाग्रत रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे कहते हैं-अज्ञानी सदा सोते हैं और ज्ञानी सदा जागते हैं। वैर (विरोध) से जिन्होंने अपने को उबार लिया है, ऐसे जाग्रत व्यक्ति ही वस्तुत: वीर है।
४. द्वन्द्व की अवस्था में युगल-भाव विरोध की स्थिति में होते हैं और दोनों ही पक्ष इस विरोध की स्थिति के प्रति अवगत होते हैं। इसके अतिरिक्त विरोध सदैव परस्पर और अंतर-संबंधित होता है। यह अंतरसंबंध कुछ इस प्रकार का होता है कि एक पक्ष की हानि, दूसरे के लाभ के रूप में या एक का लाभ, दूसरे की अपेक्षाकृत हानि के रूप में देखा जाता है। यदि एक का लाभ दूसरे को हानि न पहुँचाए तो द्वन्द्व की स्थिति बन ही नहीं सकती। यदि एक के लाभ में दोनों का लाभ हो अथवा एक की हानि में दोनों की हानि हो तो स्थिति विरोध की न होकर मैत्री की अधिक होगी। अतः कहा जा सकता है कि विरोध की स्थिति के निर्माण के लिए परस्पर विरोधी ही नहीं बल्कि एकांगी दृष्टिकोण होना अत्यंत आवश्यक है। परस्पर एकांगी दृष्टिकोण अपने लाभ में दूसरे को हानि और दूसरे की हानि में अपना लाभ देखता है । जैन दर्शन ने सदैव ही इस दृष्टि का खण्डन किया है और इस प्रकार एकांगी दृष्टि के त्याग में ही द्वन्द्व के निराकरण को संभव बताया है। तुलसी प्रज्ञा अप्रेल-सितम्बर, 2000 SIMILAITI
NATITITIV 43
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org